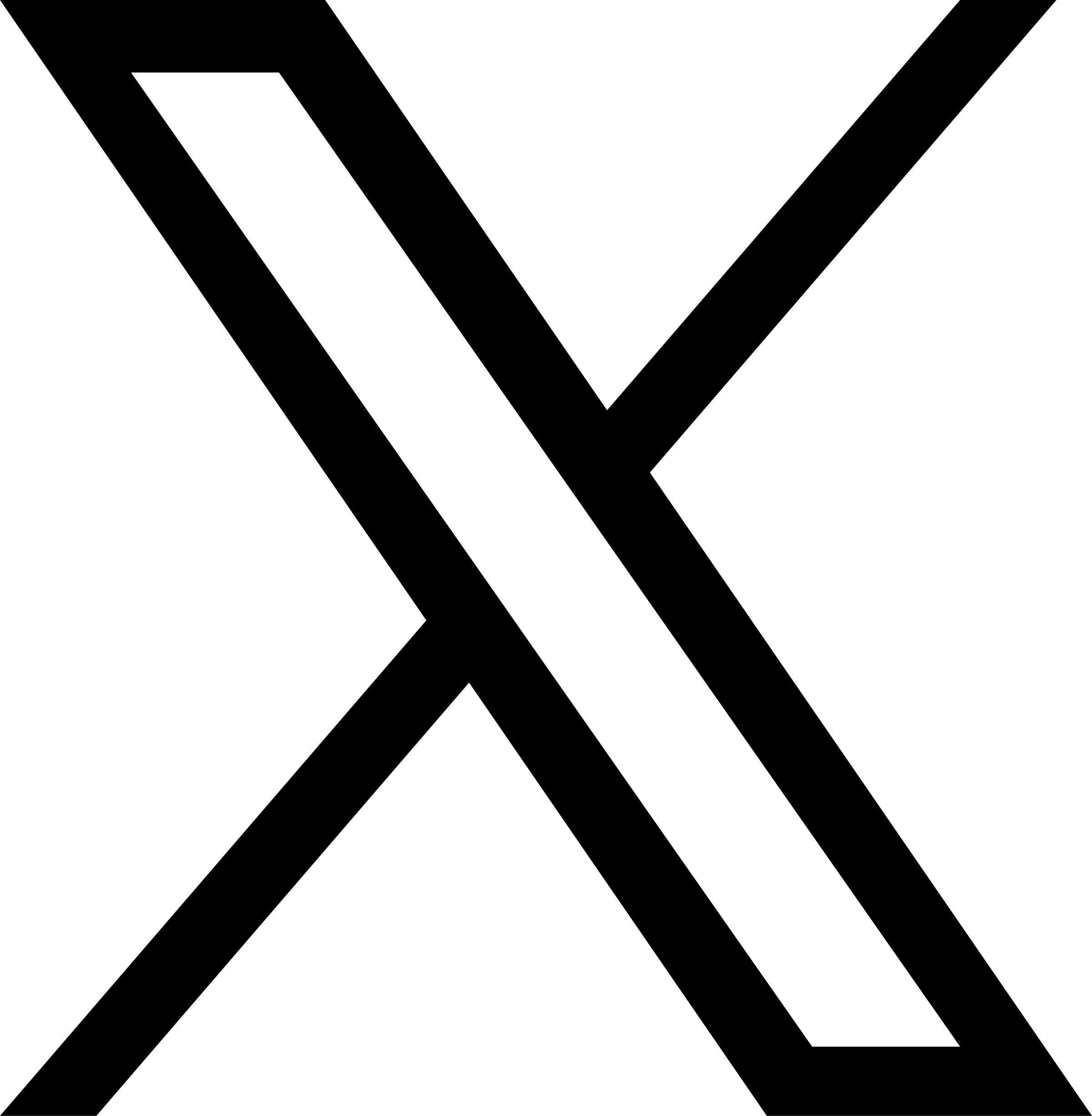“इन गलियों में”: क्या फ़क़त प्यार से अब नफ़रत का सामना हो पाएगा!

ड्रैकुला–सी हो गई नफ़रत लहू पीकर जवां
क्या फ़क़त अब प्यार इसका सामना कर पाएगा
“इन गलियों में ” इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। हालांकि यह गलियां– ‘हनुमान गली और रहमान गली’ मोहब्बत से ही नफ़रत को जवाब देना चाहती हैं। देती हैं। लेकिन यह जवाब आज का नहीं लगता, बल्कि सत्तर-अस्सी या नब्बे के दशक का जवाब लगता है।
आज नफ़रत या सांप्रदायिकता जितनी तीखी और मज़बूत हो गई है या बना दी गई है उसका जवाब इतना आासान नहीं है जितना अविनाश दास की नई फ़िल्म “इन गलियों में” देती है। कुल मिलाकर आज के संदर्भ में एक Complex सवाल का Simplify जवाब दिया गया है।
फिर भी इस फ़िल्म की सराहना करनी होगी। जो भी है, इस दौर में जब प्यार की बात करना भी गुनाह है, और हिंदू-मुस्लिम प्यार तो गुनाह-ए-अज़ीम हो गया है, पूरा माहौल ही नफ़रत की भट्टी में तप रहा है उस समय प्यार की हल्की सी भी फुहार मन को राहत देती है। एक उम्मीद देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे राहुल गांधी की ‘मोहब्बत की दुकान’ से ‘नफ़रत का बाज़ार’ बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन इस बार चुनाव में उसने इस नफ़रत के बाज़ार का धंधा, मंदा तो ज़रूर कर दिया। हालांकि यह काम भी अकेले ‘मोहब्बत की दुकान’ से संभव नहीं हुआ। यह तभी संभव हुआ जब उन्होंने अपने हाथ में संविधान मज़बूती से पकड़ा और लोकतंत्र के ज़रूरी सवाल उठाए। और सबसे महत्वपूर्ण पूरे विपक्ष ने इकट्ठा होकर इंडिया ब्लॉक जैसा गठबंधन बनाने का रणनीतिक काम किया।
मगर आप देख रहे हैं कि इस सबके बावजूद 400 पार का नारा भले ही 240 पर अटक गया, लेकिन सत्ता अभी भी हिंदुत्ववादी फ़ासीवादियों के कब्ज़े में हैं। और उनके एजेंडे में रत्ती भर भी फ़र्क़ नहीं पड़ा है। बल्कि उसे और तेज़ी से लागू किया जा रहा है।
इसलिए आज केवल एक मासूम सी प्रेम कहानी से नफ़रत का सामना हो पाएगा। ये सोचना भोली आशा है।
बेशक नफ़रत का जवाब मोहब्बत ही हो सकती है। और आज भी सांप्रदायकिता, फ़ासीवाद के ख़िलाफ़ चलने वाली हर लड़ाई, भारत की गंगा-जमुनी तहज़ीब और सेकुलर चरित्र को बचाने की हर जद्दोजहद के पीछे मूल विचार तो प्रेम का ही है। लेकिन अब यह नफ़रत, यह बंटवारा, 2014 से पहले वाला नहीं है। अब तो यह नफ़रत इंसानियत ही नहीं बाक़ायदा इंसानों का ख़ून पीकर ड्रैकुला सी जवान हो गई है। दिन-ब-दिन इसका वायरस तो कोविड से भी तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए अब मासूम मोहब्बत के फ़साने से इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।

(दिल्ली के जवाहर भवन में 1 अप्रैल को हुए फ़िल्म के प्रीमियर शो के दौरान हॉल खचाखच भरा रहा)
हालांकि अविनाश दास की फ़िल्म हिंदू-मुस्लिम के प्यार, राजनेता की कुटिलता और सांप्रदायिकता, मॉब लिंचिंग सबको रेखांकित करती है, लेकिन छूती भर है। और एक वोट या एक नेता की चुनावी हार से उसका हल करती दिखती है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है।
लेकिन एक फ़िल्मकार, एक कलाकार से आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं। या उसके कंधों पर कितनी ज़िम्मेदारी डाल सकते हैं।
हां, यह कहा जा सकता है कि जिस मज़बूती से अविनाश दास की पहली फ़िल्म ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। वैसा इस फ़िल्म में देखने को नहीं मिला।
अविनाश दास एक पत्रकार रहे हैं। कई कामों में उन्होंने पहलक़दमी की। जब ब्लॉग का ज़माना आया तो उन्होंने मोहल्ला जैसा ब्लॉग बनाया। फ़िल्म बनाई तो पहली ही फ़िल्म “अनारकली ऑफ आरा” से धूम मचा दी। 2017 में आई इस फ़िल्म में मुख्य भूमिका स्वरा भास्कर ने निभाई थी। साथ में पंकज त्रिपाठी और संजय मिश्रा थे। यह बहुत पॉवरफुल फ़िल्म थी, जिसने अविनाश को एक संजीदा फ़िल्मकार के रूप में स्थापित कर दिया। इसके अलावा भी उन्होंने कई फ़िल्मों में निर्देशन किया। और अब वे लाए हैं– “इन गलियों में”।
“इन गलियों में ” लखनऊ की दो गलियों हनुमान गली और रहमान गली के माध्यम से हिंदू-मुस्लिम एकता, हिंदू-मुस्लिम लड़के-लड़की के प्यार, एक राजनेता की सांप्रदायिक राजनीति, उसका असर और अंत में उसकी पराजय की कहानी कहती है। इस कहानी का केंद्रीय पात्र है मिर्ज़ा। जिसे बख़ूबी निभाया है जावेद ज़ाफरी ने। फ़िल्म में शेरो-शायरी का ख़ूब तड़का है। फ़िल्म की शुरुआत ही एक कवि सम्मेलन-मुशायरे से होती है। जिसमें लखनऊ के मशहूर किस्सागो हिमांशु वाजपेयी ने ख़ूब रंग जमाया है।
फ़िल्म के हीरो हैं हरिया (विवान शाह) और हीरोइन हैं शब्बो यानी शबनम (अवंतिका दसानी)। दोनों सब्ज़ी बेचने वाले बने हैं। और इन्हीं की प्रेम कहानी है इन गलियों में । लेकिन मेरे एक पत्रकार मित्र फ़िल्म देखने के बाद मुझसे पूछते हैं कि अगर कहानी में हीरो-हीरोइन का धर्म बदल दिया जाता तो। यानी लड़का मुसलमान होता और लड़की हिंदू, तो…? तो मैं कहता हूं कि बवाल हो जाता। यह फ़िल्म ‘लव जिहाद’ के विवाद में फंस जाती और शायद रिलीज़ भी न हो पाती। इसलिए शायद यह सेफ साइड चुनी गई। हालांकि इस फ़िल्म में संकेतों के ज़रिये मिर्ज़ा के बेटे-बहू की कहानी भी सामने आती है। जिसमें बहू यानी लड़की हिंदू है, और उन दोनों को भी नफ़रती भीड़ मार डालती है।
इसलिए मेरे लिए ये कहानी मिर्ज़ा की है। जो इन दोनों गलियों के बीच चाय की दुकान चलाते हैं और वहीं होती है सारी बतकही, शेरो-शायरी और आज के माहौल पर चर्चा और व्यंग्य। मिर्ज़ा कबीर से प्रेरित हैं और इन दोनों गलियों के सेतु यानी पुल हैं जो दोनों समुदाय को जोड़ते हैं और लगातार एकता की बात करते हैं और अंत में अपनी जान गंवा देते हैं, लिंचिंग का शिकार होते हैं।
एक दीवाना भी है (इश्तियाक ख़ान), जिसके ज़रिये भी व्यंग्य और सवाल उठाने की कोशिश की गई है जो फ़िल्म के अंत में इन्हीं गलियों को छोड़कर भारत की खोज में निकल जाता है। इस कहानी का विलेन है नेता तिवारी (सुशांत सिंह), जो हिंदू-मस्लिम दोनों को बांटकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इसके लिए हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का अच्छा प्रयोग किया गया है। आज की तकनीक यानी सोशल मीडिया-इंस्टाग्राम रील का भी अच्छा प्रयोग है। हीरो अपने प्यार के इज़हार के लिए इसी रील का प्रयोग करता है और एक दूसरा नफ़रत और अफ़वाह फ़ैलाने के लिए भी इसी रील का प्रयोग करता है। और अंत में हीरो की मां भी अपना संदेश देने के लिए इसी रील का प्रयोग करती हैं और कहती हैं जब नफ़रत के लिए रील का प्रयोग किया जा सकता है तो प्यार फैलाने के लिए भी रील का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता।
जावेद जाफ़री के अलावा हीरोइन अवंतिका के अभिनय ने भी काफ़ी प्रभावित किया। बाक़ी कलाकार सामान्य रहे।
फ़िल्म की कथा-पटकथा लिखी है पुनर्वसु ने। जो उनके पिता कवि-कथाकार वसु मालवीय की एक पुरानी कहानी पर आधारित है। गाने हल्के-फुल्के मनोरंजक हैं जिन्हें लिखा है विमल कश्यप, पुनर्वसु, यश मालवीय और सौरभ खालसी ने। संगीत दिया है अमाल मलिक, सौरभ खालसी और अरविंद सागोले ने। निर्माता हैं विनोद यादव और नीरू यादव।
इस फ़िल्म में लखनऊ के प्रणाम वालेकुम वाले व्यंग्यकार राजीव ध्यानी हैं तो कवि-लेखक यश मालवीय भी। राजनीतिक व्यंग्यकार डॉ. मेदुसा भी हैं।
इस फ़िल्म का प्रीमियर अभी मंगलवार एक अप्रैल को दिल्ली के जवाहर भवन में किया गया। जहां बड़ी संख्या में अविनाश दास को चाहने वाले पहुंचे। इस मौके पर फ़िल्म के कई कलाकार भी मौजूद थे।
इस मौके पर जब अविनाश से बातचीत में पहली फ़िल्म अनारकली ऑफ आरा और इन गलियों में की तुलना में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो उनकी पहली फ़िल्म थी जिसमें उन्होंने अपनी सारी मेहनत, सारी हसरत उड़ेल दी थी। इस फ़िल्म के संदेश के बारे में भी उनका यही कहना है कि प्यार ही नफ़रत का हल है।
इसलिए अंत में यही कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर इस दौर में हालांकि इतना काफ़ी नहीं लेकिन एक फ़िल्मकार के लिए फिर भी इतना बहुत है यार! ये क्या कम है कि इस दौर में जब स्टैंडअप कॉमेडी भी सत्ता को बर्दाश्त नहीं हो रही, हिंसा, तोड़फोड़, एफ़आईआर दर्ज हो रही हैं, अविनाश दास ने चुपके से हिंदू-मुस्लिम एकता और प्यार की प्यारी सी कहानी परदे पर उतार दी, और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बेशक इसे देखा और दिखाया जाना चाहिए।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।