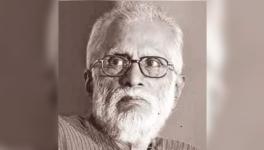विश्लेषण : ट्रंप के टैरिफ़ से विश्व सकल मांग में कमी होगी

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ़ पर मीडिया में चलताऊ ढंग से, उनके खास संदर्भ को हिसाब में लिए बिना ही चर्चा हो रही है। यह वह संदर्भ है जहां अमेरिकी सरकार, बढ़े हुए टैरिफ़ से आने वाला राजस्व मालों तथा सेवाओं को खरीदने पर खर्च करने के प्रति अनिच्छुक है, जिस मामले की हम जरा आगे चर्चा करेंगे।
दूसरे देश भी, जो कि ट्रंप के बढ़े हुए टैरिफ़ के चलते अमेरिकी बाजार खो रहे होंगे, इस घाटे की भरपाई अपने ही घरेलू बाजारों का विस्तार करने के जरिए करने में असमर्थ होंगे। उनके घरेलू बाजारों में इस तरह की बढ़ोतरी सरकारी खर्चों में बढ़ोतरी किए जाने के जरिए ही हो सकती है, लेकिन वह भी तब जब उसके लिए वित्त व्यवस्था या तो राजकोषीय घाटे के जरिए की जाए या फिर अमीरों पर कर लगाने के जरिए की जाए। लेकिन, ये दोनों ही रास्ते वैश्वीकृत वित्तीय पूंजी के लिए जैसे अभिशाप ही हैं और वर्तमान नवउदारवादी व्यवस्था में राष्ट्र राज्य को इस वित्तीय पूंंजी का हुक्म मानना ही होता है। इसलिए, अमेरिकी संरक्षणवाद के साथ कुल मिलाकर विश्व की समग्र मांग का सिकुड़ना और इसलिए नव-उदारवादी पूंजीवाद के संकट का और तीखा होना लगा हुआ है।
इस तथ्य पर बहुत कम ही ध्यान दिया गया है कि ट्रंप के टैरिफ़ से भले ही अमेरिका में घरेलू उत्पाद तथा वहां रोजगार में बढ़ोतरी हो जाए, इससे विश्व पूंजीवादी संकट बदतर ही होने जा रहा है और इसलिए, अमेरिका तथा अन्य देशों, दोनों को मिलाकर, उत्पाद का स्तर घटने ही जा रहा है।
आइए, हम देखें कि विश्व सकल मांग में यह कमी किस तरह होती है।
टैरिफ़ से घरेलू बाजार में मुद्रा मजदूरी के सापेक्ष आयातित मालों की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह कम से कम आंशिक रूप से, इस तरह के आयातों की जगह घरेलू तौर पर उत्पादित मालों द्वारा लिया जाना संभव बनाता है। टैरिफ़ जाहिर है कि सारे आयातों को खत्म नहीं कराते हैं, लेकिन साफ तौर पर कुछ तो खत्म करा ही देते हैं। जो आयात इन टैरिफ़ के बावजूद बने रहते हैं, उन पर सरकार टैरिफ़ राजस्व बटोरती है, जो उपभोक्ताओं की जेब से आता है, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा मेहनतकशों का होता है, जिनसे टैरिफ़ के चलते बढ़ी हुई कीमतों के जरिए वसूली की जाती है। दूसरे शब्दों में, टैरिफ़ जिस हद तक आयातों को पूरी तरह से खत्म करने में कामयाब नहीं होते हैं और इसलिए उनसे किसी हद तक टैरिफ़ राजस्व की उगाही संभव होती है, उनके जरिए मजदूर वर्ग के हाथों से निकल कर सरकार के हाथों में, क्रय शक्ति का पुनर्वितरण हो रहा होता है।
सकल मांग के स्तर में कमी होगी
चूंकि मेहनतकश जनता अपनी लगभग पूरी की पूरी क्रय शक्ति मालों तथा सेवाओं को खरीदने पर खर्च करती है, उसकी जेब से निकलकर, सरकार के खजाने की दिशा में क्रय शक्ति का इस प्रकार का कोई भी पुनर्वितरण, टैरिफ़ लगाने वाले देश में सकल मांग के स्तर में कमी नहीं कर रहा होगा, बशर्ते उसकी सरकार की टैरिफ़ का यह राजस्व मालों व सेवाओं को खरीदने पर खर्च कर रही हो। लेकिन, अगर वह सरकार ऐसा नहीं करती है, तो टैरिफ़ लगाने वाले देश में सकल मांग के स्तर में कमी हो जाएगी। अमेरिका में ठीक यही होने जा रहा है क्योंकि ट्र्रम्प के टैरिफ़ से आने वाले राजस्व को मालों तथा सेवाओं की खरीद पर खर्च नहीं किया जाने वाला है।
ट्रंप प्रशासन, अमीरों को भारी कर रियायतें देता आया है और टैरिफ़ से आने वाले राजस्व का उपयोग इस तरह की कर रियायतों से पैदा होने वाले राजकोषीय घाटे में कमी करने के लिए किया जाएगा। दूसरे शब्दों में टैरिफ़ राजस्व खर्च तो किया ही नहीं जाएगा बल्कि उसे तो राजकोषीय घाटे को घटाने में भी लगाया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि सरकार द्वारा बटोरा जाने वाला टैरिफ़ राजस्व का हरेक डालर, अमेरिका में सकल मांग के स्तर को घटा रहा होगा। और चूंकि शेष दुनिया की सरकारों का खर्चा, अमेरिकी मांग में इस कमी की भरपाई करने के लिए बढ़ नहीं रहा होगा, इसका अर्थ यह हुआ कि पूरी दुनिया को मिलाकर देखा जाए तो, सकल मांग का स्तर घट रहा होगा, जो विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी के हालात को और बिगाड़ देगा।
बहरहाल, खुद अमेरिका में, सकल मांग में कमी के बावजूद, आयातों की कीमत पर घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरे शब्दों में, टैरिफ़ के चलते अमेरिका में तो मंदी दूर हो सकती है, लेकिन समग्रता में पूंजीवादी दुनिया को देखा जाए तो यानी अमेरिका और बाकी दुनिया को जोडक़र देखा जाए तो, आर्थिक गतिविधि के स्तर में गिरावट हो जाएगी।
अमेरिका द्वारा बेरोज़गारी के निर्यात से बड़ा मामला
यह अमेरिका द्वारा अपने यहां से ‘‘बेरोजगारी का निर्यात’’ किए जाने से ज्यादा का मामला है यानी यह सिर्फ अमेरिका द्वारा ‘‘पड़ोसी जाए भाड़ में’’ की नीति अपनाए जाने भर का मामला नहीं है। यह ऐसा मामला है जहां अगर मालों पर टैरिफ़ लगाए जाने के चलते अमेरिका में घरेलू उत्पाद में 100 इकाई की बढ़ोतरी होती है तो, शेष दुनिया में उत्पाद में सिर्फ 100 इकाई की नहीं बल्कि 100 से ज्यादा इकाई, मिसाल के तौर पर 120 या 150 इकाई की कमी हो रही होगी। इससे समग्रता में दुनिया के स्तर पर उत्पाद के स्तर में गिरावट आ रही होगी। संक्षेप में यह ऐसा मामला है जहां समग्रता में दुनिया के स्तर पर आर्थिक गतिविधि का स्तर तो सिकुड़ रहा होगा, जबकि अमेरिका में आर्थिक गतिविधि का स्तर बढ़ रहा होगा।
दूसरे देश अगर अमेरिकी टैरिफ़ के खिलाफ जवाबी टैरिफ़ लगा देते हैं, तो उससे इस स्थिति में रत्तीभर फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। वास्तव में जिस हद तक ये देश अपने टैरिफ़ राजस्व का, जो कि अपने घरेलू मजदूरों की कीमत पर जुटाया जा रहा होगा, अपने राजकोषीय घाटों को कम करने के लिए या अपने धनवानों को कर रियायतें देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि धनवान तो अपने हाथ आए संसाधनों में से एक छोटे से हिस्से का ही उपभोग करते हैं, इसका समग्र प्रभाव सकल विश्व मांग के और भी ज्यादा सिकुड़ जाने के रूप में सामने आएगा। दूसरे शब्दों में, अमेरिकी टैरिफ़ के जवाब में अन्य देशों द्वारा ऐसा ही किया जाना, मांग को तथा इसलिए उत्पाद को भी अमेरिका से इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में वापस लाने का काम तो जरूर करेगा, लेकिन यह समग्रता में विश्व अर्थव्यवस्था के हालात को और बदतर ही बनाएगा और नव-उदारवादी पूंजीवाद का संकट और बढ़ जाएगा।
दूसरों की कीमत पर संकट से उबरना चाहता है अमेरिका
टैरिफ़ पर होने वाली आम चर्चा में, यह आखिरी नुक्ता पूरी तरह से छूट जाता है। इस तरह की चर्चा में टैरिफ़ को किसी भी देश द्वारा सिर्फ मांग का तथा इसलिए उत्पाद का, अन्य देशों से हटाकर अपने देश की ओर, तबादला करने के साधन के रूप में ही देखा जाता है। लेकिन, अगर टैरिफ़ ऐसे हालात में थोपे जा रहे हों, जहां टैरिफ़ राजस्व, जो मेहनतकश जनता की कीमत पर बटोरा जाता है, सरकार द्वारा खर्च किया ही नहीं जाता है तथा उसकी बचतों को बढ़ाने के ही काम में आता है, तब टैरिफ़ का समग्रता में दुनिया में मांग तथा उत्पाद के स्तर को सिकोड़ने में अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा यानी नवउदारवादी पूंजीवाद का संकट और उलझ जाएगा।
इस संकट के संदर्भ में अमेरिका की भूमिका खासतौर पर दर्ज करने लायक है। उदारवादी पूंजीवादी राय के अनुसार, पूंजीवादी दुनिया का नेता होने के नाते, उससे यह उम्मीद की जाती थी कि इस संकट पर काबू पाने के लिए, विकसित पूंजीवादी देशों की ओर से एक एकजुट नजरिया तय कराने का नेतृत्व करेगा। उदारवादी पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों ने यही सुझाया होता। वास्तव में, 1930 की महामंदी के दौरान जेएम केन्स ने विकसित पूंजीवादी देशों की ओर से ऐसी सम्मिलित कार्रवाई का ही सुझाव दिया था। इसके विपरीत आज हो यह रहा है कि अमेरिका अकेले खुद को ही संकट से निकालने की कोशिश कर रहा है और समग्रता में पूंजीवादी दुनिया के लिए चीजों को और भी बदतर बना रहा है।
दूसरे शब्दों में अमेरिका जो ‘‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’’ करना चाहता है, सामग्रता में पूंजीवादी दुनिया के इस संकट से उबरने के लिए कोई रास्ते सुझाने का नेतृत्व करने के जरिए नहीं करना चाहता है, बल्कि शेष दुनिया को और खासतौर पर विकासशील दुनिया के देशों को, और ज्यादा बदहाली मंजूर करने के लिए मजबूर करने के लिए, उनकी बांहें मरोड़ने के जरिए ऐसा करना चाहता है, जिससे अमेरिका अकेले ही इस संकट से खुद को निकालने में कामयाब हो सके।
ट्रंप जब ऐसा कर रहा है, तो वह ऐसा कोई इसलिए नहीं कर रहा है कि वह शैतान है या मूर्ख है और इस वजह से संकट से उबरने का जो ‘‘जागरूक’’ तरीका है, उससे वह परहेज कर रहा है। वह ऐसा इसलिए कर रहा है कि वह जो कुछ भी कर रहा है, उदारवादी पूंजीवादी बुद्धिजीवी जिस तरह की सुंदर स्थिति की कल्पना करते हैं उसके बरक्स, यही पूंजीवाद की प्रकृति के साथ मेल खाता है। चूंकि पूंजीवाद एक नियोजित व्यवस्था नहीं है, यह अपने सामने उपस्थित संकट के किसी ‘‘तार्किक समाधान’’ के अनुकूल नहीं होता है। इसलिए, अमेरिका इस संकट के बीच अपने ही स्वार्थों की हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है।
विकासशील दुनिया को संकट में धकेलने के हथियार
अमेरिका खुद को संकट से निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि शेष दुनिया को और खासतौर पर विकासशील दुनिया को इस संकट में और गहरा डुबोने के लिए तैयार है। यह विभिन्न व्यापार वार्ताओं में उसके द्वारा की जा रही मांगों से स्वत:स्पष्ट है। वह अन्य देशों को बहुत ऊंचे टैरिफ़ लगाने की धमकियों से शुरूआत करता है, लेकिन अगर संंबंधित देश वार्ताओं में भांति-भांति के अमेरिकी मालों को शून्य टैरिफ़ पर अपने यहां आने देने के लिए राजी हो जाता है, तो अमेरिका जितने टैरिफ़ की धमकी दी थी, उससे कम टैरिफ़ पर समझौता करने के लिए भी राजी हो जाता है। वास्तव में उसने अनेक देशों के साथ व्यापार वार्ताओं में इसी तरह से समझौते कर भी लिए हैं।
लेकिन, विकासशील दुनिया के लिए इसके नतीजे सत्यानाशी होंगे। मिसाल के तौर पर भारत के लिए इसका अर्थ होगा, अमेरिका के लिए हमारे देश के जो मुख्य निर्यात हैं, जिनमें टैक्सटाइल्स, जवाहरात तथा आभूषण तथा दवाएं शामिल हैं, उन पर अमेरिका द्वारा घोषित टैरिफ़ में कुछ रियायतें हासिल करने के बदले में, बिना किन्हीं नियंत्रणों के विभिन्न अमेरिकी मालों को अपने देश में आने देना, जैसे अमेरिकी दुग्ध उत्पाद, फल तथा मेवे तथा अन्य वस्तुएंं। यह करोड़ों भारतीय किसानों के लिए बदहाली लाएगा, क्योंकि वे आयातित मालों से होड़ नहीं कर पाएंगे। और ऐसा कोई इसलिए नहीं होगा कि अमेरिकी किसान उत्पादन के मामले में ज्यादा ‘‘कुशल’’ हैं, बल्कि ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि उन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा बहुत भारी सब्सीडियां दी जाती हैं। यह अलग बात है कि विश्व व्यापार संगठन ने अतार्किक तथा कपटपूर्ण तरीके से इन सब्सीडियों को, प्रतिबंधित सब्सीडियों की सूची से बाहर कर रखा है।
नव-उदारवाद ने हमारे देश को ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया है, जहां उसके पास दो ही विकल्प हैं, या तो अपने किसानों के हितों की बलि दे या फिर दवा, जवाहरात तथा आभूषण, वस्तव तथा ऐसी ही अन्य चीजों के उत्पादन में लगे लोगों के हितों की बलि दे। बहरहाल, इस मुसीबत से निकलने का रास्ता इनमें से किसी एक विकल्प का चुनाव करना नहीं है बल्कि उस व्यवस्था को ही लांघना है, जो हमारे देश को ऐसे विकल्पों में से चुनाव करने के लिए मजबूर करती है और इसका अर्थ है, नव-उदारवाद को ही लांघना।
(लेखक दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आर्थिक अध्ययन एवं योजना केंद्र में प्रोफ़ेसर एमेरिटस हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
मूल रूप से अंग्रेज़ी में प्रकाशित आलेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें–
An Out of Sight Ramification of Trump’s Tariffs
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।