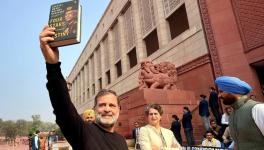79वें स्वतंत्रता दिवस पर विशेष: साम्राज्यवाद और भारत के साथ उसकी दादागीरी

यह विडंबनापूर्ण है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भारतीय जनता के संघर्ष की जीत की अठहत्तरवीं सालगिरह के मौके पर, अमेरिकी साम्राज्यवाद भारत को खुल्लमखुल्ला धौंस दे रहा है कि उसका फरमान मानना पड़ेगा। बहरहाल, यह कहा जा सकता है कि ऐसा करना तो साम्राज्यवाद की प्रकृति ही है। वास्तव में इन अठहत्तर सालों के दौरान अमेरिकी साम्राज्यवाद ने भारत को अपने फरमानों के हिसाब से चलाने की कई कोशिशें की हैं। लेकिन, पहले की इन कोशिशों और वर्तमान कोशिश में, दो बुनियादी अंतर हैं।
महत्वपूर्ण बदलाव
पहला, वर्तमान कोशिश को इस तरह की भाषा में लपेट कर पेश नहीं किया जा रहा है कि, ‘हम जो कह रहे हैं, खुद अपने लाभ के लिए वही करो।’ अब भाषा उससे कहीं ज्यादा बेलाग है: ‘हम जो कह रहे हैं, अपने फायदे के लिए वही करो, वर्ना तुम्हें सजा दी जाएगी।’ दूसरे, अतीत में जो होता आया था उसके विपरीत भारत सरकार अब इसका दो-टूक तरीके से मुकाबला नहीं कर रही है बल्कि इस दादागीरी के सामने मिश्रित संकेत दे रही है। मैं इसका खुलासा करना चाहूंगा।
स्वतंत्र भारत ने जब सीटो (एसईएटीओ) तथा सेंटो (सीईएनटीओ) जैसे, सैन्य गठजोड़ों में से किसी में भी शामिल होने से इंकार कर दिया था, जो अमेरिकी साम्राज्यवाद ने सोवियत संघ को घेरने के लिए दुनिया भर में खड़े किए थे और इसके बजाए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को चुना था, उसने अमेरिका की नाराजगी मोल ली थी। अमेरिका के तत्कालीन विदेश सचिव, जॉन फॉस्टर डलास ने यह सिद्धांत पेश किया था: ‘अगर तुम हमारे साथ नहीं हो, तो तुम हमारे खिलाफ हो’। इसी के अनुसार अमेरिका ने भारत के साथ शत्रुता का बरताव किया। नियोजन के महत्वाकांक्षी वर्षों के दौरान, जब आत्मनिर्भरता पर, सार्वजनिक क्षेत्र के तत्वावधान में अर्थव्यवस्था का भारी उद्योग आधार निर्मित करने पर और देश की अर्थव्यवस्था पर विकसित दुनिया की पूंजी के शिकंजे को हटाने पर जोर दिया जा रहा था, हमें अमेरिका से भी और विश्व बैंक जैसी उसके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं से भी, शायद ही कोई ‘विकास सहायता’ मिली थी।
अमेरिकी फंड से संचालित जो विभिन्न अमेरिकी ‘विशेषज्ञ’ भारत के दौरे पर आए थे, उन्होंने उस महलनवीस रणनीति को अपनाने खिलाफ ‘सलाह’ दी थी, जो आत्मनिर्भरता के इस तरह प्राथमिकता दिए जाने को अभिव्यक्ति देती थी। (देखिए, डेनियल और एलिस थार्नर की किताब, लेंड एंड लेबर इन इंडिया में लेख, ‘प्लाओइंग द प्लान अंडर’।
तब साम्राज्यवादी धौंस और भारत का प्रतिरोध
बहरहाल, सोवियत संघ के सुदृढ़ समर्थन से भारत गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति और आत्मनिर्भरता की अपनी नीति, दोनों पर डटा रहा और उसने ऐसा किया विकसित दुनिया की पूंजी के वर्चस्व की काट करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग करने के जरिए। उसे विदेशी मुद्रा की कड़ी राशनिंग करनी पड़ी, लेकिन वह अपने रास्ते पर बना रहा। 1950 के दशक के आखिर में, डलेस की मृत्यु के बाद अमेरिका ने धीरे-धीरे अपना रुख बदला। उसको डर था कि उसकी दूर खड़े रहने की जैसी नीतियां, भारत जैसे देशों को झुकाने का काम करने के बजाए, खुद उसी का नुकसान कर रही थीं (और सोवियत संघ की मदद कर रही थीं)। पचास के दशक के आखिर में आइजनहावर के भारत के दौरे के बाद, आखिरकार विश्व बैंक से कुछ ‘सहायता’ आनी शुरू हुई और वह भी सिर्फ बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए।
पुन: बांग्लादेश युद्ध के दौरान, जब भारत के हस्तक्षेप ने अमेरिका को गड़बड़ी का फायदा उठाने के स्वर्णिम अवसर से वंचित कर दिया, उसकी सरकार तो इतनी खफा हो गयी कि उसने अपने विमान वाहक पोत, यूएसएस एंटरप्राइज की अगुआई में अपने टास्क फोर्स 74 को भारत को धौंस देने के लिए बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। बहरहाल, अमेरिकी धमकियों से अविचल भारत अपने रास्ते पर कायम रहा और उसने बांग्लादेश के निर्माण की प्रक्रिया में मदद की।
इस तरह अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा दादागीरी चलाया जाना और सिर्फ अपना वर्चस्व कायम करने के आम साम्राज्यवादी उद्यम के तौर पर ही नहीं, ठोस मामलों में भी भारत को अमेरिकी एजेंडा के हिसाब से चलाने की कोशिशें किया जाना, एक पुरानी परिघटना है और स्वतंत्र भारत पहले सफलता के साथ इसका प्रतिरोध करता आया था। लेकिन, वर्तमान दादीगीरी, भले ही नयी चीज नहीं है, एक बिल्कुल भिन्न संदर्भ में हो रही है, जहां देश ने नव-उदारवादी पूंजीवाद को और इसलिए वैश्वीकृत वित्तीय पूंजी के वर्चस्व को अंगीकार किया है।
वर्तमान अमेरिकी धौंसबाज़ी
डोनाल्ड ट्रंप की वर्तमान धौंसबाजी, जो भारत तक ही सीमित नहीं है, दो मुद्दों को लेकर है। पहला है टैरिफ का मुद्दा। इस मामले में 1 अगस्त तक समझौता नहीं हो पाने का अर्थ यह है कि अब अमेरिकी बाजारों में भारतीय मालों पर 25 फीसद टैरिफ लगेगा। दूसरा मुद्दा दंडात्मक टैरिफों का है, जो अमेरिका, भारतीय मालों पर सिर्फ इसलिए लगाने की धमकियां दे रहा है कि भारत, रूस के खिलाफ पश्चिमी द्वारा लगायी गयी पाबंदियों का उल्लंघन करते हुए, उससे तेल खरीदता रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने ब्रिक्स को लेकर भी टिप्पणियां की हैं, जो इसका इशारा है कि वह भारत को इसके लिए धौंस में लेने का इरादा रखता है कि वह या तो ब्रिक्स संगठन को छोड़ ही दे या और भी ज्यादा संभावना उससे इस संगठन में अमेरिका के एजेंट या ट्रोजन हॉर्स का काम कराने की है।
बहरहाल, रूसी तेल खरीदने के तात्कालिक तथा बुनियादी मुद्दे पर भारत सरकार किंतु-परंतु करती रही है, परस्पर-विरोधी बयान देती रही है, जो अमेरिका के तुष्टिकरण की ओर इशारा करते हैं।
चूंकि रूसी तेल, अमेरिका द्वारा अनुमोदित, भारत को उपलब्ध दूसरे सभी तेल स्रोतों से सस्ता है, यह स्वत:स्पष्ट है कि भारत को दबाव डालकर रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए मजबूर किया जाना, उसे अपने ही हितों के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर किया जाना है। और वह भी किसलिए? ये कोई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लगायी गयी पाबंदियां तो हैं नहीं, जैसी पाबंदियां मिसाल के तौर पर रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगायी गयी थीं। ये तो अमेरिका तथा अन्य साम्राज्यवादी देशों द्वारा अपना हुक्म न मानने वाले देशों के खिलाफ लगायी गयी पाबंदियां हैं, जैसे क्यूबा, ईरान या वेनेजुएला के खिलाफ उसकी पाबंदियां। इसलिए, अन्य देशों को धौंस देकर ऐसी पाबंदियां स्वीकार करने के लिए मजबूर करना, साम्राज्यवाद के हितों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें अपने ही हितों के खिलाफ जाने के लिए मजबूर करना है।
दूसरे शब्दों में इसका कोई आवरण तक नहीं है कि इन देशों से किसी उच्चतर सिद्धांत के नाम पर, अमेरिका का अनुसरण करने के लिए कहा जा रहा है। उन्हें तो खुल्लमखुल्ला और साफ तौर पर धौंस में लिया जा रहा है, ताकि खुद उनकी कीमत पर, साम्राज्यवाद के रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाया जा सके।
नियंत्रणात्मक से नवउदारवादी निजाम में संक्रमण
मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर ट्रंप की बात को साहसपूर्वक और निर्णायक तरीके से ठुकराया क्यों नहीं? आखिरकार, अगर चीन को छोड़ भी दिया जाए तब भी, ब्राजील जैसे पूंजीवादी देश की भी सरकार ने ट्रंप का साहस के साथ जवाब दिया है। राष्ट्रपति लूला ने एलान किया है कि अगर ट्रंप, ब्राजील के मालों पर 50 फीसद टैरिफ लगाएगा, तो ब्राजील भी अमेरिकी मालों पर 50 फीसद टैरिफ लगा देगा। कांग्रेस पार्टी ने उचित ही मोदी की बुजदिली को रेखांकित किया है और उसके मुकाबले में बांग्लादेश युद्ध के दौरान निक्सन से इंदिरा गांधी की साहसिक टक्कर को रखा है। (निक्सन ने एक बार कबूल किया था कि उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने में डर लगता था।) लेकिन, एक नेता की साहसिकता या बुजदिली, वर्गीय आधार से स्वतंत्र नहीं होती है। और लूला और मोदी के बीच यही अंतर है कि जहां लूला की जड़ें मजदूर वर्ग के बीच हैं, मोदी को मजदूरों के कुछ वोट भले ही मिलते हों, वह बुनियादी तौर पर बड़े पूंजीपति वर्ग के सहारे खड़े हैं। इसी प्रकार, अमेरिकी साम्राज्यवाद के धौंसबाजी के हथकंडों के प्रति, भारत के रुख में तब और अब में जो अंतर है, वह उतना ज्यादा मोदी की तुलना में नेहरू तथा इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत गुणों की भिन्नता में निहित नहीं है (हालांकि उनके व्यक्तिगत गुणों के अंतर से इंकार नहीं किया जा सकता है), बल्कि यह अंतर साम्राज्यवाद-विरोधी नियंत्रणात्मक निजाम और नव-उदारवादी निजाम के बीच के अंतर में ही ज्यादा निहित है।
यह स्वत:स्पष्ट है कि किसी देश की विदेश नीति और उसकी आर्थिक नीति के बीच घनिष्ठ रिश्ता होता है। जहां नियंत्रणात्मक आर्थिक नीति, जो आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देती थी, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति से मेल खाती थी और इसलिए, साम्राज्यवादी दादागीरी का मुकाबला करने के लिए उसके तैयार होने से तथा मुकाबला करने की उसकी सामर्थ्य से मेल खाती थी, नव-उदारवादी निजाम तो आत्मनिर्भरता की किसी भी कोशिश को विफल करने में ही गर्व करता है। ‘मेक इन इंडिया’ विदेशी पूंजी के लिए इसका आमंत्रण भर है कि यहां आकर उत्पादन करे। नव-उदारवाद का मूल तर्क ही, किसी भी विकासशील देश का आत्मनिर्भरता की तमाम कोशिशों से दूर हटना है और यह अपरिहार्य रूप से इन देशों को साम्राज्यवादी धौंसबाजी के सामने वेध्य बना देता है।
साम्राज्यवाद की गढ़ी वैश्विक व्यवस्थाएं बदल जाती हैं
भारत में जब नव-उदारवादी निजाम लाया गया था, उसके पक्ष में यह दलील दी जा रही थी कि यह एक स्थायी नयी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अंतर्गत पूंजी वैश्विक स्तर पर गतिमान होगी, जिसके चलते विकासशील दुनिया या ग्लोबल साउथ के कम मजदूरी वाले देश अब ऐसी अनेक आर्थिक गतिविधियों का मुख्य ठिया बन जाएंगे, जो पहले विकसित दुनिया या वैश्विक उत्तर में अपना ठिया बनाए रही थीं। उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरह का पुनर्स्थापन, दक्षिण में पिछड़ेपन और गरीबी को मिटा देगा। बहरहाल, इस दलील की एक स्वत:स्पष्ट समस्या यह थी कि किसी वैश्विक व्यवस्था के संबंध में कुछ भी सदा-सदा के लिए वैध मानकर नहीं चला जा सकता है। इस तरह की व्यवस्थाएं साम्राज्यवाद द्वारा गढ़ी जाती हैं और जैसाकि अब स्वत:स्पष्ट है, साम्राज्यवाद उन्हें अपनी मर्जी से कभी भी बदल सकता है। लेकिन, जब साम्राज्यवाद ऐसी किसी मौजूदा व्यवस्था से अपने पांव पीछे खींचता है, उसके शिकंजे में फंसे भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, खुद को उसमें से निकाल पाना मुश्किल होता है।
जब कोई देश व्यापार निर्भर हो जाता है, उसके व्यापार में कोई भी खलल पडऩे से, उस पर भारी चोट पड़ती है। इसलिए, जब तक वह देश अपनी आर्थिक व्यवस्था में एक बड़ा पुनर्संयोजन करने के लिए तैयार नहीं होता है, साम्राज्यवाद जब भी खुल्लखुल्ला दादागीरी करे, वह उसके सामने समझौता करने को तत्पर होता है। दूसरी ओर ऐसे किसी भी पुनर्संयोजन का बड़े पूंजीपति वर्ग और शहरी उच्च मध्य वर्ग द्वारा विरोध किया जाएगा, जो नव-उदारवादी निजाम के मुख्य लाभार्थी रहे हैं। इसलिए, कोई भी सरकार जो मुख्यत: इसी तबके के हितों की चिंता करती हो, वह तो साम्राज्यवाद की दादागीरीभरी मांगों के सामने समर्पण ही करने के लिए तत्पर होगी।
समर्पण का ख़तरा
एक उदाहरण से यह बात साफ हो जाएगी। ट्रंप की टैरिफ की धमकी से रुपया पहले ही कमजोर हो गया है। जैसे-जैसे बढ़े हुए टैरिफ लागू होंगे, रुपए का मूल्य और गिरेगा, बशर्ते पूंजी नियंत्रण लागू नहीं कर दिए जाएं। और इसके अलावा व्यापार नियंत्रण भी लागू करने होंगे, ताकि विदेशी विनियम के मोर्चे को संभाला जा सके। इस सबका अर्थ होगा, नव-उदारवादी निजाम से पीछा छुड़ाना और उसकी जगह एक वैकल्पिक आर्थिक निजाम लाना। लेकिन, बड़ा पूंजीपति वर्ग, जो वैश्वीकृत वित्तीय पूंजी के साथ एकीकृत हो चुका है, इसका प्रतिरोध करेगा और उसके हितों के प्रति प्रतिबद्ध सरकार ऐसे किसी विकल्प की बात सोचेगी भी नहीं। इसके बजाए उसके तो साम्राज्यवादी दादागीरी के सामने समझौते ही करने की ज्यादा संभावनाएं हैं।
इसका अर्थ यह है कि साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता, एक नव-उदारवादी नीति पर चले जाने के बुनियादी तौर पर ही खिलाफ है, जैसा कि 1990 की पल्टी से पहले, एक के बाद एक आयी भारत की सरकारों ने पहचाना था। नव-उदारवाद के अपनाए जाने ने, देश की स्वतंत्रता पर सीमाएं लगा दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप दादागीरी झाड़ने के पैंतरे, इस बात को बिल्कुल साफ करने का ही काम करते हैं।
(लेखक दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आर्थिक अध्ययन एवं योजना केंद्र में प्रोफ़ेसर एमेरिटस हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
मूल रूप से अंग्रेज़ी में प्रकाशित इस आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें–
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।