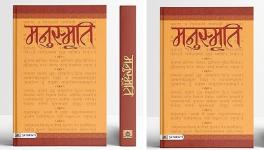विचार: एक समरूप शिक्षा प्रणाली हिंदुत्व के साथ अच्छी तरह मेल खाती है

स्वतंत्र भारत में शिक्षा से सिर्फ छात्रों को ज्ञान व कौशल मुहैया कराने की ही अपेक्षा नहीं थी बल्कि उससे एक अनगढ़ संज्ञा का सहारा लें तो ‘राष्ट्र निर्माण’ की प्रक्रिया को सुगम बनाने की भी अपेक्षा थी। ‘भारतीय राष्ट्र’ की अवधारणा, हालांकि अपने बीज रूप में तो इससे पहले भी रही थी (जिसकी शुरूआत अमीर खुसरो की रचनाओं में देखी जा सकती है), लेकिन ये अवधारणा चलन में तो भारत के उपनिवेश विरोधी संघर्ष के दौरान ही आयी थी। इसलिए, शिक्षा की राष्ट्र निर्माणकारी भूमिका सबसे पहले तो इस संघर्ष के प्रति सचेतता का ही तकाजा करती है। और यह इसका तकाजा करता है कि औपनिवेशिक शासन में भारत की दशा से परिचय हो और उस राज में भारत की जनता के शोषण की सच्चाइयों की जानकारी हो। इस सबसे परिचय, सिर्फ ह्यूमैनिटीज तथा समाज विज्ञानों के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि यह परिचय तो सभी छात्रों का होना चाहिए, जिसमें प्राकृतिक विज्ञानों तथा इंजीनियरिंग के छात्र भी शामिल हैं। तभी यह शिक्षा, एंटोनियो ग्राम्शी द्वारा प्रयुक्त संज्ञा का सहारा ले तो स्वतंत्र भारत की जनता के ‘आवयविक बुद्घिजीवी’ पैदा कर पाएगी।
इसलिए, ऐसे ‘आवयविक’ बुद्घिजीवियों का निर्माण अनिवार्यत: ऐसी पाठ्यचर्या तथा पाठ्य अंतर्वस्तु की मांग करता है और सिर्फ उच्च शिक्षा में ही नहीं, शिक्षा के आरंभिक स्तर पर भी उनकी मांग करता है, जो विकसित देशों की तुलना में, भारत में अलग हों। मिसाल के तौर पर विकसित देशों में तो शिक्षा में उपनिवेशीकृत जनगणों पर उपनिवेशवाद द्वारा थोपी गयी वंचनाओं का शायद ही कोई जिक्र होता है। वास्तव में, जाने-माने ब्रिटिश वैज्ञानिक, जे डी बर्नाल का तो मानना था कि भारत जैसे देशों में प्राकृतिक विज्ञानों में भी खास अपनी ही पाठ्यचर्या तथा पाठ्यवस्तु होनी चाहिए और उन्हें विकसित दुनिया की नकल नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर भारत की बीमारियों के प्रोफाइल की प्रकृति को देखते हुए, भारतीय डाक्टरों की चिकित्सकीय शिक्षा अपने जोर में, मिसाल के तौर पर ब्रिटेन से भिन्न होनी चाहिए। और यह इस तथ्य के अलावा है कि भारतीय डाक्टरों को भी उपनिवेशवाद और उपनिवेशविरोधी आंदोलन के संबंध में जानकारी होनी चाहिए।
इसका अर्थ यह है कि अगर भारत जैसे देशों में शिक्षा को सचमुच अपना उद्देश्य पूरा करना है, तो उसकी अंतर्वस्तु को, विकसित देशों से भिन्न होना चाहिए। यह कहने का आशय यह कतई नहीं है कि भारत में, मिसाल के तौर पर भौतिकी या रसायनशास्त्र या गणित की बुनियादी प्रस्थापनाएं पढ़ाई ही नहीं जानी चाहिए। यह कहने का आशय सिर्फ इतना है कि उन्हें एक ऐसी पाठ्यचर्या के दायरे में संयोजित किया जाना चाहिए, जो विकसित देशों में जो पढ़ाया जाता है, उसकी अनुकृति नहीं हो। और यह ऐसा विचार है जिसे लंबे अरसे से भारत में अकादमिक हलकों में आमतौर पर स्वीकृति हासिल रही है।
ये भी पढ़ें: ओडिशा: रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न-आय वाले परिवारों के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित
बहरहाल, नवउदारवाद के आने के साथ हम इससे ठीक उल्टा ही होते देख रहे हैं। दुनिया भर में अपने पांव पसार रहे बहुराष्ट्रीय निगमों को ऐसे कार्मिक चाहिए, जिन्हें एक देश से दूसरे देश, दुनिया में कहीं भी भेजा जा सकता हो। और उनके कार्मिकों की स्थानांतरणीयता के प्रश्न के अलावा देशों के आर-पार पूंजी की गतिशीलता के लिए भी ऐसे वातावरण की जरूरत होती है, जो अलग-अलग मेजबान देशों में होते हुए भी एकरूप हों। और इसमें इन बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों की प्रवृत्तियों तथा बौद्धिक संरचना की एकरूपता भी शामिल है। संक्षेप में यह कि वैश्वीकृत पूंजी के लिए, अपने कारकून भर्ती करने के लिए, ऐसे शिक्षित मध्यवर्ग की उपस्थिति आदर्श होगी, जो हर जगह जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, एक जैसा हो और अपने नजरियों में विकसित दुनिया के विचारों के जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करीब हो।
इसलिए, उसकी इसमें गहरी दिलचस्पी है कि तमाम देशों में एक एकरूप शिक्षा प्रणाली हो, जो उसके लिए एक जैसे संभावित रंगरूट और उसके लिए सामाजिक समर्थन आधार पैदा कर सके। नवउदारवाद, भारत जैसे देशों में ठीक इसी का अनुकरण होते देखना चाहता है और मोदी सरकार की नयी शिक्षा नीति, ठीक यही करने की कोशिश करती है।
शिक्षा का ऐसा एकरूपीकरण, प्राचीन भारत की तथाकथित ‘महानता’ पर, प्राचीन काल के भारतीय विज्ञान तथा गणित के चमत्कारों पर, इस या उस खास क्षेत्र योगदानों (तमाम इस्लामी योगदानों को छोडक़र) पर और मध्यकालीन भारत में हिंदुओं के कथित उत्पीड़न पर, हिंदुत्व के जोर से भी बखूबी मेल खाता है।
आखिरकार, इनमें से कोई भी औपनिवेशिक दौर को या उपनिवेशवाद द्वारा हिंदू तथा मुसलमान, सभी भारतीयों के समान रूप से किए जाते रहे शोषण को नहीं छूता है। यह शोषण, इस देश के इससे पहले के तमाम ऐतिहासिक अनुभव से पूरी तरह से भिन्न था क्योंकि इसके तहत भारत से संपदा का ‘निकास’ हो रहा था और भारत के दस्तकारों का निरुद्योगीकरण हो रहा था। इन दोनों ने ही मिलकर, यहां आधुनिक जन-दरिद्रता पैदा की थी।
इस तरह भारत में, पाठ्यचर्या तथा पाठ्यवस्तु का ऐसा रूपांतरण, जो खास भारत की हिंदुत्ववादी विचारधारा का तड़का लगाकर, उन्हें विकसित दुनिया के विश्वविद्यालयों की पौधों के रूप में, नवउदारवादी दुनिया में अन्यत्र जो भी पढ़ाया जाता है, उसके आधार पर ढाल दे, मोदी सरकार के एजेंडा में पूरी तरह से फिट बैठता है। यह वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में उस कार्पोरेट-हिंदुत्व गठजोड़ का समकक्ष है, जिसका इस समय भारतीय राजनीति में बोलबाला है। कार्पोरेट तत्व, जो वैश्वीकृत पूंजी के साथ खुद को जोड़ चुका है, शिक्षा के ऐसे एकरूपीकरण को खुशी-खुशी मंजूर कर रहा है, जो उपनिवेशवाद तथा उपनिवेशवादी शोषण के प्रभावों की सारी चर्चा को मिटाता है और पूंजीवाद को कमोबेश एक स्वत: संपूर्ण व्यवस्था की तरह देखता है। दूसरी तरफ, हिंदुत्ववादी तत्व तो शाबाशी के ऐसे टुकड़ों पर ही खुश हैं, जो प्राचीन भारत की तथाकथित ‘महानता’ को स्वीकार करने के रूप में उनकी ओर फेंके जाते हैं।
पाठ्यचर्या तथा पाठ्यवस्तु के इस एकरूपीकरण को, जिसकी अभिव्यक्ति प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएं खोलने के लिए पटाने में भी होती है (वैसे इस मुहिम की शुरूआत भी कोई मोदी सरकार ने नहीं की है बल्कि इसकी शुरूआत तो यूपीए-द्वितीय में ही कर दी गयी थी, जो उसके नवउदारवादी नजरिए के अनुरूप ही था), यह दलील देकर उचित ठहराने की कोशिश की जाती है कि इससे भारतीय विश्वविद्यालय ‘विश्वस्तरीय’ बनेंगे। लेकिन, यह दलील ही गलत है। यह दलील सबसे पहले तो इसीलिए गलत है कि ‘विश्वस्तरीय’ की इस अवधारणा को स्वीकार करना और इस लक्ष्य को हासिल करने के हिसाब से अपने विश्वविद्यालयों में कमतर व्यक्त करना, अपने आप में विकसित दुनिया के विश्वविद्यालयों के वर्चस्व को स्वीकार करना है। ऐसा इसलिए है कि इस ‘विश्वस्तरीयता’ के मानदंड भी, खुद विकसित दुनिया द्वारा ही गढ़े गए हैं। जिन तथाकथित ‘‘रैफ्रीड जर्नल्स’’ में छापे जाने को ‘विश्वस्तरीयता’ का पैमाना माना जाता है, वे भी मुख्यत: विकसित दुनिया में ही स्थित हैं और वे औपनिवेशिक शोषण के जिक्र तक से बचते हैं, आदि, आदि। जाहिर है कि लक्ष्य तो यह होना चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालय सचमुच ‘राष्ट्र निर्माण’ की जरूरतें पूरी करें, न कि तथाकथित ‘विश्वस्तरीयता’ के पीछे भागते रहें।
ये भी पढ़ें: चर्चा में नई किताब 'भारत के प्रधानमंत्री'
जाहिर है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि उच्च शिक्षा की हमारी अधिकांश संस्थाओं की जो दयनीय स्थिति है, उसकी तरफ से हम अपनी आंखें ही मूंद लें। लेकिन, उनकी गुणवत्ता को हमारे अपने ही पैमानों पर नापा जाना चाहिए और उनमें सुधार ऐसे रास्ते पर होना चाहिए, जिसके लिए हमारी शिक्षा प्रणाली के ‘राष्ट्र निर्माण’ के लक्ष्य का ही त्याग नहीं करना पड़े।
दूसरे, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की नकल करना तो, गुणवत्ता हासिल करने का भी कोई तरीका नहीं है। हॉर्वर्ड, ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज की नकल करने में हमारी संस्थाएं, हमेशा-हमेशा मिडियॉकर रहने को ही अपनी नियति बना लेंगी। इससे भी बड़ी बात यह कि यह प्रक्रिया हमारी समूची शिक्षा प्रणाली को ही मीडियॉकर बनने के लिए अभिषप्त कर देगी। हमारी संस्थाओं के पास तो, जो आम तौर पर सार्वजनिक संस्थाएं ही हैं, ऐसी फैकल्टी तथा सुविधाएं हासिल करने के लिए भी संसाधन नहीं हैं, जिनकी विदेशी विश्वविद्यालयों से, दूर-दूर तक भी तुलना की जा सकती हो। ऐसे माहौल में जब विकसित दुनिया के विश्वविद्यालयों को मॉडल माना जा रहा होगा, यह एक एहसास-ए-कमतरी ही पैदा करेगा, जो उनके ऐसी बुनियादी रोजमर्रा की जरूरत की शिक्षा मुहैया कराने में भी आड़े आएगा, जो अन्यथा उन्होंने मुहैया करायी होती। दूसरी ओर, जिन संस्थाओं के पास विदेशी विश्वविद्यालयों के तुलनीय फैकल्टी को लुभाने तथा ढांचागत सुविधाएं जुटाने के लिए संसाधन होंगे भी, उनकी फैकल्टी में से बेहतरीन हिस्सा लगातार विदेशी विश्वविद्यालयों की ओर पलायन कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर किसी के पास अगर येल विश्वविद्यालय की फैकल्टी तक पहुंचने या विदेश में किसी ऐसी संस्था की फैकल्टी तक पहुंचने का भी कोई मौका होगा, जिसको माध्यम बनाकर आगे चलकर येल तक तक पहुंचने का कोई मौका बन सकता हो, तो वह तीसरी दुनिया की किसी ऐसी संस्था में क्यों पड़ा रहेगा, जो येल की नकल करने की कोशिश कर रही हो?
दूसरे ढंग से कहें तो, पाठ्यचर्या तथा पाठ्यवस्तु के अर्थ में शिक्षा का एकरूपीकरण, अनिवार्य रूप से छात्रों की पृष्ठभूमि का (मुख्यत: मध्यवर्गीय) और कार्य-प्रेरणाओं का भी, एकरूपीकरण करता है। अपनी क्षमताएं ऐसी व्यवस्था को समर्पित करने की आकांक्षा की जगह, जो सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं में आम लोगों के बच्चों को प्रशिक्षण देकर, उन्हें अपना योगदान देने के लिए तैयार करे, उन मूल संस्थाओं तक पहुंचने की लालसा ले लेगी, जिनकी प्रतिलिपि बनने की आकांक्षा लेकर घरेलू शिक्षा संस्थाएं चल रही होंगी।
इसलिए, अगर भारत जैसे देशों में ऐसी शिक्षा संस्थाओं को खड़ा किया जाना है, जिनकी सिर्फ ‘राष्ट्र निर्माण’ के लिए ही नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण अकादमिक माहौल मुहैया कराने के लिए भी कोई सार्थकता होगी, तो उन्हें दूसरे देशों में स्थित संस्थाओं की पाठ्यचर्या, उनके कार्य-प्रोत्साहनों तथा नजरिए की नकल करने के दबाव में आने से बचकर चलना होगा, चाहे यह दबाव कितनी ही प्रतिष्ठित संस्था की नकल करने का क्यों न हो। शिक्षा की जड़ें देश के यथार्थ में होना जरूरी है वर्ना वह दोयम दर्जे की बनकर रह जाती है।
ऐसे में भारतीय समाज की अपनी विशिष्टता से जुड़ी समस्याएं, मिसाल के तौर पर जातिवादी उत्पीडऩ की समस्या, अकादमिक नजर से ही बाहर कर दी जाएंगी क्योंकि वैश्वीकृत पूंजी के लिए ऐसी समस्याओं का कोई खास महत्व ही नहीं है और हिंदुत्ववादी पलटन के लिए तो वैसे भी ये ऐसी चीजें हैं जो भारतीय सभ्यता की ‘महानता’ को कमतर बनाती हैं और जिन्हें बुहार कर दरी के नीचे छुपा देने में ही समझदारी है।
यह कोई संयोग ही नहीं है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समूचे दस्तावेज में, जाति का शायद ही कोई जिक्र आता है, न तो भारतीय समाज की एक जघन्य विशेषता के रूप में और न ही ऐसी सच्चाई के रूप में जिससे निपटने के लिए विश्वविद्यालयों में दाखिले, नियुक्ति तथा पदोन्नति की प्रक्रियाओं में, सकर्मक कदमों की जरूरत है। यह चुप्पी भी, एकरूपीकरण का ही नतीजा है।
अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।