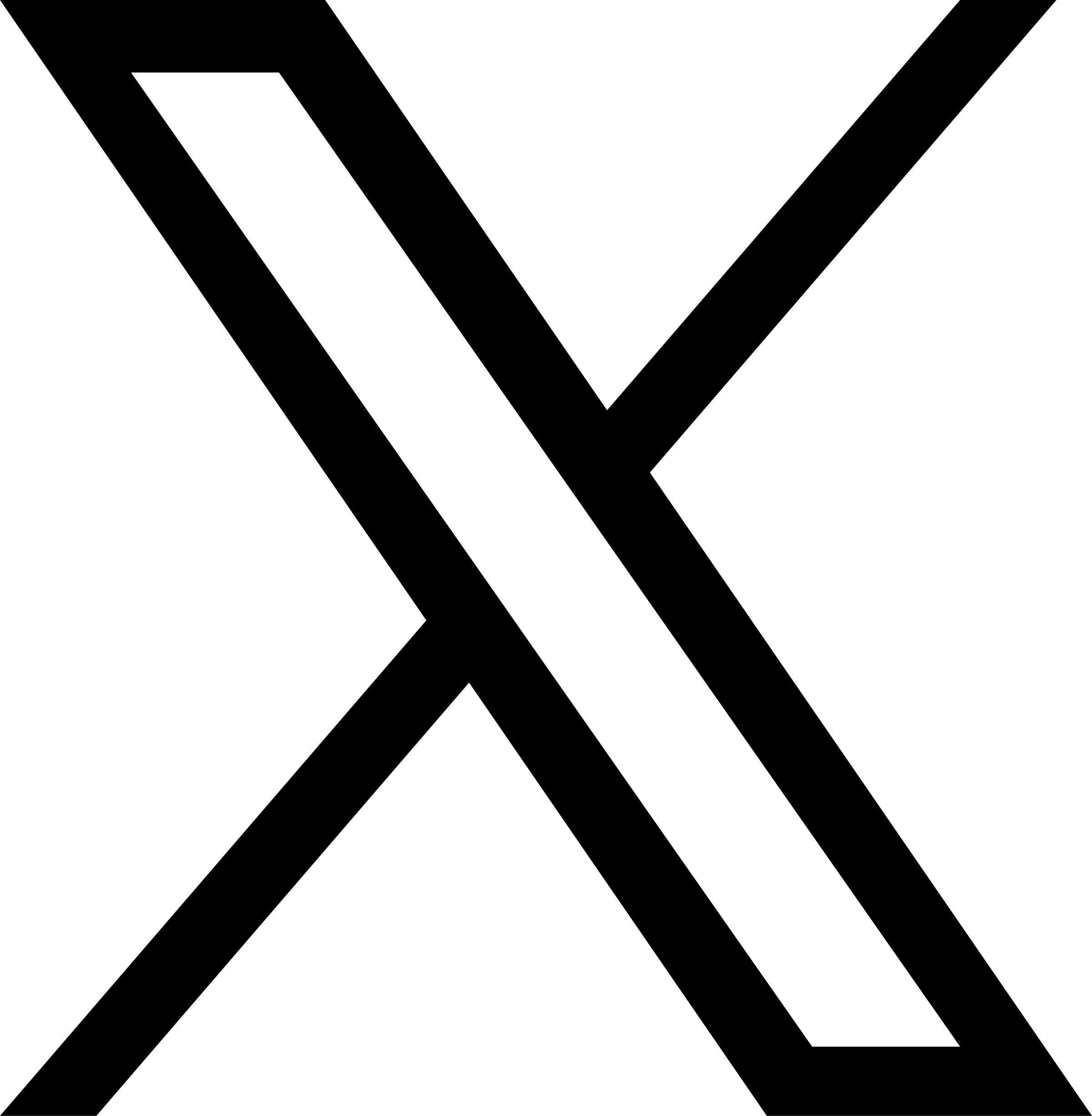महामारी से निपटने लिए युद्ध की नहीं सहकार की भाषा दरकार है

बीते 14 अप्रैल 2020 को हावर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के दूसरे चरण की संभावनाओं पर एक आंकलन पेश किया है।
इसके अनुसार इस वायरस से संक्रमण को पूरी तरह रोकने के लिए 2022 तक सोशल डिस्टेन्सिंग (मतलब दो लोगों के बीच शारीरिक दूरी, अब शब्द बदलना तो संभव नहीं रहा और उसे शब्द्श: ग्रहण किया जाने लगा है जो भारत जैसे छुआ-छूत मनाने वाले देश में बहुत गंभीर मामला बनता जा रहा है) बरतने की ज़रूरत होगी और 2024 तक इस पर बारीक निगरानी रखे जाने की ज़रूरत होगी। हालांकि इस निगरानी के गंभीर राजनैतिक मायने भी हैं लेकिन इस सूरत में कोई नागरिक इससे इंकार भी नहीं कर पाएगा।
यह अध्ययन अंतिम निष्कर्ष नहीं है लेकिन इसके उलट भी अभी हमारे सामने कुछ नहीं है। संभव है कि बहुत जल्द एक भयानक सपने की तरह यह वायरस नींद खुलते ही खत्म हो जाये और लोगों के दिमाग से उतर जाये। कुछ भी कहना अभी अंतिम नहीं है। हालांकि महामारियाँ ऐसी ही होती हैं। उनके निशान इतिहास की लंबी अवधि पर अंकित रहते हैं।
अगर हावर्ड का यह आंकलन सच होने की एक प्रतिशत भी संभावना है तो दुनिया को इस वायरस से निपटने की अपनी रणनीति बदलनी होगी। इसे युद्ध की तरह तो कम से कम नहीं लड़ा जाना होगा। ऐसे में एक लंबी अवधि के लिए कार्य-योजना दरकार होगी।
हाल ही में कोलकाता रिसर्च ग्रुप ने बॉर्डर्स ऑफ एन अपेड्मिक शीर्षक से कोविड -19 और अप्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर एक निहायत ज़रूरी सामग्री सामने लायी है। इसका संपादन रणबीर सम्मदर ने किया है। इस किताब की भूमिका में रणबीर ने बहुत ज़रूरी पहलू पर ध्यान दिलाया है कि युद्ध और महामारी से निपटना दो निहायत अलग-अलग मौजूँ हैं। जहां युद्ध की अंतिम परिणति मौतों में होती है वहीं महामारी के दौरान सारा ध्यान इंसानों की ज़िंदगियाँ बचाने में होता है।
अगर महामारी से निपटने को उससे युद्ध भी मान लिया जाता है तब भी एक पारंपरिक युद्ध और इसमें एक बुनियादी और सैद्धान्तिक अंतर है और वो है सुरक्षा का। पहले यानी दो समूहों, दो कबीलों, दो नस्लों, दो राजाओं, दो राष्ट्रीयताओं के बीच जो युद्ध मानव सभ्यता के इतिहास में हमें देखने मिलते हैं उनमें मौत एक ‘सैद्धान्तिक आधार’ है। शत्रु पर विजय पाने के लिए उसे मार देना जायज़ है। लेकिन इस ‘युद्ध’ में जीवन की सुरक्षा ही एकमात्र सैद्धान्तिक आधार है। पहले में जो भी संगठन हैं यानी सरकार, सेना, नागरिक वो सब मौत के लिए कार्रवाइयां आयोजित करते हैं जबकि दूसरे में जो भी संगठन हैं वो जीवन बचाने के लिए हर तरह की कार्रवाइयां करते हैं।
जीवन बचाने के लिए युद्ध जैसी शब्दावली अपने आप में अंतर्विरोधी है। लेकिन जैसे जीवन में बहुत विरोधाभास होते हैं यह भी हमारे जीवन का एक गंभीर विरोधाभास है शायद। अपने वजूद के एहसास के लिए क्या एक दुश्मन होना ज़रूरी ही है?
24 मार्च को रात 8 बजे जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया था तब इसकी तुलना युद्ध से की थी। ‘महाभारत’ जैसे युद्ध से। जो एक ही परिवार के बीच लड़ा गया था। उनका आशय शायद यह रहा होगा कि जब महाभारत जैसा संग्राम 18 दिन में खत्म हो गया था तब यह 21 दिन का लॉकडाउन इस कोरोना वायरस से युद्ध के लिए ज़रूर कारगर साबित होगा। हालांकि अब यह लॉकडाउन 19 दिन और आगे बढ़ाया जा चुका है। 21 दिन नाकाफी साबित हुए।
इस तुलना में या महाभारत का हवाला देने में प्रधानमंत्री यह भूल गए शायद कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों में समाप्त ज़रूर हो गया था पर इस युद्ध की समाप्ति पर कोई जीवित नहीं बचा था सिवा पाँच पांडवों और एक द्रोपदी के जो अपने वफादार कुत्ते को लेकर हिमालय के रास्ते स्वर्ग की तरफ जाते हुए वहीं खेत हो गए।
महाभारत भी एक युद्ध ही था और जिसकी बुनियादी प्रेरणा मृत्यु थी। ऐसे युद्ध मृत्यु के लिए आयोजित होते हैं। यही उनका मूल सिद्धान्त है। महाभारत चूंकि एक पौराणिक कथा है अत: इसमें समयबद्ध युद्ध भी संभव हो सका वरना मानव सभ्यता का इतिहास तो हमें यही सिखाता है कि युद्ध शुरू होने के बाद उनका खत्म होना किसी के हाथ में नहीं रह जाता। बहरहाल।
जीवन बचाने की प्रेरणा और उद्देश्य से की जाने वाली कार्यवाहियों के लिए युद्ध की बजाय किसी और रूपक की तलाश करना होगी। इस वायरस को निष्क्रिय या बेअसर करने के लिए उससे युद्ध की नहीं बल्कि उसे वश में करने की ज़रूरत है। जो काम विज्ञान करता है। विज्ञान उसे हराने की नहीं उसे वश में करने की तरकीबें तलाश कर रहा है।
इतिहास में ऐसे कई वायरसों को विज्ञान ने उन्हें समग्रता में जानकर, समझकर वश में किया है और मानव शरीर पर बेअसर बना दिया है। वायरस आज भी हैं और मानव शरीर में हैं लेकिन या तो वो मित्र बना लिए गए या उन्हें निष्प्रभावी बना दिया गया। इसके लिए युद्ध की तरह उन्माद और उत्तेजना की नहीं धैर्य और अनुशासन की ज़रूरत है। इसलिए भी यह युद्ध से नितांत भिन्न है।
महामारी अकेले नहीं आती। अपने साथ इतना कुछ लाती है जिसके असरात कई पीढ़ियों तक लोगों के जीवन के हर पहलू पर रहते हैं। आज इस महामरी के सामने दुनिया के तमाम ताकतवर देश बेबस नज़र आ रहे हैं।
विकसित देशों की स्वास्थ्य सेवाएँ सवालों के घेरे में हैं जिन्हें आज की नव –उदरवादी अर्थव्यवस्था के आक्रामक दबाव में पिछले एक –दो दशकों में कमजोर किया गया।
भारत जैसे विकासशील देशों की हालत तो और भी खराब है क्योंकि यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ 1990 में लागू हुए आर्थिक विकास के नए मॉडल में प्राथमिकता ही नहीं पा सकीं। निजीकरण के दबाव में स्वाथ्य सेवाओं को राज्य के अनिवार्य दायित्यों से हटाकर एक कमोडिटी में बदल दिया गया और निजी अस्पतालों की चेन खड़ी की गईं।
यह बहुत दिलचस्प है कि दिसंबर 2019 तक जब तक चीन में इस वायरस का असर नहीं हुआ तब तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ अर्थव्यवस्था की बलि चढ़ गईं और आज पूरी दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्थाएँ इस सार्वजनिक स्वास्थ्य पर मँडराते खतरे की बलि चढ़ रही हैं।
आज वही देश अपनी अर्थव्यवस्था भी बचा सकेंगे जो अपनी जनसंख्या के स्वास्थ्य की देखभाल ठीक से कर पाएंगे। ऐसे में दोनों को वश में करने की कवायदें तमाम सरकारों द्वारा किए जाने की ज़रूरत है।
भारत जैसे देश में दोनों ही मोर्चों पर स्थिति नाज़ुक है और अगर हावर्ड के आंकलन थोड़े ही पैमाने पर सही साबित होते हैं तो परिस्थितियाँ बहुत चिंताजनक होने वाली हैं। ऐसे में अगर युद्ध और उसके लिए ज़रूरी उन्माद की भाषा इसी तरह शीर्ष नेता की तरफ से जारी रही तो हालात और चिंताजनक होंगे।
यह ऐसी अदृश्य और अब तक अबूझ शक्ति है जिससे युद्ध करने की सलाहियतें किसी के भी पास नहीं हैं। यहाँ जनसंख्या दो भागों में बँट रही है। एक जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या संभावित हैं और दूसरी जो इससे संक्रमित नहीं हैं। परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हर कोई अपने से अलग खड़े व्यक्ति को संक्रमित मान सकता है और खुद को उससे अप्रभावित। ऐसे में हर कोई एक दूसरे की जान जोखिम में डाल सकता है।
हमें संभावित संक्रमित व्यक्ति के साथ एक मोहल्ले, एक सोसायटी, एक कार्यस्थल में रहने की काबिलियतें पैदा करना होंगीं और जो युद्ध की शब्दावली और युद्ध का वातावरण बनाने से पैदा नहीं होंगीं बल्कि इसके लिए बड़ा हृदय और निर्भय मन तैयार करने की ज़रूरत होगी।
हिंदुस्तान की 138 करोड़ जनता ने जिस परिपक्वता से लॉकडाउन का पालन अब तक किया है वो न केवल काबिले तारीफ है बल्कि इससे धीरे धीरे वो सामूहिक चेतना भी तैयार हो रही है कि खुद की सुरक्षा में ही दूसरों की सुरक्षा निहित है। अपवाद हैं। अपवाद नियमों को पुख्ता करते हैं ऐसा विज्ञान मानती है। ज़रूरत है इन अपवादों को आपराधिक नहीं बनाने की।
अप्रवासी मजदूरों की मजबूरियों को समझने की ज़रूरत है। उन्हें अपराधी बना दिये जाने की नहीं। कोरोना के अलावा जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं उनकी जरूरतों को समझने की। किसी एक धर्म या मजहब या क्षेत्र के लोगों पर सारी तोहमतें मढ़ने की बजाय ज़रूरत है उन्हें सहानुभूति देने की। यह महज़ एक बीमारी है और इसके वाहक हम सब हो सकते हैं इसलिए सबको सब में और खुद को भी देखने की।
जिन्हें अपने घरों में बैठे हुए, सड़क पर मजबूरी में आए लोगों को देखकर गुस्सा आ रहा है उन्हें यह याद रखने की ज़रूरत है जब ब्रिटिश राज में 1897 में पूना शहर में इसी तरह के संक्रामक रोग ‘प्लेग’ के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए तत्कालीन प्लेग कमिश्नर वाल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या चापेकर भाइयों (तीन भाई) ने कर दी थी। उल्लेखनीय है कि यह हत्या इस बात को लेकर की गयी थी क्योंकि वाल्टर चार्ल्स रैंड ने आपदा से निपटने के लिए शहर में आर्मी तैनात करा दी थी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि वह गुलाम भारत था।
आज इक्कीसवीं सदी में देश का हर व्यक्ति एक संप्रभु राष्ट्र का जिम्मेदार नागरिक है और जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता है। एक राष्ट्र के तौर पर इसकी तमाम सरकारों को भी उतनी ही परिपक्वता व ज़िम्मेदारी से काम लेना होगा। युद्ध की शब्दावली से बाहर निकलकर सहकार और सहयोग की साझा समझ और संयमित भाषा गढ़ने की।
(लेखक सत्यम श्रीवास्तव पिछले 15 सालों से सामाजिक आंदोलनों से जुड़कर काम कर रहे हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
इसे भी पढ़ें : क्या है ‘फंसे होने’ और ‘छिपे होने’ के पीछे की राजनीति
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।