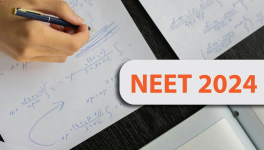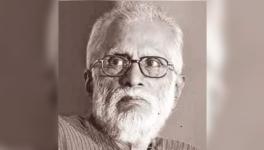“आरक्षण मेरिट के ख़िलाफ़ नहीं”, सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को ज़बानी याद करने की ज़रूरत है

आरक्षण की वजह से मेरिट खराब होती है। आरक्षण की वजह से काबिल लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन पा रहे हैं। आरक्षण पर ठीकरा फोड़ने की यह सारी बातें सवर्ण जाति के कई लोग तब से करते आ रहे हैं, जब से समाज की नाइंसाफी को दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई। नीट की व्यवस्था के अंतर्गत ली जाने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑल इंडिया कोटे के तहत 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया है। इस आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने से मेरिट खराब होता है। डॉक्टर बनने के लिए काबिल लोग डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। जनवरी के पहले हफ्ते की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तो सुना दिया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाने वाला 27% आरक्षण का कोटा संवैधानिक है। इसे खारिज नहीं किया जाएगा। लेकिन आरक्षण देने की वजह से मेरिट खराब नहीं होता है। इसके ठोस कारणों को नहीं बताया था।
20 जनवरी को सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और ए एस बोपन्ना की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आरक्षण मेरिट के खिलाफ नहीं जाता है। इसके लिए ठोस कारण भी दिए हैं। सवर्ण जाति से लेकर उन तमाम लोगों को जो आरक्षण की व्यवस्था को मेरिट के खिलाफ देखते हैं, उन्हें इन कारणों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
मेरिट की परिभाषा संकीर्ण नहीं हो सकती है। मेरिट का मतलब केवल यह नहीं हो सकता कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में किसी ने कैसा प्रदर्शन किया है। प्रतियोगी परीक्षाएं महज औपचारिक तौर पर अवसर की समानता प्रदान करने का काम करती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का काम बुनियादी क्षमता को मापना होता है ताकि मौजूद शैक्षणिक संसाधनों का बंटवारा किया जा सके।
इसे भी पढ़े: EWS कोटे की ₹8 लाख की सीमा पर सुप्रीम कोर्ट को किस तरह के तर्कों का सामना करना पड़ा?
प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रदर्शन से किसी व्यक्ति की उत्कृष्टता, क्षमता और संभावना यानी एक्सीलेंस, कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति की उत्कृष्टता, क्षमता और संभावना व्यक्ति के जीवन में मिलने वाले अनुभव, ट्रेनिंग और उसके व्यक्तिगत चरित्र से बनती है। इन सब का आकलन एक प्रतियोगी परीक्षा से संभव नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक फायदों की माप नहीं हो पाती है, जो किसी खास वर्ग की इन प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलने वाली सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी को मिलने वाले ज्यादा से ज्यादा अंक मेरिट की जगह नहीं ले सकते हैं। मेरिट को सामाजिक संदर्भों में परिभाषित किया जाना चाहिए। मेरिट की अवधारणा को इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए जो समानता जैसी सामाजिक मूल्य को बढ़ावा देता हो। समानता जैसा मूल्य जिसे हम एक सामाजिक खूबी के तौर पर महत्व देते हैं। ऐसे में आरक्षण मेरिट के खिलाफ नहीं जाता है, बल्कि समाज में समानता यानी बराबरी को स्थापित करने के औजार के तौर पर काम करता हुआ दिखेगा।
आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े कुछ जातिगत समुदायों को दिया जाता है। ऐसा मुमकिन है कि जिन समुदायों को आरक्षण दिया जा रहा है, उसके कुछ सदस्य पिछड़े ना हो। इसका उल्टा यह भी मुमकिन है कि जिन समुदायों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, उसके कुछ सदस्य पिछड़े हो। लेकिन कुछ सदस्यों के आधार पर समुदायों के भीतर मौजूद संरचनात्मक नाइंसाफी के सुधार के लिए दी जाने वाली आरक्षण की व्यवस्था को खारिज नहीं किया जा सकता है।
कहने का मतलब यह नहीं है कि प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत अधिक मेहनत और समर्पण करने के बाद ही कोई प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो पाता है। उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला ले पाता है। लेकिन मेरिट का विचार बदलना चाहिए। मेरिट या योग्यता या काबिलियत में केवल किसी व्यक्ति की निजी मेहनत और समर्पण की भूमिका नहीं होती है। जिस तरह की बहस मेरिट को लेकर की जाती है, उसमें परिवार, स्कूल, धन सांस्कृतिक पूंजी की भूमिका छिपा दी जाती है। मेरिट को लेकर इस तरह की बहसों की वजह से उनकी गरिमा को ठेस पहुंचता है, जिन्होंने खुद को बेहतर बनाने के लिए वैसी बाधाओं का सामना किया जो बाधाएं समाज में उनकी वजह से नहीं बनी है।
मेरिट की संकीर्ण परिभाषा समाज को व्यापक समानता का अर्थ समझा पाने में बाधक बनती है। इसलिए मेरिट की पूरी अवधारणा का बदलना जरूरी है। केवल प्रतियोगी परीक्षा में मिलने वाले अंक मेरिट नहीं कहला सकते हैं। मेरिट को इस तरह से परिभाषित करना पड़ेगा जैसे वह समाज की गैर-बराबरी को दूर करने का औजार बन सके। मेरिट की परिभाषा वैसी नहीं हो सकती जिसे सामाजिक तौर पर बराबरी हासिल करने के लिए महत्व नहीं दिया जा सके। यहां यह समझने वाली बात है कि समानता या बराबरी स्थापित करने का मतलब केवल इतना नहीं है कि उन तरीकों को अपना लिया जाए जिससे भेदभाव को दूर किया जा सके, बल्कि समानता स्थापित करने में हर एक व्यक्ति का मूल्य, गरिमा और उसका सम्मान भी शामिल है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5), अनुच्छेद 15(1) के अपवाद नहीं हैं, बल्कि अनुच्छेद 15(1) में निर्धारित व्यापक समानता या तात्विक समानता या अंग्रेजी में सब्सटेंटिव इक्वलिटी कह लीजिए, इसको हासिल करने के लिए अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 15 (5) की मौजूदगी है। सरल शब्दों में समझें तो यह कि अनुच्छेद 15(1) राज्य को केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग, जन्म, स्थान या इनमें से किसी के आधार पर अपने नागरिकों के साथ भेदभाव करने से रोकता है। लेकिन अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) के जरिए कानून बनाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को राज्य के जरिए दिया जाने वाला आरक्षण समुदायों के बीच मौजूद भेदभाव को दूर कर समानता स्थापित करने का तरीका है।
इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट को लेकर के जो बातें कहीं हैं, उन बातों को उन तमाम लोगों को नोट कर के रख लेना चाहिए जो मेरिट के तौर पर केवल परीक्षा में मिलने वाले अंको को देखते हैं। व्यक्ति के इर्द-गिर्द बनी हुई सामाजिक सहयोग और असहयोग की भूमिका को नहीं आंक पाते। हर परीक्षा के रिजल्ट के बाद आरक्षण को मेरिट खराब करने का दोष देते हुए पाए जाते हैं।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।