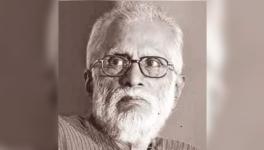हमारी मनचाही जीवनशैली में हिंदी जैसा कुछ भी नहीं
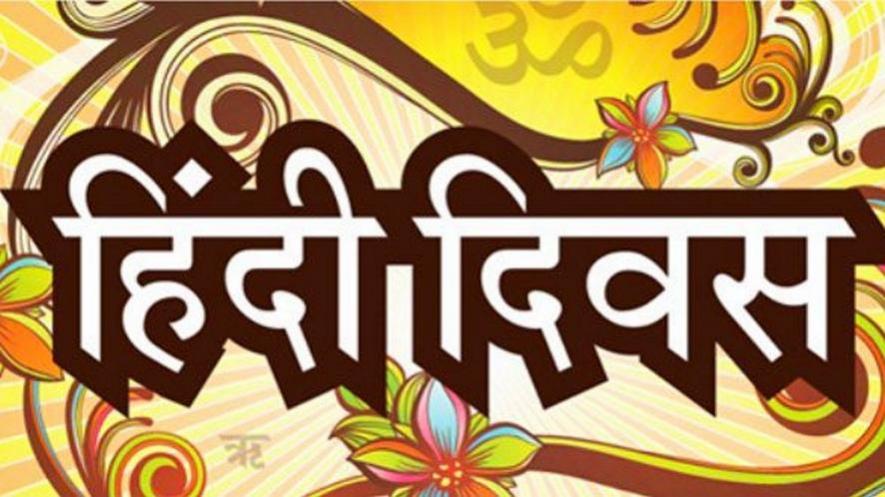
हिंदी को लेकर चिंता करना या खुशी जताना हिंदी को भी पसंद नहीं होगा। भाषाओं का अस्तित्व संस्कृतियों पर निर्भर करता है और संस्कृतियां तालाब की तरह रुकी नहीं होतीं बल्कि नदी की तरह बहती रहती हैं। इस बहाव के लिए भाषा पर चिंता या खुशी जताने की जरूरत नहीं बल्कि इसके लिए संस्कृतियों की पूरी की पूरी रूपरेखा जिम्मेदार होती है। इसलिए हिंदी दिवस पर हिंदी को बचाने या बढ़ावा देने की बातों की बजाय इस पर बात करनी चाहिए कि भाषाओँ के संदर्भ में हिंदी का महत्व क्या है ? यह कैसे हमें और हमारे समाज को रच रही है? इसके छूटते हुए साथ को संभाला जा सकता है या यह केवल हमारा भ्रम है।
एक तरफ हिंदी अंग्रेजी जैसी भाषा की हैसियत से हाशिये पर जाती हुई लगती है तो दूसरी तरफ भारत के लोकप्रिय मतों के बीच राष्ट्रभाषा का तमगा हासिल करने की वजह से भारत के अन्य भाषाओं और बोलियों को हाशिये की तरफ धकेलती है।
मौजूदा दौर में भारत में अंग्रेजी के दबदबे ने हिंदी को नेपथ्य में धकेल दिया है। कई हिंदी बोलने वालों को लगता है कि वह हिंदी को बचाने का काम कर रहे हैं। हिंदी दिवस के कई आयोजनों में दिए जाने वाले चीखते पुकारते भाषणों में दम तोड़ती हिंदी का बेदमपन देखा जा सकता है। पूरे विश्व की जीवनशैली अपने मूल को छोड़कर जब एक खास तरह के जीवनशैली को अपनाने की लड़ाई लड़ रही हो, उस समय भाषाओं को बचाने के लिए गला फाड़ना बेईमानी लगता है। लेकिन इस बात के साथ एक सच्चाई यह भी है कि कोई भी जीवनशैली अपने मूल रूप में हमेशा मौजूद नहीं रहती है ,वह समय के सफर में बदलती रहती है। जैसे कि आज से पचास साल पहले जो भारत की जीवनशैली थी, वह आज नहीं है और आज वाली जीवनशैली, आज के पचास साल बाद नहीं रहेगी। इसलिए हिंदी के ढंग में होने वाले बदलाव को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है वह भी बदलती रहेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि हिंदी के ढंग में बदलाव नहीं हो रहा है बल्कि बदलाव के बजाय हिंदी ढलान पर जाते हुई लग रही है। एक ऐसी नदी के तौर पर दिख रही है, जिसके फैलाव का इलाका कम हो रहा है, धार मंद हो रही है और भविष्य सूखता नजर आ रहा है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे समाज की अधिकांश विद्वता अब हिंदी में नहीं रची जाती। अपने खानसामे से लेकर ड्राइवर तक से वह हिंदी में तो बात करती है लेकिन वह अंग्रेजी में सोचती और अंग्रेजी में लिखती है। ज्ञान के सभी क्षेत्रों की पढ़ाई लिखाई अब अंग्रेजी में होती है। ऐसा हो सकता है कि शुरुआती पढ़ाई लिखाई हिंदी में हो लेकिन उच्चतम स्तर की पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में ही होती है। इसलिए ज्ञान उत्पादन की भाषा हिंदी के बजाय अब पूरी तरह से अंग्रेजी बन चुकी है। समाजशास्त्र से लेकर अर्थशास्त्र तक मानविकी से लेकर विज्ञान तक सभी के शोध पर सोचने, विमर्श करने और रिसर्च पेपर लिखने की भाषा अंग्रेजी है। इस तरह से ज्ञान उत्पादन की भाषा न होने की वजह से हिंदी के नदी के फैलाव का इलाका खुद ही कम हो गया है।
अब चूँकि ज्ञान उत्पादन की भाषा अंग्रेजी है इसलिए समाज में रोजगार पाने और मनचाही जीवनशैली अपनाने की भाषा अंग्रेजी बन चुकी है। अगर हम वेटर से क्लर्क और डॉक्टर से लेकर कलक्टर बनना चाहते हैं तो हिंदी अपनाने से हम औरों के मुकाबले बहुत पीछे हो जाते हैं तो हम हिंदी क्यों अपनाये। अगर हमारे आर्थिक मॉडल ने हमें रोजगार की तलाश में हमें शहरों की तरफ धकेल दिया है, जहां भाषा बचाने से ज्यादा जरूरी जीने की चिंता है तो हिंदी जैसी बातों की चिंता किसे हो। हमारी अनंत चिंताओं का हल अगर विज्ञान अपनी तकनीक से कर दे रहा है और विलासिताओं के मोह में धकेल देने की मद्दा रखता है तो उस भाषा की जरूरत पैदा होती है, जिसमें विज्ञान रचा जाता है, न कि हिंदी कि जिसने विज्ञान के बारें में सोचना ही बंद कर दिया है। इन सारे जरूरी हिस्सों से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की गैरमौजूदगी लेकिन भारतीय राजनीति में जनता से संवाद करने में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की मौजूदगी ने भारत में एक अजीब सा समाज रचा है। जहां के नेताओं के भाषणों और आम जनता की बातचीतों से जरूरी हिस्सा गायब होता जा रहा है। जनता और सरकार के बीच का संवाद लफ्फाजियों और जुमलों से भरा पड़ा है। सब यह सोचने और मानाने लगे हैं कि भाषणों और आम जनता की बातचीत का मुद्दा गंभीर नहीं होना चाहिए, वही होना चाहिए जो जनता सुनना चाहती है, वही होना चाहिए, जिसमे रस हो, मनोरंजन हो, जो बातूनी हो लेकिन जिसमें बात न हो। इसकी सबसे बड़ी गवाही हमारा आज का मीडिया प्रतिष्ठान देता है। जैसे कि जिस गंभीरता की मौजूदगी हमें अंग्रेजी मीडिया में मिलती है,वह हिंदी मीडिया से पूरी तरह गायब हो चुकी है।
अंग्रेजी ने जिस तरह से हिंदी को दबाया है, ठीक इसी तरह हम हिंदी की महिमामंडन और राष्ट्रभाषा के तौर पर पुकारते समय भारत की अन्य भाषाओं को दबाते हैं। ठीक इसी तरह भारत की राजभाषाएँ बोलियों को दबाती हैं। भाषाओं के संदर्भ में दबाना फिर भी बहुत नरम अभिव्यक्ति है क्योंकि भाषाओं के दबने से संस्कृतियां बदलती हैं और जीवनशैलियां मरती हैं। हिंदी की वजह से एक आम भारतीय केवल उत्तर भारत को देश समझने लगता है और हिंदी से इतर जुबान बोलने वाले को दूसरा देशी समझने लगता है। एक भाषाविद् इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि आज इस देश में हिंदी भाषा अंग्रेजी की दासी ,अन्य भारतीय भाषाओं की सास और अपनी ही दर्जनों बोली या उप भाषाओं की सौतली मां बन गयी है। लेकिन यह बात उन्हें नहीं समझ में आएगी जो गला फाड़ फाड़कर एक देश, एक भाषा और एक धर्म की बात करते हैं। इस तरह से बात करने वाले भारत का क्या किसी भी देश के नागरिक नहीं हो सकते। लेकिन विडंबना यह है कि इस सोच से चले वाले आज भारतीय सरकार के कर्ता धर्ता हैं।
अब यह सवाल उठता है कि क्या हिंदी के इस ढलान या अन्य भारतीय भाषाओं के ढलान को रोका जा सकता है। इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। सरकारी हिंदी मठाधीशी की तरह काम करती है। इसमें ऐसी पंडिताई की भरमार है, जिसकी जटिलता किसी को भी न भाए और न किसी को समझ में आये। और भाषा जब सरल, सहज और सरस होने से अलग एक दूसरी दुनिया की चीज लगने लगती है तो भाषा मरने लगती है। अब उत्तर प्रदेश में नियम है कि यहां के कल कारखानों में मजदूरों के लिए बने नियम को दिवारों पर चिपकाना जरूरी है लेकिन दिवारों पर चिपके नियम की भाषा ऐसी होती है जिसे मजदूर तो क्या हिंदी भाषी विद्यार्थी भी न समझ पाए। इस तरह की सरकारी हिंदी तो ऐसी लगती है कि जैसे वह हिंदी के बहाव को रोकने का काम कर रही हो। इसके बाद अनुवादों की बारी आती है। सरकारी अनुवाद इतने बेढंगे होते हैं कि ढंग से पढ़ा लिखा आदमी भी उसे पढ़ते समय बेढंगा हो जाए। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से प्रकाशित होने वाली सरकारी किताबें जैसे कि सालाना प्रकाशित होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण की किताबें इसका जीता जागता उदाहरण हैं।
इस सबके बावजूद सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की मौजूदगी की वजह से हिंदी में कुछ नया होता दिख रहा है। सब लेखक बन चुके हैं। और हिंदी का बेतरतीब लेकिन सुंदर विस्तार हो रहा है। चूँकि आम जनता के सरोकारी मुद्दों का दायरा बहुत फैला हुआ नहीं होता है इसलिए सोशल मीडिया की वजह से हिंदी की जो लोकप्रियता बढ़ी है, वह जनसरोकारी मुद्दों तक ही सीमित है। लेकिन डिजिटल मीडिया की वजह से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का जो भी फैलाव हो रहा है, वह हिंदी नदी के कम इलाके में बहाव को फैलाता नहीं है लेकिन इस तरफ इशारा तो जरूर करता है कि इस नदी का बहाव हमेशा जारी रहेगा।
अब सवाल उठता है कि क्या हिंदी को संभाला जा सकता है या यह केवल हमारा भ्रम है। पत्रकार सोपान जोशी इसका बहुत सुंदर जवाब देते हैं। वह कहते हैं कि भाषाएं नदियों की तरह होती हैं। किसी भी जगह पर नदी का पानी किसी ऊपरी इलाके से आता है, क्योंकि पानी सदैव नीचे ही बहता है। ऊपर जाने के लिए उसे भाप बनना पड़ता है, जिसके लिए सूरज जैसे विशाल हीटर की ज़रूरत होती है।
पानी इस्तेमाल करने वाले को पता नहीं होता कि उसका पानी हिमालय के किसी हिमनद के पिघलने से आया है या किसी के खेत में गिरी बारिश के पानी का रिसाव है। वह उस पानी को अपना संवैधानिक अधिकार भी मान सकता है, या देवताओं का प्रसाद भी। लेकिन नदियों की धारा किसी संविधान की धारा से नहीं बहती, न ही बादल मौसम विभाग के नीति निर्धारण या श्वेत पत्र की बाट जोहते हैं, बरसने के लिए। उनका धर्म सूरज, तापमान, दबाव, हवाओं जैसे कारणों से तय होता है। इस तरह से अगर हमारी जीवनशैली अगर हिंदी जैसा कुछ नहीं है तो हिंदी को बचाना या बढ़ाना भी हमारे बस की बात नहीं।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।