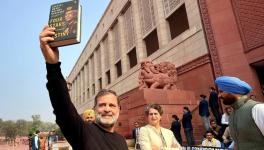जीडीपी के आंकड़े बनाम असली तरक़्क़ी

वाणिज्यवादी (mercantilists ) किसी राष्ट्र की संपन्नता को उसके पास बहुमूल्य धातुओं की मात्रा से आंका करते थे और राष्ट्र की प्रगति को उसके पास इन बहुमूल्य धातुओं की मात्रा में बढ़ोतरी से आंकते थे। इन बहुमूल्य धातुओं की अपनी इस मात्रा में बढ़ोतरी के लिए, संबंधित राष्ट्र के लिए माल तथा सेवाओं के व्यापार का संतुलन अनुकूल या बचत वाला होने यानी उसके निर्यात के आयात से ज्यादा होने की अपेक्षा होती थी और इस व्यापार बचत का निपटारा बहुमूल्य धातुओं, खासतौर पर सोने के आयात के जरिए होता था और इस तरह संबंधित देश के पास सोने की मात्रा बढ़ने की उम्मीद की जाती थी।
अपने महाग्रंथ, द वैल्थ ऑफ नेशन्स में एडम स्मिथ ने इन वाणिज्यवादियों को ही निशाना बनाया था। स्मिथ का कहना यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी व्यापार इजारा कंपनियां जो दावा करती थीं उसके विपरीत, बहुमूल्य धातुओं के भंडारों से किसी राष्ट्र की संपदा परिभाषित नहीं होती थी। इसके बजाए किसी देश के पास कितना पूंजी स्टॉक था, उससे राष्ट्र की संपदा परिभाषित होती थी। इसलिए, किसी राष्ट्र की संपन्नता पूंजी के ज्यादा से ज्यादा स्टॉक जमा करने में निहित होती है और इसके लिए सबसे अनुकूल स्थितियां बाजारों तथा पूंजी के काम-काज पर राज्य द्वारा लगायी जाने वाली सभी बंदिशों के हटाए जाने से पैदा होती हैं। यानी इसके लिए अर्थव्यवस्था में मुक्त बाजार की परिस्थितियां सुनिश्चित किए जाने की जरूरत होती है। और इसे संभव बनाने के लिए, शासन पर से ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी इजारेदाराना कंपनियों का शिकंजा खत्म किया जाना जरूरी है।
स्मिथ के रुख के संबंध में ध्यान खींचने वाली बात यह थी अपने से पहले की अवधारणा से क्रांतिकारी पथ-परिवर्तन के बावजूद, यह रुख राष्ट्र पर ही केंद्रित बना रहता है, न कि जनता पर। इसमें राष्ट्र की संपदा को एक ऐसी सत्ता माना जाता है, जो जनता से ऊपर है और जिसे अभीष्ट के तौर पर गिना जाता है। इस तरह, संपदा के रूप में किसे गिना जाना चाहिए, इसकी अवधारणा बदल जाती है और सोने तथा चांदी की जगह पर, पूंजी स्टॉक की गिनती होने लगती है, लेकिन वह सत्ता नहीं बदलती है, जिसकी संपदा की बात की जा रही होती है।
जनता से ऊपर राष्ट्र: पूंजीवादी राष्ट्रवाद
यह विचार कि राष्ट्र, जनता से अलग है और वह जनता से ऊपर है, उस पूंजीवादी राष्ट्रवाद की विशेषता था, जो वैस्टफेलियाई शांति संधियों के बाद यूरोप में विकसित हुआ था। जहां यह पूंजीवादी राष्ट्रवाद, 1930 के दशक में यूरोपीय फासीवाद के अंतर्गत अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था, यह विचार अपने आप में वह सामान्य सूत्र था, जो पूंजीवादी विचार की समूची यात्रा में समाया नजर आता है। बेशक, चूंकि राष्ट्र कथित रूप से अपनी जनता से ऊपर था, ‘‘राष्ट्रीय हित’’ की पहचान अनिवार्य रूप से पूंजीपति वर्ग के खास हिस्सों के हितों के रूप में की जाती थी।
इस प्रकार वाणिज्यवाद से एडम स्मिथ तक का बदलाव, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी इजारेदाराना व्यापारी कंपनियों के हितों की, ‘‘राष्ट्रीय हित’’ के समानार्थी के रूप में पूजा की जगह पर, उदीयमान विनिर्माता पूंजीपति वर्ग के हितों को ‘‘राष्ट्रीय हित’’ के मूर्त रूप के तौर पर स्थापित करता है। अब पूंजीपति वर्ग के इस बाद वाले हिस्से के हितों का आगे बढ़ाया जाना, राष्ट्र के हितों के आगे बढ़ाए जाने का समानार्थी बन जाता है। लेकिन, यह बदलाव करते हुए हमेशा, राष्ट्र की एक ऐसी अवधारणा पर कायम हो जा रहा था, जिसके हितों को आगे बढ़ाया जाना था और जो एक ऐसी सत्ता थी जो जनता से भिन्न थी और उससे ऊपर थी।
डेविड रिकार्डो की प्रगति की ठीक वही धारणा थी, जो एडम स्मिथ की थी और वह थी, राष्ट्र में पूंजी स्टॉक का संचय। उनका यह डर कि पूंजीवादी व्यवस्था एक अचल अवस्था की ओर चली जाएगी, जहां पूंजी संचय होना बंद हो जाएगा, ठीक इसी धारणा से निकलता था कि पूंजी स्टॉक , किसी राष्ट्र की संपदा होते हैं। उनकी नजर में पूंजी संचय के रुकने का अर्थ होगा, प्रगति का अंत।
जॉन स्टुअर्ट मिल बेशक इस लिहाज से एक अपवाद थे। वह यह कहते थे कि अचल अवस्था की परवाह करने की जरूरत नहीं है, अगर उसके अंतर्गत मजदूर उस स्थिति के मुकाबले बेहतर स्थिति में हों, जब अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय हो रहा हो। यानी स्मिथ तथा रिकार्डो जैसे अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, मिल मजदूरों के कल्याण को पूंजी के संचय के ऊपर रखते हैं। लेकिन, क्लासिकी राजनीतिक अर्थशास्त्र के रुख से इस विचलन को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि अपनी पत्नी हैरियट के प्रभाव से वह एक खास समाजवादी रुख की ओर बढ़ रहे थे।
अभीष्ट के रूप में पूंजी स्टॉक संचय
बहरहाल, अभीष्ट के रूप में, राष्ट्र की मेहनतकश आबादी की खुशहाली की जगह पर, पूंजी स्टॉक की मात्रा पर और उससे पैदा होने वाले उत्पाद की मात्रा पर ही ध्यान केंद्रित करने के लिए, स्मिथ तथा रिकार्डो जैसे क्लासिकी अर्थशास्त्रियों की ज्यादा सख्ती से आलोचना नहीं की जानी चाहिए। मजदूरों के प्रति उनकी भी काफी सहानुभूति थी, लेकिन वे यह मानते थे कि अगर उनकी माली हालत बेहतर होती है, तो मजदूर ज्यादा तेजी से संतानोत्पादन करते हैं। यह वही विचार था जिसकी अभिव्यक्ति आबादी के संबंध में माल्थस के सिद्धांत में हुई थी। उनका मानना था कि अगर वास्तविक मजदूरी, गुजारे के स्तर से बढ़ जाएगी, तो आबादी भी बढ़ जाएगी और इसलिए श्रम की आपूर्ति भी बढ़ जाएगी। और यह वास्तविक मजदूरी को वापस गुजारे के स्तर पर धकेल देगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मजदूरों की जीवन दशा में कोई भी सुधार, खुद उनके ऊपर ही निर्भर करता है। यानी अगर वे अपनी आदतें बदल लेते हैं तथा अपनी जीवन दशा में सुधार होने पर भी अपनी आबादी में बढ़ोतरी को अंकुश में रख सकते हैं, तभी वे अपनी माली हालत में हुए सुधार को बनाए रख सकते हैं। चूंकि नीति इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है, नीति का ध्यान तो कुल पूंजी स्टॉक को और इस तरह उत्पाद को बढ़ाने पर ही लगा रहना चाहिए। इससे, सब के लिए उपलब्ध कुल राशि बढ़ जाएगी और मजदूरों को इससे कहीं बड़ा हिस्सा मिल सकेगा, बशर्ते वे अपनी आदतें बदल लें।
बहरहाल, स्मिथ और रिकार्डो के मामले में हम जिस तरह की नरमी अपना सकते हैं, वैसी ही नरमी के तथाकथित ‘‘मुख्यधारा’’ के अर्थशास्त्र के साथ नहीं बरती जा सकती है। आबादी के माल्थस के सिद्धांत में विश्वास का अंत बहुत पहले ही चुका था। वास्तव में मार्क्स ने इस सिद्धांत को ‘‘मानव जाति का कलंक’’ कहा था, उससे अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध तथा उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध के विपरीत, आज कहीं ज्यादा आम सहमति होगी। लेकिन, इसके बावजूद ‘‘मुख्यधारा’’ का पूंजीवादी सिद्धांत अब भी कुल उत्पाद के स्तर को किसी ‘‘राष्ट्र’’ की खुशहाली का सूचक मानता है और उसकी वृद्धि दर को प्रगति का सूचक मानता है। चूंकि इस अर्थ में प्रगति तो पूंजीपतियों की गतिविधियों से ही हासिल की जा सकती है, इसका अर्थ यह हुआ कि ‘‘राष्ट्र’’ का बेहतरीन हित इसी में है कि पूंजीपतियों को खुश रखा जाए, उन्हें प्रोत्साहन दिए जाएं, उनके हितों को आगे बढ़ाया जाए और उनके साथ विशेषाधिकार-प्राप्त लोगों वाला सलूक किया जाए।
स्मिथ और रिकार्डो ने फिर भी, जाहिर है कि गलती से मगर यह सोचने के चलते इस तरह का रुख अपनाया हो सकता है कि जब तक मजदूर ही अपनी आदतें नहीं बदल लेते हैं, इसके सिवा और कुछ किया ही नहीं जा सकता था। लेकिन, बाद के अर्थशास्त्रियों का इस तरह का रुख अपनाना, शुद्ध विचारधारात्मक पूर्वाग्रह को ही दिखाता है।
विचारधारात्मक पूर्वाग्रह
इस पूर्वाग्रह की ताजातरीन मिसाल नीति आयोग के सीईओ की इसकी घोषणा है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अपने जीडीपी के आकार के हिसाब से उसने अब, 4 ट्रिलियन (या 40 खरब) डालर का आंकड़ा पार कर, हाल ही में जापान को पछाड़ दिया है। नीति आयोग के सीईओ ने सिर्फ चलते-चलाते यह बात नहीं कह दी। उन्होंने बाकायदा एक बड़ी भारी उपलब्धि के रूप में इसका ढोल पीटा और हैरानी की बात नहीं है कि भारत के बड़े कारोबारी हलके सदस्यों ने इसकी तारीफों के पुल बांधे हैं। बहरहाल, यह उल्लेखनीय है कि नीति आयोग के सीईओ ने इस तथ्य का जिक्र तक नहीं किया कि भारत की आबादी, जापान के मुकाबले दस गुनी से ज्यादा है। नीति आयोग के सीईओ उसी तरह इसका बखान कर रहे थे, जैसे अब से कुछ ही अर्सा पहले नरेंद्र मोदी यह कह रहे थे कि भारत का जीडीपी जल्द ही 5 ट्रिलियन (50 खरब) डालर हो जाएगा।
बहरहाल, देश के आकार के अलावा, जो हमारे देश के जीडीपी के कुल आकार की विकसित पूंजीवादी देशों के साथ तुलना पर आधारित ऐसे सभी दावों को निरर्थक बना देता है, जीडीपी पर ही ध्यान केंद्रित करना पूरी तरह से झूठे परिप्रेक्ष्य को दिखाता है। यह न सिर्फ उस पुराने परिप्रेक्ष्य पर लौटना है, जो कभी माल्थसवाद में विश्वास किया करता था, बल्कि यह एक जनतांत्रिक समाज से पूरी तरह से बेमेल भी है। जनतंत्र में जनता की दशा से ही फर्क पड़ता है और प्रगति को पूरी तरह से इसी के पैमाने से नापा जाना चाहिए कि जनता की दशा में कितना सुधार हो रहा है।
यह परिप्रेक्ष्य हमारे उपनिवेश-विरोधी संघर्ष के परिप्रेक्ष्य से भी मेल नहीं खाता है। ‘‘राष्ट्र’’ की वह अवधारणा, जिसके जीडीपी के मामले में जापान का पछाड़ देने को खुशी मनाने का मौका बताया जा रहा है, एक ऐसे राष्ट्र की अवधारणा है, जो अपनी जनता से ऊपर है, जिसकी ‘‘शानदार’’ उपलब्धि का, जनता की जीवन दशाओं से कुछ लेना-देना ही नहीं है। यह पूरी तरह से उस उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष की भावना के लिए अभिशाप है, जो साम्राज्यवादी शासन से ‘‘राष्ट्र’’ की मुक्ति को, उसकी जनता की मुक्ति का समानार्थी मानती थी।
बहरहाल, आजादी की तीन-चौथाई सदी से ज्यादा के बाद भी, न सिर्फ जनता की दशा करीब-करीब पहले जितनी ही दयनीय बनी हुई है और जिन 127 देशों के लिए वैश्विक भूख सूचकांक तैयार किया जाता है, 2024 में भारत इन देशों में से 105वें स्थान पर था। इसके ऊपर से आज देश में ऐसी सरकार है तो इस सच्चाई पर शर्मिंदा होने की जगह, देश के जीडीपी के कुल आकार को लेकर जश्न मना रही है।
(लेखक दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आर्थिक अध्ययन एवं योजना केंद्र में प्रोफ़ेसर एमेरिटस हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
मूल रूप से अंग्रेज़ी में प्रकाशित इस आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें–
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।