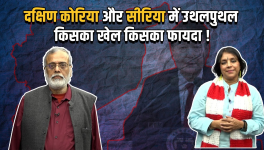अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर: अस्थायी युद्धविराम, पर शांति का रास्ता अब भी अनिश्चित

डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की 30 अक्तूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के बुसान (Busan) में हुई बैठक ने अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध में फिलहाल एक अस्थायी राहत जरूर दी है। लेकिन जब तक इस समझौते की पूरी रूपरेखा (fine print) सामने नहीं आती, यह आकलन करना कठिन है कि यह एक अस्थायी युद्धविराम संधि (temporary truce) है या वास्तव में दोनों देशों के बीच संबंध सुधार (rapprochement) की शुरुआत।
फिलहाल इस पर निर्णय आना बाकी है, और हमें बुसान में क्या हासिल हुआ, इसे समझने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा।
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल (second presidential term) की शुरुआत से ही सबसे गर्म मुद्दा उनका टैरिफ युद्ध (tariff war) रहा है — न केवल चीन के साथ, बल्कि पूरी दुनिया के साथ। अब यह केवल व्यापार नीति (trade policy) का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि यह खुद अमेरिकी विदेश नीति का चालक (driver) बन गया है।
यह कहना गलत नहीं होगा कि अब अमेरिका की राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी नीतियां भी इन टैरिफों से संचालित होती दिखती हैं।
हालांकि अमेरिका की सैन्य ताकत अभी भी दृश्य से बाहर नहीं है, लेकिन उसका ध्यान अब दो क्षेत्रों तक सीमित लगता है —
पहला, पश्चिम एशिया (West Asia) में इज़राइल को समर्थन देना, और दूसरा, मोनरो सिद्धांत (Monroe Doctrine) के तहत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन को अपने "प्रभाव क्षेत्र (sphere of influence)" के रूप में दावा करना।
1995 में बड़े धूमधाम से शुरू हुआ नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था (rule-based global order) का सपना — यानी विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization - WTO) प्रणाली — ट्रंप के दौर में फीका पड़ गया है।
उनकी नीतियों ने टैरिफों को हथियार (weaponising tariffs) में बदल दिया है — यह शीत युद्ध (Cold War) के दौर की निर्यात नियंत्रण नियमावली (export control rules) की याद दिलाती है, जो मुख्यतः सोवियत संघ के ख़िलाफ़ थी, लेकिन इसमें भारत जैसे देश भी शामिल थे।
उन्हीं नियमों को तब COCOM Rules कहा जाता था, जो सोवियत संघ के पतन के बाद Wassenaar Arrangement के रूप में बदल गए।
1995 में शुरू हुआ WTO का निर्यात-आयात तंत्र (export-import regime), जो तथाकथित रूप से "नियम-आधारित व्यवस्था" का हिस्सा था, अब बहुत कमज़ोर पड़ चुका है।
इसका विवाद निपटान ढांचा (dispute settlement mechanism) लगभग ठप है — क्योंकि अमेरिका ने इसके शीर्ष निकाय, WTO Appellate Tribunal, को ही निष्क्रिय कर दिया है।
अमेरिका ने नए सदस्यों की नियुक्ति को लगातार रोका, जिससे पुराने सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के बाद यह निकाय अब कोरम (quorum) से खाली है।
नतीजा — WTO में कोई भी व्यापार विवाद अब सुलझ नहीं पाता।
अब जो व्यवस्था बन रही है, वह पहले के तकनीकी नियंत्रण ढांचे (COCOM और Wassenaar) से भी अलग है —
क्योंकि यह पूरी तरह “Made-in-US policy” है।
अमेरिका के सहयोगियों (allies) की इसमें कोई भूमिका नहीं; उन्हें बस ट्रंप के आदेश को स्वीकार करना पड़ता है।
स्वाभाविक है कि यूरोपीय संघ (European Union) और उसके संभावित साझेदार झुक गए हैं और “सम्राट ट्रंप” के आदेशों को मानने में ही भलाई समझ रहे हैं।
अब वैश्विक व्यापारिक व्यवस्था कहीं अधिक खतरनाक रूप ले चुकी है।
ट्रंप की दुनिया में व्यापार का नियम यही है कि “कोई नियम नहीं”, सिवाय उसके जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उस दिन कह दें।

वैश्विक मीडिया ने चीन द्वारा रेयर अर्थ (Rare Earths) निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों और आपूर्ति शृंखला (supply chain) पर उसके प्रभाव पर काफी चर्चा की है,
लेकिन बहुत कम ने उस अमेरिकी अधिसूचना का ज़िक्र किया है जो 29 सितंबर 2025 को US Department of Commerce ने जारी की थी —
जो चीन के रेयर अर्थ प्रतिबंधों से ठीक पहले आई थी।
29 सितंबर की अमेरिकी घोषणा के तहत निर्यात नियंत्रण सूची (Export Control List) में शामिल चीनी कंपनियों की संख्या 1,300 से बढ़ाकर 20,000 से अधिक कर दी गई — यानी 15 गुना वृद्धि।
अब ये कंपनियां अमेरिकी निर्यात नियंत्रण के नए नियमों का पालन करने को बाध्य होंगी। लेकिन यह तो केवल हिमशैल का ऊपरी हिस्सा है।
मार्टिन चोर्ज़ेम्पा (Martin Chorzempa) ने Peterson Institute for International Economics (PIIE) की वेबसाइट पर (27 अक्तूबर 2025) लिखा —
“अब कोई भी अमेरिकी कंपनी अगर चीन को एक सोयाबीन भी निर्यात करना चाहती है, तो उसे अपने चीनी ग्राहकों की पूरी स्वामित्व श्रृंखला (ownership chain) की जटिल जांच करनी होगी, ताकि किसी जुर्माने या जेल की सज़ा से बचा जा सके…
‘50 प्रतिशत नियम’ (50% rule) भले ही एक तकनीकी बदलाव लगे,लेकिन इसका असर — खासकर चीन पर — बेहद बड़ा होगा।”
मैं यहां यह नहीं कहूंगा कि अमेरिका के निर्यात प्रतिबंध और चीन की प्रतिक्रिया बराबर या पारस्परिक (reciprocal) हैं।
इतना कहना पर्याप्त है कि इन दोनों कदमों से वैश्विक आपूर्ति शृंखला (global supply chain) के टूटने और विभाजित होने का ख़तरा अब बहुत निकट है।
हम GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) और उसके बाद WTO की उस विश्व व्यवस्था का अंत देख रहे हैं जिसमें लगभग सभी देशों ने एक साझा नियमों के ढांचे को स्वीकार किया था — भले ही वह ढांचा पश्चिमी देशों, विशेषकर OECD समूह के पक्ष में झुका हुआ था। अब 29 सितंबर का अमेरिकी आदेश और चीन के रेयर अर्थ प्रतिबंध — इन दोनों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि हर देश को अपनी आपूर्ति शृंखला नए सिरे से तैयार करनी होगी,
ताकि एक व्यापारिक ब्लॉक से जुड़ी इकाइयां दूसरे से व्यापार न करें।
हम लगभग उसी दौर में लौट रहे हैं जब पश्चिमी और समाजवादी देशों की अर्थव्यवस्थाएं अलग-अलग थीं,
और बाकी दुनिया दोनों के साथ तालमेल बिठाने की कठिन राह पर थी।
अब फर्क यह है कि उत्पादों की जटिलता (complexity) पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है। मसलन, मॉडल टी फोर्ड (Model T Ford) — जो पहला बड़े पैमाने पर बना कार मॉडल था — उसका इंजन लगभग 100 चलने वाले हिस्सों (moving parts) वाला था। आज की साधारण पेट्रोल कार में ही 1,000 से 2,000 हिस्से होते हैं — यानी दस से बीस गुना अधिक। इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles - EVs) में इंजन के हिस्से भले कम हों, लेकिन उनकी बैटरी और उसकी आपूर्ति शृंखला कहीं अधिक जटिल है। यहां तक कि पेट्रोल या डीज़ल कार में भी आज चिप-आधारित इलेक्ट्रॉनिक असेंबली की लागत कुल वाहन की कीमत का 40–50% होती है।
इस तरह की जटिल आपूर्ति शृंखलाओं को अलग-अलग ब्लॉकों में बांटना अमेरिका जितना आसान समझ रहा है, उतना है नहीं।
यह केवल व्यापारिक संरचना की जटिलता नहीं, बल्कि
उत्पादन प्रणाली (production system) की तकनीकी जटिलता है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को विभाजित करना लगभग असंभव बना देती है।
ट्रंप प्रशासन चाहे जितना विश्वास रखे, दुनिया अब “Back to the Future” के दौर में नहीं लौट सकती। अब अगर दो अहम उद्योगों — चिप उद्योग (semiconductors) और रेयर अर्थ उत्पादन (rare earth production) — पर नज़र डालें,
तो साफ है कि जो देश इन आपूर्ति शृंखलाओं के “बॉटलनेक (bottlenecks)” को नियंत्रित करता है, वही असल नियंत्रण रखता है।
मीडिया का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि रेयर अर्थ्स का अर्थ सिर्फ खनन (mining) है — जबकि असली तकनीकी नियंत्रण चीन ने धातुओं के परिष्करण (ore concentration and separation) की प्रक्रिया में हासिल किया है।

जैसे केरल की मोनाज़ाइट रेत (monazite sands) में पाया जाने वाला थोरियम (thorium), जो रेडियोधर्मी होता है।
रेयर अर्थ्स का इस्तेमाल स्थायी चुंबकों (permanent magnets) में होता है, जो लगभग हर उच्च दक्षता वाले मोटर या जनरेटर में जरूरी हैं।
ऑस्ट्रेलिया जैसे देश खनन तो करते हैं — लेकिन भारी रेयर अर्थ्स (heavy rare earths) के अंतिम शोधन (final separation) की प्रक्रिया लगभग पूरी तरह चीन में होती है।
Benchmark Mineral Intelligence के अनुसार,
चीन वैश्विक भारी रेयर अर्थ प्रसंस्करण (processing) का 99% हिस्सा नियंत्रित करता है।
Goldman Sachs का अनुमान है कि पश्चिम को इस नियंत्रण को ढीला करने में कम से कम एक दशक लगेगा। रेयर अर्थ्स न केवल नवीकरणीय ऊर्जा (renewable energy) बल्कि
सैन्य उपकरणों (military equipment) — मिसाइल, ड्रोन, विमान, जहाज़, पनडुब्बी — तक के निर्माण में अनिवार्य हैं।
यानी अगर चिप निर्माण (chipmaking) की तकनीक (जैसे लिथोग्राफी) पर नियंत्रण अमेरिका के पास है, तो रेयर अर्थ इकोसिस्टम (rare earth ecosystem) पर चीन का कब्ज़ा है।
दिलचस्प है कि ASML की लिथोग्राफिक मशीन — जो अमेरिकी नियंत्रण की धुरी है— उसे भी अपने लेज़र और चुंबक तंत्र (laser and magnet systems) में बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ्स की ज़रूरत होती है।
अमेरिका के पास इस समय सिर्फ रक्षा क्षेत्र में बढ़त है —
जिसे ट्रंप ने सटीक नाम दिया है — Department of War.
अमेरिका का सैन्य खर्च दुनिया के अगले नौ देशों के संयुक्त खर्च के बराबर है। ट्रंप की रणनीति है कि इस सैन्य शक्ति (military power) को आर्थिक दबाव (trade and financial leverage) में बदला जाए।
उनकी दृष्टि में “extortion” यानी धमकी ही अब वैश्विक व्यापार की नई भाषा है।
अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपनी सैन्य ताकत और डॉलर (global currency) को वैश्विक आर्थिक वर्चस्व (economic dominance) में बदल पाएगा?
यही इस पूरे वैश्विक व्यापार युद्ध का केंद्र है — जिसे ट्रंप ने सिर्फ चीन नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों तक पर छेड़ दिया है।
संभव है कि अभी के लिए अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध (tariff battle) में कुछ राहत दिखे, और बुसान में ट्रंप-शी बैठक ने तत्काल संकट को टाल दिया हो। लेकिन जब तक अमेरिका वैश्विक व्यापारिक ढांचे (global trading regime) में लौटने को तैयार नहीं होता, यह युद्ध समाप्त नहीं होगा।
और फिलहाल यह संभावना बहुत कम दिखती है — क्योंकि विश्व व्यापार संगठन (WTO) को कमजोर करना ट्रंप और जो बाइडन (Joe Biden) — दोनों के दौर में एक समान द्विदलीय नीति (bipartisan policy) रही है।
मूल रूप से अंग्रेज़ी में प्रकाशित आलेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें–
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।