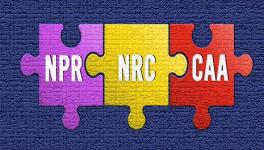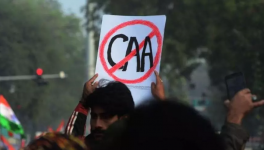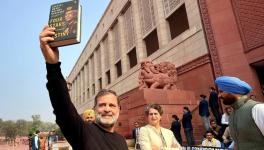मध्यप्रदेश : 60 लाख विमुक्त, घुमंतू, अर्ध-घुमंतू जनजातियां खो सकती हैं अपनी नागरिकता

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करने के फ़ैसले से मध्यप्रदेश की विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां, जो राज्य की आबादी का लगभग 7 से 8 प्रतिशत हैं, अपनी नागरिकता खोने के भय में जी रही हैं।
केंद्र सरकार ने सोमवार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने के लिए 3,941.35 करोड़ रुपये ख़र्च करने की मंज़ूरी दे दी है, जो कि गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) की ओर पहला क़दम है। एनपीआर तैयार करने की प्रक्रिया अप्रैल 2020 से शुरू होगी और असम को छोड़कर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा (जहां एनआरसी पहले ही पूरी हो चुकी है)।
जब से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और एनआरसी के मुद्दे ने देश में उथल-पुथल मचाई है, इन समुदायों को अपने लिए दस्तावेज़ इकट्ठा करने में मानसिक पीड़ा और कठिनाई के दौर से गुज़रना पड़ रहा है।
विमुक्त घुम्मक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की 51 जातियाँ हैं, जिन्हें 2012 में आदिवासी विभाग से अलग कर दिया गया था। इसके अलग होने के सात साल बाद भी, विभाग के पास कोई आधिकारिक डाटा नहीं है कि इन समुदायों की कुल जनसंख्या कितनी है।
लेकिन, विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राज्य में 50 लाख से अधिक विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विमुक्त घुम्मक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति प्रकोष्ठ के अनुसार और कांग्रेस के अंदाज़े के मुताबिक़ इनकी आबादी लगभग 60 लाख है। यह राज्य की कुल आबादी का 8 प्रतिशत बैठता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी 7.5 करोड़ है।
इसके अलावा, भाजपा के विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति प्रकोष्ठ के प्रमुख संजय यादव, जिन्होंने भाजपा शासन में घुमक्कड़ जाति विकास परिषद, मध्य प्रदेश (एक सरकारी निकाय) के प्रमुख के रूप में प्रभार सँभाला था, ने भी आबादी को लगभग 60 लाख ही आँका है।
जहां तक देश का संबंध है, रेनका समिति 2008 की रिपोर्ट, जो कि 2001 की जनगणना पर आधारित है, के मुताबिक़ देश भर में ऐसे 11 करोड़ से अधिक लोग हैं, जो विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों से हैं। इनकी संख्या अब अधिक भी हो सकती है।
चूंकि, इन समुदायों के सदस्य शायद ही किसी एक विशेष स्थान पर रहते हैं, उनके पास निवास, जन्म, शिक्षा, जाति और भूमि का कोई भी आधिकारिक प्रमाण नहीं है। वे बड़े पैमाने पर दैनिक मज़दूरी करते हैं, पशु चराते हैं, खेतों में खेत मज़दूर की तरह काम करते हैं या फिर वे पारंपरिक कला कार्यों में कुशल होते हैं और उनके ज़रिये कमाई करते हैं।
“कुछ को छोड़कर, उनमें से अधिकांश के पास जन्म का प्रमाण या ज़मीन के कोई दस्तावेज़ नहीं हैं। न ही वे इन्हें हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह भी याद नहीं कि वे पैदा कहाँ हुए हैं। वे अशिक्षा के कारण भी जन्म प्रमाण पत्र कभी नहीं बनवा पाते हैं।” ये बातें ख़ानाबदोश जनजाति के कार्यकर्ता, ललित दौलत सिंह ने बताई हैं।
शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 2014 में, इन जनजातियों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया था, लेकिन कुछ अधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार, आधिकारिक दस्तावेज़ों की कमी के कारण शायद ही 10-15 प्रतिशत लोग प्रमाण पत्र बनवाने में सफल रहे।
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “ज़्यादातर लोग तय नियमों के अनुसार किसी भी आधिकारिक दस्तावेज़ को पेश करने में विफल रहे, जिसके आधार पर उनका जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना था। जिन लोगों ने दस्तावेज़ प्रस्तुत किए, उन्हें प्रमाणपत्र मिल गया।”
एक अधिकारी ने बताया, “मप्र में 51 समुदाय हैं इनमें से कुछ को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) में जोड़ा गया है और कुछ को अनुसूचित जाति के रूप में जोड़ा गया है। इसलिए, यह पहचानना मुश्किल है कि कौन कौन है, और नए जाति प्रमाण पत्र कैसे जारी करें। यह केवल एक सर्वेक्षण के आधार पर ही किया जा सकता है जो अभी भी पाइपलाइन में बंद है।”
कांग्रेस सरकार ने भी कुछ मानदंडों को छोड़ते हुए जाति प्रमाणपत्र अभियान शुरू किया है।
अधिकारियों ने दावा किया है कि आधार और जन धन योजना के अस्तित्व में आने के बाद से, कुछ लोगों के पास आधार, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और बैंक खाते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय के एक ट्वीट के अनुसार, "भारत की नागरिकता सिर्फ़ जन्म की तारीख़ या जन्म स्थान से संबंधित दस्तावेज़ के आधार पर ही साबित की जा सकती है।”
ऐसी स्थिति में, इन समुदायों को जन्म की तारीख़ और जन्म स्थान का प्रमाण दिखाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कथन देव सिंह चौहान जो मध्यप्रदेश कांग्रेस के विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा, "वे लोग जो जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए कोई दस्तावेज़ दिखाने में विफल रहे, वे जन्म स्थान या जन्म प्रमाण पत्र कैसे दे सकते हैं?"
प्रकोष्ठ ने एनपीआर और एनआरसी के फ़ैसले का भी विरोध किया है और मुख्यमंत्री कमलनाथ से राज्य में इसे लागू न करने का आग्रह किया है।
दूसरी तरफ़, बीजेपी के यादव ने एनपीआर और एनआरसी का समर्थन किया है और कहा है, "एनपीआर और एनआरसी को राज्य में लागू किया जाना चाहिए, ताकि हम मूल निवासी और घुसपैठियों के बीच अंतर कर सकें।"
यह पूछे जाने पर कि जन्म प्रमाण न होने के कारण, क्या एनआरसी लागू होने पर उनके समुदाय के सदस्यों को नुकसान होगा, यादव ने कहा, "अगर हमें सताया जाता है, तो हम गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलेंगे और उनसे छूट देने का आग्रह करेंगे क्योंकि हम हिंदू हैं और देशज समुदाय से हैं।”
क्यों इन जनजातियों के पास दस्तावेज़ नहीं हैं?
ख़ानाबदोश जनजाति के कार्यकर्ता ललित दौलत सिंह ने कहा कि इस बात को समझने के लिए इन जनजातियों के पास कोई दस्तावेज़ क्यों नहीं हैं, ब्रिटिश के 'आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871' को पढ़ने की ज़रूरत है।
देश की जिप्सी और घुमंतू जनजातियों ने 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन की पहली लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों पर कई हमले किए थे। हमलों से नाराज़ होकर, ब्रिटिश हुकूमत ने 'आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871’ को लागू कर दिया, भारत को नियंत्रण करने लिए ग़लत रणनीति थी जिसके तहत उन्होंने देश की बड़ी संख्या में भारतीय जातियों और समुदायों को अपराधी क़रार दे दिया था।
देश के विभिन्न हिस्सों में इन जनजातियों की बस्तियों का निर्माण होता था लेकिन इस क़ानून के बदौलत पुलिस उनकी आवाजाही और व्यवहार पर निरंतर निगरानी रखने लगी ताकि उन्हें किसी भी किस्म का अपराध करने से रोका जा सके। लेकिन इस व्यवस्था ने इन जनजातियों और समुदायों का काफ़ी उत्पीड़न किया और बेइंतहा कष्ट दिया है, इसने उनकी जीवन शैली और जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाला। और इसलिए ख़ुद को बचाने के लिए वे एक जगह से दूसरी जगह भागने लगे।
1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, 'आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871' की समीक्षा की गई और अंततः 1952 में अय्यंगर समिति की 1949 में की गई सिफ़ारिश के तहत इसे निरस्त कर दिया गया।
परिणामस्वरूप, सभी जातियों और समुदायों को आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 के तहत विमुक्त कर दिया गया। हालांकि क़ानून को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इसका प्रतिकूल प्रभाव दोनों जातियों और समुदायों पर आज भी जारी रहा, जिन्हें पहले ही बड़े पैमाने पर नागरिक समाज ने अपराधी के रूप में घोषित किया हुआ है। ब्रिटिश हुकूमत की यह असामाजिक एवं आपराधिक विरासत आज भी क़ायम है और पुलिस और नागरिक समाज दोनों जनजातियों को संदेह और अपमान के साथ देखते हैं।
राज्य की राजधानी भोपाल के प्रमुख फ्लाईओवरों, पुलों के नीचे और सड़क के डिवाइडर के किनारे, भोपाल और हबीबगंज रेलवे स्टेशनों के आस-पास रहने वाले सैकड़ों जिप्सी और घुमंतू जनजातियों के सदस्य, शहर की पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हैं।
“पुलिस हमारे साथ क्रूर व्यवहार करती है। वे हमारी झोपड़ियों के साथ तोड़फोड़ करती है, हमारे परिवार के सदस्यों की पिटाई करती है और हमें धमकी देती है कि हम सभी को रात भर सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा।” उपरोक्त बातें राजस्थान के मूल निवासी मेजर बागड़ी ने कही हैं, जो राज्य की राजधानी के बोर्ड ऑफ़िस चौक के पास रहते हैं, और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यातायात सिग्नल पर गुब्बारे बेचते हैं।
बागड़ी की तरह, दर्जनों ऐसे लोग हैं जो लगभग हर दिन ट्रैफ़िक सिग्नल, स्टेशन पर पुलिस की बर्बरता का सामना करते हैं।
अफ़सर क्या कहते हैं?
विमुक्त घुम्मक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति विकास के प्रधान सचिव रमेश थेते से कई प्रयास करने की बाद भी बात नहीं हो पाई।
लेकिन, विभाग की उप निदेशक दीप्ति एस कोटशाने ने कहा कि विभाग शुरू में एक सर्वेक्षण कर एक डाटाबेस बनाने की योजना बना रहा था, जिस आधार पर नीतियों को तैयार किया जाना था। उन्होंने कहा, “विभाग के पास आज तक कोई डाटा नहीं है।”
जब इन समुदायों से एनपीआर और एनआरसी को लागू करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, “पीएस रमेश थेते के सुझावों पर, विभाग प्रत्येक व्यक्ति को एक आईडी कार्ड जारी करने की योजना बना रहा है, जो एनआरसी दस्तावेज़ों के लिए मान्य हो सकता है। लेकिन, यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है।”
कोटशाने ने आगे कहा कि, “इन समुदायों के लगभग 30 से 40 प्रतिशत लोगों के पास ही दस्तावेज़ हैं। यदि एनआरसी लागू होती है, तो बाक़ी को इससे बाहर किया जा सकता है, इसलिए हम इसके बारे में चिंतित हैं और एक योजना तैयार कर रहे हैं।” उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि इन घुमंतू और अर्धघुमंतू जनजातियों के लिए पटवारी भी दस्तावेज़ जारी करने के लिए के लिए योग्य हैं जो कुछ वर्षों या दशकों तक, एनआरसी के लिए एक वैध प्रमाण हो सकते हैं।
उन्होंने कहा, "एनपीआर को लागू करने का काम प्रारंभिक स्तर पर चल रहा है, इसलिए अभी निवास या जन्म के प्रमाण के बारे में बात नहीं करनी चाहिए।"
रेनका कमेटी 2008, जिसका गठन विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का जायज़ा लेने के लिए किया गया था, का दावा है कि देश में 11 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनमें एससी/एसटी जैसे आरक्षण के प्रावधान भी शामिल हैं। हालाँकि, वह रिपोर्ट 2001 की जनगणना पर आधारित थी। इसलिए, ऐसा अंदाज़ा है कि यह संख्या अब तक बढ़ गई होगी।
अंग्रेजी में लिखा मूल आलेख आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं।
In MP, 60 lakh Denotified, Nomadic, Semi-Nomadic Tribes May Lose Citizenship
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।