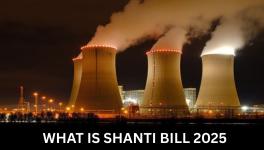विश्लेषण: GST समायोजन से नहीं होगी ट्रंप के टैरिफ़ की काट

भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ हमले का भारतीय अर्थव्यवस्था पर संकुचनकारी (contractionary ) प्रभाव पड़ने में कोई संदेह नहीं है। अगर ट्रंप इस समय लगाये जा रहे 50 फीसद की दर से अपने टैरिफ को कम भी कर देता है, तब भी यह भारत के अमेरिकी माल पर टैरिफ घटाए जाने के बदले में ही किया जा रहा होगा। ऐसा खासतौर पर उसके कृषि उत्पादों तथा दुग्ध उत्पादों पर टैरिफ घटाए जाने के बदले में ही किया जा रहा होगा, जिसका मतलब होगा अमेरिका से आयात का बढ़ना और इसलिए भारत में आमदनियों का घट जाना।
ट्रंप के टैरिफ के इस संकुचनकारी प्रभाव की काट करने के लिए जरूरत इसकी होगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्रय शक्ति डाली जाए और इसके तीन संभव रूप हो सकते हैं।
- पहला, राजकोषीय घाटे का बढ़ाया जाना।
- दूसरा, अमीरों पर ज्यादा कर लगाने के जरिए बढ़े हुए सरकारी खर्च के लिए वित्त व्यवस्था किया जाना, जो अमीरों की बचत यानी उनके गैर-व्यय के एक हिस्से को, सरकारी खर्चों में तब्दील कर रहा होगा।
- या तीसरा, ऋण की वित्त व्यवस्था से संचालित, निजी उपभोग व्यय में बढ़ोतरी या उसी हिसाब से निजी बचत अनुपात में कमी।
गुड्स एंड सर्विसेज कर की दरों में, 22 सितंबर से लागू हुए जिन समायोजनों की घोषणा की गयी थी, वह अपने आप में अर्थव्यवस्था में कोई क्रय शक्ति नहीं डालते हैं। इस तरह का समायोजन, जो पहले की चार कर दरों– 5, 12, 18 तथा 28 फीसद– की जगह पर सिर्फ दो दरें, 5 तथा 18 फीसद करता है (यह चंद ‘‘कलंकित मालों’’ के अलावा है, जिन पर अब 40 फीसद की दंडात्मक दर लागू होगी), निश्चित रूप से उपभोक्ताओं पर कुल बोझ घटाने का काम करेगा, बशर्ते ये रियायतें उन तक ‘‘पहुंचायी जाएं’’।
इसके साथ ही, अगर इससे होने वाली सरकार के राजस्व की हानि की भरपाई, खर्च में उसी हिसाब से कटौती कर के की जाती है, न कि राजकोषीय घाटे के आकार में बढ़ोतरी से, तो इस कदम के जरिए अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति में कोई शुद्ध बढ़ोतरी नहीं हो रही होगी। ऐसी सूरत में तो कर रियायतों के बल पर निजी उपभोग में जितनी बढ़ोतरी होगी, सरकारी खर्चों में उतनी ही कटौती हो जाएगी और इस तरह सकल मांग के स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही होगी। इसलिए, इस तरह के हालात में जीएसटी दर में दी गयी रियायतें, अर्थव्यवस्था पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा थोपे गए सकल मांग के संकुचन की काट नहीं कर सकती हैं।
इतना ही नहीं, इस सूरत में इसका तो दावा किया ही नहीं जा सकता है कि जीएसटी की दरों के घटाए जाने से, मेहनतकश जनता का कुल उपभोग बढ़ जाएगा, जिसका सरकार दावा कर रही है। अगर, उन क्षेत्रों में जिनमें इस तरह की रियायतों से उपभोग बढ़ने जा रहा है, मजदूरी-आमदनियों का हिस्सा उतना ही है, जितना उन क्षेत्रों में है, जिनमें राजस्व हानि के चलते सरकारी खर्चों में कटौतियां की जाने वाली हैं, तो मजदूरों का कुल उपभोग (या और सामान्य रूप से मेहनतकशों का कुल उपभोग), सरकार के राजकोषीय कदमों के चलते अपरिवर्तित ही रहेगा। और यह किसी भी तरह से असंभव पूर्व-कल्पना नहीं है क्योंकि सरकार के खर्चों में कटौतियां मुख्यत: ढांचागत क्षेत्र में होंगी, जिसका निर्माण क्षेत्र एक बड़ा घटक है। और निर्माण बहुत ही रोजगार सघन होता है, जिसमें कुल उत्पाद में मजदूरी-आय का हिस्सा, उसी हिसाब से ज्यादा होता है।
जीएसटी रियायतों के वित्तपोषण का सवाल
इसका अर्थ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेहनतकश जनता की आमदनियों में जो कटौती थोपी जा रही है, उसकी काट सरकार के राजकोषीय कदमों से मेहनतकशों की आमदनियों में किसी भी बढ़ोतरी से नहीं होने वाली है। सरकार के राजकोषीय कदम उनकी आमदनियों को जहां का तहां, उस निचले स्तर पर ही छोड़ देंगे, जिस पर ट्रंप के टैरिफ उन्हें धकेल देंगे। संक्षेप में यह कि ट्रंप के टैरिफों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे संकुचनकारी प्रभावों की काट करने के लिए और इन टैरिफ के चलते मेहनतकश जनता की आय में होने वाले संकुचन को निष्प्रभावी बनाने के लिए, मोदी सरकार से कुछ भी किया ही नहीं है। हालांकि, ऐसा लग सकता है कि जीएसटी रियायतें देना, मेहनतकश जनता के उपभोग में बढ़ोतरी करने के बराबर है, लेकिन जब तक राजकोषीय घाटा बढ़ाया नहीं जाता है (या इसके विकल्प के तौर पर अमीरों से और ज्यादा प्रत्यक्ष कर इकट्ठा करने के जरिए, इस तरह की जीएसटी रियायतों से होने वाली राजस्व हानि की भरपाई नहीं की जाती है), तब तक सरकार के इन राजकोषीय कदमों से मेहनतकश जनता का कुल उपभोग वास्तव में अपरिवर्तित ही बना रहेगा।
जहां भारतीय अर्थव्यवस्था पर ट्रंप के टैरिफ के संकुचनकारी प्रभावों की मोदी सरकार के राजकोषीय कदमों से तो शायद ही कोई काट हो रही होगी, निजी उपभोक्ता खर्चों में ऐसी बढ़ोतरी का क्या जो ऋण से संचालित हो सकती है या बचत अनुपात में कटौती से संचालित हो सकती है? अखबार इसकी खबरों से भरे हुए हैं कि जीएसटी की दरों में समायोजन से, सरकार को अनुमानत: कितनी राजस्व हानि होने जा रही है। खुद केंद्र सरकार ने एक पूरे साल में राजस्व हानि का आंकड़ा 48,000 करोड़ रुपये लगाया है। यह इस पूर्वकल्पना पर आधारित है कि जीएसटी की दरों में कमी से कुल 93,000 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होने जा रही है, जिसमें से 45,000 करोड़ रुपये की भरपाई ‘‘कलंकित मालों’’ पर कर की दरों में होने वाली बढ़ोतरी से हो जाएगी। दूसरी ओर, भारतीय स्टेट बैंक ने पूरे साल का घाटा 3,700 करोड़ रुपये ही लगाया है। इस अनुमान का आधार यह है कि जीएसटी दरों में कटौतियों के चलते कीमतों में गिरावट से उपभोग को इतना ज्यादा उत्प्रेरण मिलेगा कि कर की दरों में कटौती के बावजूद, कुल राजस्व में बहुत मामूली गिरावट ही हो रही होगी। बहरहाल, विभिन्न निजी अनुमानों में, और इसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अनुमान भी शामिल हैं, जीएसटी दरों में कटौती से राजस्व हानि को कहीं कहीं ज्यादा, 1.2 से 1.5 लाख करोड़ रुपये तक आंका है। बहरहाल, इन अनुमानों के पीछे जो सैद्धांतिक पूर्वकल्पनाएं काम कर रही हैं, उन्हें कभी उजागर ही नहीं किया जाता है, जबकि उन्हें उजागर किया जाना चाहिए।
अतिरिक्त क्रय शक्ति कहां से आएगी?
यह दावा कि इन कर कटौतियों से उपभोग खर्चों में इतनी जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी कि राजस्व हानि मामूली ही होगी (क्योंकि अब कर की घटी हुई दर, कहीं बढ़ी हुई मात्रा पर लागू की जा रही होगी) असली सवाल से बचकर निकल जाता है। सवाल यह है कि इस बढ़े हुए उपभोग के लिए क्रय शक्ति आएगी कहां से? अगर बेस लेवल उपभोग पर कर रियायतें, मान लीजिए कि 100 रुपये की दी जा रही हों, तो बेस लेवल से ऊपर उपभोग में 100 रुपये की बढ़ोतरी स्पष्ट रूप से समझ में आती है। लेकिन, उस सूरत में राजस्व घाटा 100 रुपये का होगा, इससे एक पैसा कम का नहीं। लेकिन, अगर दावा यह किया जा रहा है कि बेस लेवल पर उपभोग खर्च में 100 रुपये की कर रियायत के चलते 200 रुपये बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे राजस्व का वास्तविक नुकसान बेस लेवल उपभोग पर कर रियायतों से घटकर होगा, तो सवाल यह खड़ा होता है कि 100 रुपये की यह अतिरिक्त क्रय शक्ति आएगी कहां से? यह तर्क दिया जा सकता है कि इन कर रियायतों से उपभोक्ताओं में ऐसा जोश पैदा होगा कि वे उपभोग बढ़ाने के लिए ऋण लेंगे या फिर इसके लिए अपनी बचत में हाथ डालेंगे। बहरहाल, हम एक क्षण के लिए इसे सच भी मान लें, तब भी यह तथ्य तो अपनी जगह रहता है कि मजदूर वर्ग को न तो इस तरह के ऋणों का पात्र समझा जाएगा और ना उनके पास ऐसी बचत होगी, जिसमें से पैसा निकाल कर, टिकाऊ उपभोक्ता मालों की कीमतों में कमी का फायदा उठा सकें। दूसरे शब्दों में उपभोग में तथाकथित उछाल, मजदूर वर्ग के बीच से आने की उम्मीद तो की नहीं जा सकती है।
मध्यवर्गीय उपभोक्ता, जिनमें वेतनभोगी भी शामिल हैं, यह देखकर कि कर रियायतों के चलते चीजें अचानक पहले से कुछ सस्ती हो गयी हैं, ऋण लेने के बल पर या अपनी बचतों में हाथ डालने के सहारे, शायद पहले से ज्यादा खरीददारी करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन, उस सूरत में भी उपभोग में यह उछाल अस्थायी ही होगी। जब संबंधित ऋण के भुगतान का समय आएगा या जब ऋण की किस्तें (ईएमआइ) चुकाने का समय आएगा, उन्हें अपने उपभोग में कटौती करनी पड़ रही होगी। दूसरे शब्दों में, उपभोग में ऋण के बल पर बढ़ोतरी न सिर्फ अस्थायी उछाल ही पैदा करती है बल्कि वास्तव में एक प्रक्रिया के जरिए, जिसे अर्थशास्त्री जोज़फ शुम्पीटर ने ‘स्व-संकुचन’ या ऑटो डिफ्लेशन का नाम दिया था, खुद को पलटती भी है। इस रास्ते के जरिए, जो वह तीसरा रास्ता है जिसका हमने पीछे जिक्र किया था, अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति का डाला जाना, अस्थायी भी होता है और खुद को पलटने वाला भी होता है।
इसका अर्थ यह हुआ कि मोदी सरकार ने, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हमले के संकुचनकारी प्रभावों की काट करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। यहां तक कि उसने ऐसे स्वत:स्पष्ट कदम भी नहीं उठाए हैं, जैसे प्रभावित लघु उत्पादकों को वित्तीय सब्सीडियां मुहैया कराना और इसके लिए अमीरों पर कर बढ़ाने के जरिए (जिसमें एक संपदा कर भी शामिल हो सकता है) वित्त जुटाना। उसने जिन जीएसटी रियायतों की घोषणा की है, अपने आप में उपभोग नहीं बढ़ाने जा रही हैं और इस तरह ट्रंप के कदमों की काट करने के लिए अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरण मुहैया नहीं कराने जा रही हैं। इसकी वजह यह है कि ये रियायतें अपने आप में अर्थव्यवस्था में कोई क्रय शक्ति नहीं डालती हैं।
शॉर्ट कट, जो मोदी सरकार अपनाएगी
बहरहाल, एक रास्ता है जो मोदी सरकार के अपनाने की संभावना है और चाहे सचेत रूप से एक आर्थिक-संकुचन विरोधी कदम के तौर पर नहीं भी हो, उसके इसे अपनाने की संभावना है। इस रास्ते को शासक वर्ग के सभी हिस्सों का अनुमोदन भी मिल जाएगा। यह रास्ता है, ऐसे उपायों से राजकोषीय घाटा बढ़ाना, जिन्हें राजकोषीय घाटे में नहीं गिना जाता है, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सा पूंजी की बिक्री। किसी कालखंड में सार्वजनिक उद्यमों के निजीकरण के ठीक वही वृहद आर्थिक नतीजे होते हैं, जो नतीजे बढ़े हुए वित्तीय घाटे के होते हैं। इसके जरिए सरकारी हिस्सा पूंजी निजी हाथों में दे दी जाती है, जबकि राजकोषीय घाटा सरकारी बॉन्ड निजी हाथों में देने का काम करता है। उनका असर एकदम एक जैसा होता है। लेकिन, पूरी तरह से फर्जी तथा बेईमानी-भरे कारणों से, आइएमएफ तथा वैश्वीकृत वित्त की अन्य एजेंसियां, इस सरल तथा स्वत:स्पष्ट परिघटना को पहचानती ही नहीं हैं। ये एजेंसियां राजकोषीय घाटे पर तो नाक-भौं सिकोड़ती हैं, लेकिन निजीकरण का अनुमोदन करती हैं, क्यों कि वह उन्हें पसंद है। मोदी सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों का निजीकरण करने और इस तरह के निजीकरण से होने वाली प्राप्तियों से वित्त चालित खर्चों के जरिए, वैश्वीकृत वित्तीय पूंजी को भी खुश कर रही होगी और घरेलू बड़े व्यवसाय को भी, जबकि ये प्राप्तियां घाटे की वित्त व्यवस्था से अलग नहीं होती हैं और उनका अर्थव्यवस्था पर उसके चाहे बिना भी वही संकुचन-विरोधी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन, इस तरह के निजीकरण से पूंजी का केंद्रीकरण और बढ़ जाएगा और पहले ही ज्यादा संपदा असमानता और बढ़ जाएगी।
(लेखक दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आर्थिक अध्ययन एवं योजना केंद्र में प्रोफ़ेसर एमेरिटस हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
मूल रूप से अंग्रेज़ी में प्रकाशित यह आलेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें–
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।