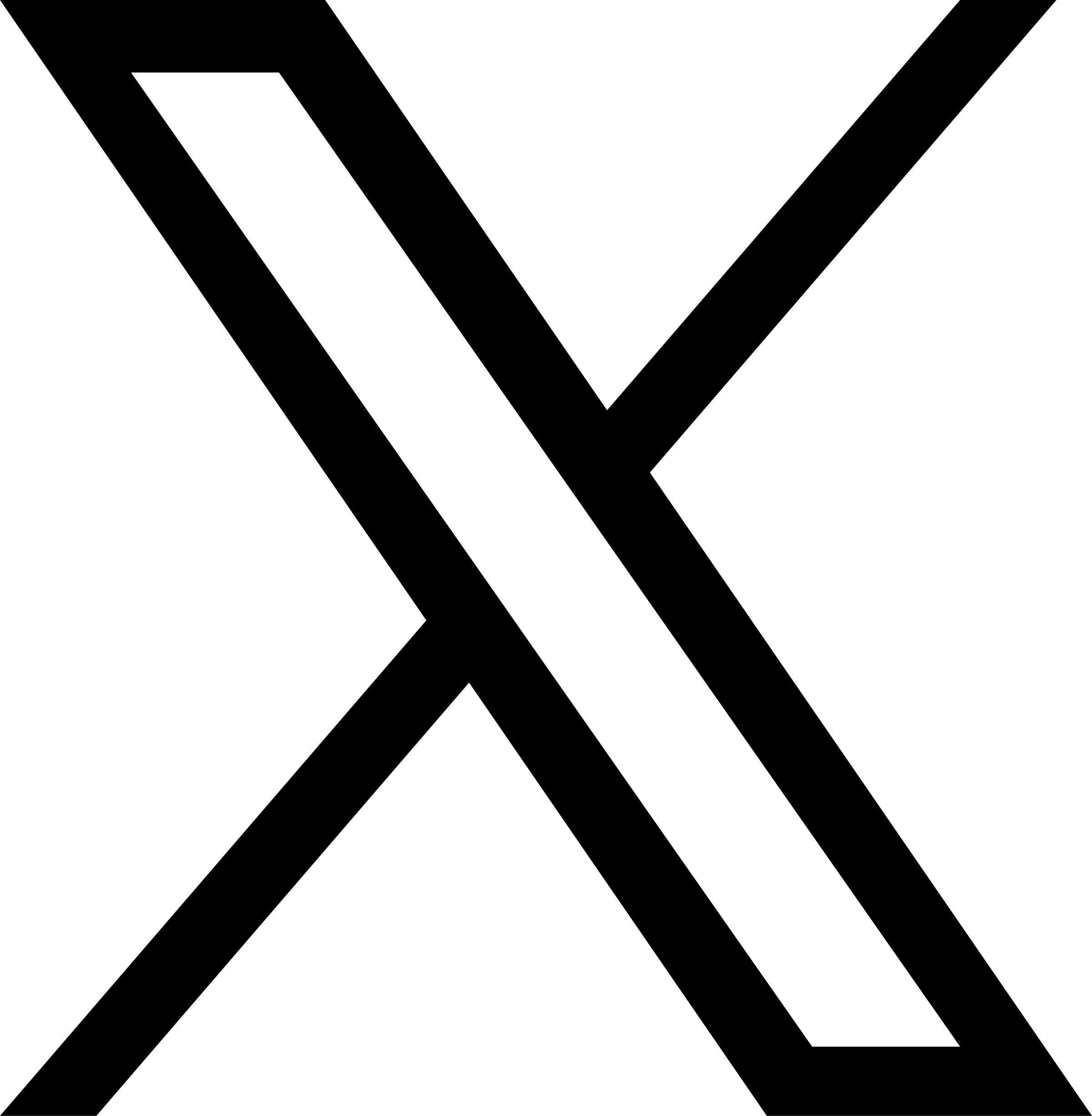कॉर्पोरेट-हिंदुत्व गठजोड़ और किसान

हम अजीबो-गरीब हालात से दो-चार हो रहे हैं। कई बार ऐसे मामले देखने का मिलते हैं, जहां उपभोक्ता चाहते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरतों की भरपाई करने के लिए, कहीं ज्यादा खाद्य फसलें उगाई जाएं, जबकि पहली नज़र में कृषि उत्पादक ही नकदी फसलों को अपनाने से होने वाले लाभों के लालच में आ जाते हैं और ज्यादा खाद्य फसलें उगाने के प्रति अनिच्छुक होते हैं। ऐसे हालात में इन विरोधी हितों के बीच, सरकार को मध्यस्थता कर के रास्ता निकालना पड़ता है।
सरकार बनाम जनता
लेकिन, भारत में फिलहाल तो किसानों की खाद्य फसलों को छोडक़र दूसरी फसलों की ओर जाने की कोई इच्छा नहीं है, जबकि उपभोक्ता तो जाहिर है कि यह चाहते ही हैं कि काफी खाद्यान्न पैदावार हो ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्नों की आपूर्ति हो सके। इस तरह, उनके हितों के बीच कोई ऐसा टकराव है ही नहीं, जिसमें सरकार के मध्यस्थ बनने की जरूरत हो। इसके बावजूद, हमारे देश की सरकार किसानों को खाद्य फसलों को छोडक़र, नकदी फसलों की ओर धकेलने के लिए उन्हें ऐसा बदलाव करने के लिए मजबूर कर रही है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नष्ट कर देगा।
सरकार के कृषि कानून ठीक ऐसा ही बदलाव लाना चाहते हैं। इन कानूनों की हिमायत करते हुए सरकारी अर्थशास्त्री, इसी तरह के बदलाव के लाभों पर जोर देते हुए, इन विधेयकों की हिमायत कर रहे हैं। इस तरह, इस मामले में सरकार कोई जनता के दो तबकों के हितों के बीच के टकराव में मध्यस्थता नहीं कर रही है। साफ तौर पर वह तो खुद अपने ही हित में जनता पर यानी किसानों तथा उपभोक्ताओं, दोनों पर समान रूप से इस तरह का बदलाव थोप रही है, जिसके खिलाफ किसान दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में आंदोलन में डटे रहे हैं। यह अजीबो-गरीब मामला जनता बनाम जनता का नहीं है बल्कि सरकार बनाम आमतौर पर समूची जनता का है।
इसी प्रकार, किसान एकराय से ठेका खेती को ठुकरा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार, इसके किसानों के हित में होने के नाम पर, इन कानूनों के जरिए किसानों पर ठेका खेती थोप रही है। पुन: यह कोई ऐसा मामला नहीं है कि जनता के किसी तबके के मांग करने पर सरकार ने ये कदम उठाए हों। ये कदम तो प्रकटत: वह अपने ही हितों में, जनता पर थोप रही है।
कार्पोरेटों के स्वार्थ को बनाया राष्ट्रहित
लेकिन, इन कदमों में इस सरकार का अपना स्वार्थ क्या हो सकता है? यह तो स्वत: स्पष्ट ही है कि इस मामले में सरकार का अपना हित, कार्पोरेटों तथा अंतर्राष्ट्रीय एग्रीबिजनस के स्वार्थों से पूरी तरह से मेल खाता है। फिर भी सरकार का जवाब तो यही होगा कि वह तो ‘राष्ट्रीय हित’ में ऐसा कर रही है। इस तरह, ‘राष्ट्रीय हित’ को कॉर्पोरेट हित के साथ एकरूप कर दिया जाता है। राष्ट्रीय हितों का कॉर्पोरेट हितों के साथ एकाकार किया जाना मोदी सरकार की निशानी रही है और यह उस कॉर्पोरेट-हिंदुत्व गठजोड़ की विशेषता ही है जिसे मोदी ने गढ़ा है और जो उन्हें सत्ता में बनाए रखा है।
बहरहाल, इस मामले का अजीबो-गरीबपन इस बात में छुपा हुआ है कि दक्षिणपंथी सरकारें भी, अपनी कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों को जनता के किसी न किसी तबके के हितों की हिफाजत करने की दुहाई देकर सही ठहराती हैं। मिसाल के तौर पर मार्गरेट थैचर ने ट्रेड यूनियनों पर अपने हमले को इस दलील के सहारे सही ठहराने की कोशिश की थी कि ये कदम मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए जरूरी थे, जो कथित रूप से ट्रेड यूनियनों की वजह से पैदा हो रही थी और जिसकी चोट आम जनता पर पड़ रही थी। लेकिन, भारत में हम बिल्कुल इकतरफा तथा मनमाने तरीके से ऐसे कदमों के थोपे जाना देख रहे हैं। जिनकी जनता के किसी भी तबके ने कभी मांग की ही नहीं थी, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ध्वस्त करने के आसार बनाते हैं, जिनका व्यापक जनता द्वारा विरोध किया जा रहा है और जिनके खिलाफ विशाल संख्या में जनता जोर-शोर से विरोध कर रही है। और यह सब किया जा रहा है सिर्फ कॉर्पोरेट हितों को आगे बढ़ाने के लिए। यह किसी भी जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए अभूतपूर्व है।
जनादेश का झूठा दावा
सरकार यह दावा करेगी कि चूंकि 2019 के चुनाव में उसकी जीत हुई थी, उसे अपनी मर्जी के ‘सुधार’ करने का जनादेश प्राप्त हैं। लेकिन, इस तरह का दावा गलत होगा और इसके कारण अनेक हैं। पहला तो यही इस तरह का दावा सिद्धांत के रूप में ही गलत है। किसी चुनाव में जीतना किसी भी सरकार को अपनी मर्जी से कुछ भी करने का जनादेश नहीं दे देता है। दूसरे, ऐसा इसलिए और भी ज्यादा है कि 2019 का चुनाव कोई ‘कृषि सुधारों’ के मुद्दे पर तो लड़ा नहीं गया था। वास्तव में ये कथित सुधार तो सत्ताधारी पार्टी के चुनावी नारों में कहीं आए तक नहीं थे। उसके चुनावी नारे तो पुलवामा हमले और बालाकोट हवाई हमलों पर ही केंद्रित थे। तीसरे, अब तो बड़े पैमाने पर राजनीतिक को ही एक माल में तब्दील किया जा चुका है, जहां विधायिका में बहुमत होने का भी कोई खास महत्व नहीं रह गया है।
चुनाव लडऩा अपने आप में असाधारण रूप से महंगा हो गया है। चुनाव से पहले, विरोधियों के बीच से अपने पक्ष में दलबदल कराना, अब आम-फहम हो गया है और बहुत महंगा भी। और चुनाव में कोई भी जीते, चुनाव के बाद पैसा बहाकर दूसरी पार्टियों से दलबदल कराए जाते हैं और इस तरह सरकार बनाने के लिए, आवश्यक बहुमत जुगाड़ लिया जाता है। इन सभी कारणों से जिस पार्टी की तिजोरियां सबसे भारी हों, उसे दूसरी पार्टियों के मुकाबले स्पष्ट बढ़त हासिल होती है और चूंकि ऐसा पैसा मुख्यत: कार्पोरेटों से ही आ सकता है, उनके साथ गठबंधन करना सत्ता में आने के लिए जरूरी हो जाता है। जाहिर है कि इसके लिए उन्हें बदले में भी कुछ चाहिए होता है। माल में तब्दील कर दी गयी राजनीति की ऐसी दुनिया में, अपने सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरणकारी एजेंडा तथा कॉर्पोरेट वित्तीय अनुमोदन के साथ, हिंदुत्ववादी ताकतें वर्चस्व कायम करने में कामयाब हो जाती हैं। बदले में उनकी ओर से कार्पोरेटों को दिए जा रहे प्रतिदान में, निहितार्थत: किसानी खेती पर नियंत्रण दिलाया जाना शामिल है।
कार्पोरेटों, खासकर, उनके नौसिखिया गुट का ज़्यादा मुनाफ़ा
वैसे तो ऐसी ताकतों के उभार से समग्र रूप से कार्पोरेटों को फायदा होता है। फिर भी उनके बीच से भी एक घटक- नौसिखिया घटक को- कहीं ज्यादा स्थापित घटकों के मुकाबले अक्सर कहीं ज्यादा फायदा मिलता है। देनिएल गुएरिन ने (‘फासिज्म एंड बिग बिजनस’) में दिखाया था कि 1930 के दशक में जर्मनी में, इजारेदार पूंजी का एक घटक, जो हथियारों के उत्पादन तथा उत्पादक मालों के काम में लगा हुआ था, नाजियों के साथ कार्पोरेटों के गठजोड़ के विशेष लाभार्थी बन गए थे, जबकि कपड़े तथा उपभोक्ता मालों के उत्पादन में लगे कार्पोरेटों के पुराने स्थापित घटक उतने लाभान्वित नहीं हुए थे। जापान में भी 1931 में सत्ता में आए फासिस्ट निजाम में, जिसके साथ कार्पोरेटों के घनिष्ठ रिश्ते थे, जापान के नये कारोबारी घरानों, शिंको जेईबत्सु को कहीं ज्यादा फायदा मिला था, जबकि मित्सुई जैसे पुराने घरानों को उतना फायदा नहीं मिला था। बेशक, आज का भारत, 1930 के दशक के जर्मनी या जापान से अलग है, फिर भी नये बने कॉर्पोरेट घरानों के एक घटक का उसी प्रकार विशेष रूप से लाभान्वित होना तो यहां भी देखा ही जा सकता है। यह किसानों के बीच और भी नाराजगी पैदा कर रहा है।
कार्पोरेटों को ‘संपदा निर्माता’ करार देकर मोदी, कॉर्पोरेट हितों को, खासतौर पर कार्पोरेटों के इस नौसिखिया हिस्से के हितों को, राष्ट्रीय हितों के समानार्थी बनाने की जमीन तैयार करते हैं। उनका आशय राष्ट्र की सम्पदा से था। इस तरह, इस प्रस्तुति के जरिए ही वह, निजी संपदा बटोरने को राष्ट्र की सेवा के स्तर पर पहुंचा देते हैं और और ऐसी संपदा बटोरने वालों को ‘राष्ट्र’ के विशेषाधिकार प्राप्त’ सदस्य बना देते हैं, जिनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। इसका अर्थ यह होता है कि जनता के सभी तबकों से, इन नौसिखिया कार्पोरेटों की मांगें मनवायी जानी चाहिए। ऐसा करना खुद देश की जनता के हित में होगा क्योंकि, इन कार्पोरेटों द्वारा संपदा बटोरा जाना तो कथित रूप से सभी के फायदे के लिए है।
इस तरह मोदी सरकार ने ‘राष्ट्रवाद की अवधारणा को ही सिर के बल पर खड़ा कर दिया है। कहां तो उसकी पहचान जनता से होती थी, उससे बदलकर उसकी पहचान को कार्पोरेटों, खासतौर पर नये कार्पोरेटों के साथ जोड़ दिया गया है। कृषि कानून, राष्ट्रवाद के इसी शीर्षासन में खड़े किए जाने को दिखाते हैं।
उपनिवेशविरोधी संघर्ष से विश्वासघात
बहरहाल, यह हमारे उपनिवेशविरोधी संघर्ष के साथ विश्वासघात है। सत्रहवीं सदी में यूरोप में वैस्टफेलियाई शांति संधियों की पृष्ठभूमि में जो ‘राष्ट्रवाद की अवधारणा विकसित हुई थी, साम्राज्यवादी थी, गैर-समावेशी थी (उसने एक ‘अंदरूनी शत्रु’ खोज लिया था) और कथित रूप से जनता द्वारा सम्मान की हकदार थी, जिसके लिए जनता से कुर्बानियां देने की अपेक्षा थी। इसके विपरीत, भारत जैसे देशों में उपनिवेशविरोधी राष्ट्रवाद, इससे बिल्कुल भिन्न था। वह तो अपने आप में अनोखी परिघटना ही था। वह राष्ट्रवाद को समावेशी नजर से देखता था, जिसका धमनिरपेक्षता एक अभिन्न हिस्सा थी। और राष्ट्रवाद की प्रणाली का तर्क ही यह मानता था कि वह अपने जनगण की जिंदगियां बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए। मोदी सरकार की समझदारी में छिपी राष्ट्रवाद की अवधारणा, उक्त उपनिवेशविरोधी धारणा से बिल्कुल उल्टी है और यूरोप की ही उस विस्तारकारी अवधारणा के ज्यादा नजदीक है, जिसका तार्किक उत्कर्ष फासीवाद में हुआ था।
दिल्ली के गिर्द जमा हुए किसान, हरेक पहलू से मोदी की विश्वदृष्टिकोण का विरोध कर रहे हैं। वे धर्मनिरपेक्षता को बुलंद कर रहे हैं, जो कि हिंदू, सिख तथा मुस्लिम किसानों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ आना खुद ब खुद इस बात को स्पष्ट करता है। खेती पर कॉर्पोरेट अतिक्रमण के अपने विरोध के जरिए वे, मुट्ठीभर कॉर्पोरेट घरानों के साथ ‘राष्ट्रवाद’ के एकरूप किए जाने को नकार रहे हैं। और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के पक्ष में खड़े होकर वे, राष्ट्रवाद के अस्तित्व के तर्क के रूप में, जनता की सेवा करने को स्थापित कर रहे हैं। मोदी सरकार ने राष्ट्रवाद की अवधारणा का अपहरण कर उसे जहां पहुंचा दिया है, किसान आंदोलन वहां से इस अवधारणा को जनता के पाले में वापस ला रहा है।
(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।