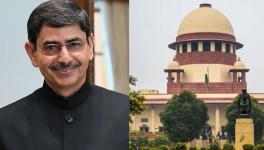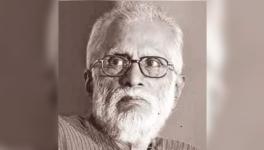लोकतंत्र में पुलिस राज की कभी जगह नहीं हो सकती, ज़मानत नियम है और जेल एक अपवाद!

'ज़मानत नियम है और जेल एक अपवाद है'
कानून के इस प्रसिद्ध सिदधांत को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अपने फैसले में कहा कि अंधाधुंध गिरफ़्तारियां औपनिवेशिक मानसिकता का संकेत हैं। अनावश्यक गिरफ़्तारियां सीआरपीसी की धारा 41 व 41(ए) का उल्लंघन हैं। कोर्ट ने ज़मानत आवेदनों के निपटारे को लेकर निचली अदालतों को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और उच्च अदालतों को निर्देश दिया कि सभी दिशानिर्देशों पर चार महीनों के अंदर हलफनामा या स्थिति रिपोर्ट दायर करें। केंद्र सरकार को ज़मानत के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश लाने के लिए नया ज़मानत कानून बनाने के लिए सख्त हिदायत दी है।
बता दें कि धारा 41 के तहत उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जब पुलिस बिना वॉरंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, जबकि धारा 41(ए) में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के बजाय नोटिस दिए जाने का प्रावधान है। अदालत के मुताबिक लोकतंत्र पुलिस तंत्र जैसा नहीं लगना चाहिए क्योंकि दोनों धारणात्मक तौर पर ही एक दूसरे के विरोधी हैं और इसलिए इससे बचा जाना चाहिए। अदालत ने ज़मानत को संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का मापदंड करार दिया। अदालत ने यह भी कहा कि संज्ञेय अपराधों के मामले में भी गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है।
क्या है पूरा मामला?
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो केस में आदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सोमवार, 11 जुलाई को अफसोस जताया कि भारत में जेलें विचाराधीन कैदियों से भरी पड़ी हैं। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी अपने आप में एक कठोर कदम है जिसका कम ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पुलिस अफसर को सिर्फ इसलिए किसी को गिरफ्तार कर लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। गिरफ्तारी की कुछ शर्तें होती हैं और उनका पूरा होना आवश्यक है।
अदालत ने आम लोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में अदालतों की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि अदालतें इस स्वतंत्रता की "लोकपाल" हैं और उसका "पूरे उत्साह से" संरक्षण करना उनका "पावन कर्तव्य" है। शीर्ष अदालत ने निजी स्वतंत्रता की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि जेलों में कुल कैदियों में से कम से कम दो तिहाई विचाराधीन कैदी हैं, जिनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। अदालत ने यह भी कहा कि ये ना सिर्फ गरीब और अनपढ़ हैं, बल्कि इनमें महिलाएं भी हैं। अदालत ने कहा कि भारत की दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 और 41ए में गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया बताई गई है और पुलिस अफसरों को इन धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को ऐसे अफसरों के खिलाफ कड़ी करवाई करने के निर्देश दिए जो इन धाराओं का अनुपालन किए बिना गिरफ्तारी करते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकारों से भी कहा कि इन धाराओं के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए वो स्थायी आदेश जारी करें। अदालत के अनुसार ब्रिटेन समेत कुछ देशों में ज़मानत के लिए अलग से कानून है। अदालत ने केंद्र सरकार से उसी तर्ज पर एक कानून भारत में भी लाने पर विचार करने के लिए कहा। इसके अलावा अदालत ने उच्च अदालतों से कहा कि वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे विचाराधीन कैदियों का पता लगाएं जिनकी गिरफ्तारी में सीआरपीसी में दी गई शर्तों का पालन नहीं हुआ और उनकी रिहाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।
क्या है देश में ज़मानत का नियम?
1977 में देश की सबसे बड़ी अदालत ने बेल को लेकर राजस्थान बनाम बालचंद मामले में अहम व्यवस्था दी थी। इसका जिक्र अक्सर किया जाता है। तब कोर्ट ने कहा था कि ज़मानत नियम और जेल अपवाद होना चाहिए। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने दो पन्नों के जजमेंट में कहा था कि सभी मामलों में बेल दी जानी चाहिए। इससे तभी इनकार किया जाना चाहिए जब आरोपी के भाग जानने, दोबारा अपराध दोहराने या गवाहों को प्रभावित करने का जोखिम हो। जस्टिस अय्यर ने गुदीकांती नरसिंमहुलु बनाम राज्य (1978) में भी दोबारा इस बात पर जोर दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि आजादी आरोपी का बुनियादी अधिकार है। चूंकि वह आरोप सिद्ध होने के साये में है, इसलिए उससे यह अधिकार नहीं छीना जा सकता है। इसेक बाद गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980) केस में ज़मानत देने की मंशा को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से समझाया था। तब यह कहा गया था कि दंडात्मक उपाय के रूप में ज़मानत को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि ज़मानत का उद्देश्य मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। ज़मानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए।
इसके बाद 1994 में जोगिंदर कुमार बनाम राज्य मामले में शीर्ष अदालत ने पुलिस की गिरफ्तार करने की ताकत के दुरुपयोग का जिक्र किया था। कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए जब तक यह संतोष न कर लिया जाए कि आरोपी के खिलाफ साक्ष्य प्रमाणित हैं। फिर डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल (1996) मामले में भी शीर्ष न्यायालय का यही रुख देखने को मिला था। कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तार और पूछताछ की शक्ति का इस्तेमाल नागरिक स्वतंत्रता के प्रावधानों का ख्याल रखकर किया जाना चाहिए।
वैसे 1882 में ड्राफ्ट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (सीआरपीसी) सीआरपीसी में बेल यानी ज़मानत को परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत सिर्फ कैटेगरी हैं। इनमें 'बेलेबल' (जमानती) और 'नॉन बेलेबल' (गैर-जमानती) शामिल हैं। सीआरपीसी मजिस्ट्रेटों को जमानती मामलों में बेल देने का अधिकार देती है। इसमें सिक्योरिटी या सिक्योरिटी के बिना बेल बॉन्ड पर रिहाई मिल जाती है। गैर-जमानती अपराध संज्ञेय होते हैं। ये वॉरंट के बगैर पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार देते हैं। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट तय करते हैं कि आरोपी को बेल दी जाए या नहीं।
सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी कई मायनों में ख़ास
गौरतलब है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2020 में भारत की जेलों में कुल 4,88,511 कैदी थे, जिनमें 3,71,848 यानी करीब 76 प्रतिशत विचाराधीन कैदी थे। इनमें से करीब 68 प्रतिशत या तो अशिक्षित थे या स्कूल छोड़ चुके थे। जाहिर है इन कैदियों की स्थिति चिंताजनक है। इनके साथ ही पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद और फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट 'ऑल्ट न्यूज' के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर जैसे अनेक लोगों की गिरफ्तारी भी सवालों के घेरे में है। 84 साल के स्टैन स्वामी के मामले में भी यही देखने को मिला। भीमा-कोरेगांव मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बीते साल ही 5 जुलाई को न्यायायिक हिरासत में ही उनकी मौत हो गई थी। जबकि 21 अप्रैल से उनकी ज़मानत याचिका हाई कोर्ट में लंबित थी। इसके अलावा कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी, कथित तौर पर सीएम ममता बनर्जी की मॉर्फ्ड पिक्चर पोस्ट करने वाली बीजेपी यूथ विंग एक्टिविस्ट प्रियंका शर्मा, स्टैंडअप कोमेडियन मुनव्वर फारूकी, पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता नताशा नरवाल, देवंगना कलिथा, नागरिग सत्याग्रह पदयात्रा पर निकले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र समेत तमाम छात्र और नागरिक समाज के लोग जेलों में कई दिन संघर्ष करने के बाद बाहर आए। ऐसे में सर्वोच्च अदालत की यह टिप्पणी और ये निर्देश कई मायनों में खास है।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।