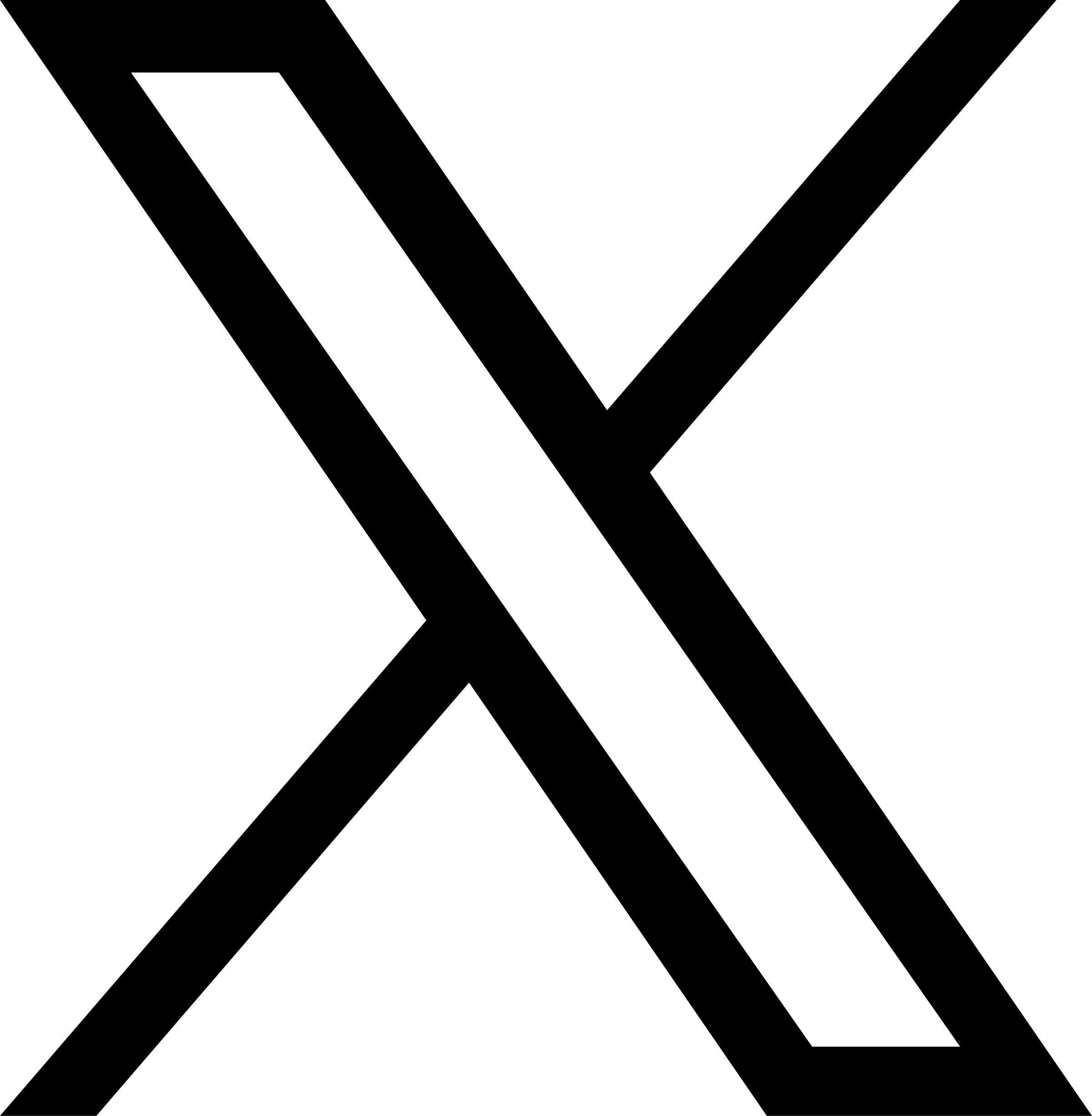IGMC: सार्वजनिक सेवा और पेशेवर नैतिकता पर ज़रूरी विमर्श

इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC), शिमला में घटित हुई मारपीट की घटना और उसके बाद के घटनाक्रम - निलंबन, बर्खास्तगी, चिकित्सकों की हड़ताल और फिर सामाजिक-राजनीतिक हस्तक्षेप से सुलह को केवल दो व्यक्तियों के बीच की झड़प के रूप में देखना इसकी गंभीरता को नजरअंदाज करना है।
यह घटना एक दर्पण है, जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, नैतिकता, सार्वजनिक सेवा के संकट और सामाजिक शक्ति-संरचनाओं की जटिल बुनावट को दिखाती है।
इसे समग्रता में समझने के लिए हमें व्यक्तिगत दोष से आगे बढ़कर उन व्यवस्थागत दरारों को भी देखना अनिवार्य है, जिनमें यह विवाद पनपा। और इसे पूरी तरह समझने के लिए, हमारी लोकप्रिय संस्कृति विशेषकर हिंदी सिनेमा ने जो चिकित्सकों के स्टीरियोटाइप्स गढ़े हैं, उन पर नज़र डालना भी उतना ही जरूरी है। हिंदी फिल्में ‘कबीर सिंह’ और ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ इस बहस के दो विपरीत ध्रुवों पर खड़ी हैं, और आईजीएमसी की घटना इन दोनों के बीच के संघर्ष की वास्तविक अभिव्यक्ति लगती है।
दरअसल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (IGMC), शिमला एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक डॉक्टर द्वारा मरीज को थप्पड़ मारते देखा गया। यह घटना 22 दिसंबर, 2025 को अस्पताल के पल्मोनरी वार्ड में डॉक्टर राघव नारुला और एक मरीज अर्जुन पवांर के बीच हुई। मरीज अर्जुन का कहना है कि पूरा विवाद ‘तू’ कहने से शुरू हुआ।
यह बात दुरुस्त है कि हिंदी डिक्शनरी में ‘तू’ शब्द का प्रयोग नकारात्मक नहीं है. फिर भी, सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि इसका प्रयोग एक स्पष्ट सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, और बौद्धिक हाइरार्की को दर्शाता है। इस पूरे विवाद की कुंजी 'तू' शब्द में छिपी है। चिकित्स्क ने मरीज के प्रति तू-तड़ाक और रुखा व्यवहार अपनाया जो मरीज को नापसंद रहा, जाहिर है रहना भी चाहिए था. और फिर उससे उपजा वो सारा विवाद व हिंसा।
इस घटना के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक संघ द्वारा उक्त चिकित्सक के बचाव में आयोजित की गयी एक प्रेस कॉन्फ्रेस में एक प्रतिनिधि द्वारा यह कहना कि हम-उम्र लोगों के बीच ‘तू’ कहकर बात करना "सामान्य" है - अपने आप में चिंताजनक है। लेकिन इससे भी अधिक चिंताजनक और अस्वीकार्य तथ्य यह है कि पूरे प्रदेश के मेडिकल संघ ने चिकित्सक राघव द्वारा मरीज पर किए गए शारीरिक हमले की स्पष्ट शब्दों में निंदा करने से पूरी तरह परहेज़ किया। जबकि यह पूरा मामला सोशल मीडिया के ज़रिये सार्वजनिक हो चुका था, तब भी मेडिकल संघों का “गलत” और “हिंसा” जैसे बुनियादी नैतिक प्रश्नों पर चुप रहना कोई साधारण चूक नहीं, बल्कि एक सूझी-बूझी संस्थागत खामोशी थी। यह खामोशी दरअसल जवाबदेही से बचने की रणनीति है, न कि किसी तटस्थता का प्रमाण।
पेशागत संगठनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सदस्यों का अंधा बचाव नहीं, बल्कि पेशे की नैतिक मूल्यों और मर्यादाओं की रक्षा करें। जब एक पूरा पेशागत समुदाय, खुले तौर पर सामने आई हिंसा के बावजूद, उसे गलत कहने का नैतिक साहस नहीं दिखा पाता, तो यह केवल किसी एक व्यक्ति की विफलता नहीं रह जाती, बल्कि पूरी मेडिकल कम्युनिटी के स्तर पर प्रोफेशनल एथिक्स का सामूहिक पतन बन जाती है। यह चुप्पी उस खतरे की ओर इशारा करती है, जहाँ पेशागत एकजुटता नैतिक विवेक से ऊपर रख दी जाती है और यहीं से संस्थाएँ अपने सामाजिक भरोसे को खोने लगती हैं। राघव ने जो हिंसा/ दुर्व्यवहार मरीज के साथ किया है वो स्पष्टत: अपराध की श्रेणी में आता है, और किसी भी अपराधी का अपराध देखकर सजा सुनिश्चित की जाती है न की उसके योग्यता, उपलब्धियो तथा योगदान को देखकर।
चलिए इसे समझने के लिए एक काल्पनिक परिदृश्य पर गौर करें। मान लीजिये कोई भी एक साधारण व्यक्ति या फिर कोई मरीज एक सरकारी अधिकारी या अस्पताल में किसी चिकित्सक के साथ उनकी ड्यूटी के दौरान उन्हीं के दफ्तर या कार्यस्थल पर तू-तड़ाक से पेश आता है, क्या उस अधिकारी को वह भी उतना ही "नार्मल" रहेगा जितना कि चिकित्स्क राघव द्वारा मरीज के प्रति व्यवहार को समझे जाने की चेष्ठा या अपेक्षा हो रही थी? क्या यह वाकई में स्वीकार्य रहेगा? शायद नहीं। उस अधिकारी को तुरंत अपनी पद, 'इज्जत' का एहसास होगा। ठीक यही एहसास एक मरीज को भी होता है जब एक सार्वजनिक सेवक उसके साथ इस लहजे में बात करता है। अस्पताल में प्रवेश करते ही मरीज की सामाजिक हैसियत, पेशा या उम्र गौण हो जाती है; वह सिर्फ एक 'पेशेंट' बन जाता है। क्या रोगावस्था में भी कोई व्यक्ति गरिमा और सम्मानजनक व्यवहार का पात्र नहीं रहता?
आइये पहले भाषायी ढांचे में हिंदी के "तू" शब्द के प्रयोग को समझते हैं. दरअसल यह शब्द हमारी सामाजिक संरचना में गहरे पैठे हुए वर्चस्व का सूचक है। यह एक औपनिवेशिक और सामंती विरासत है जहाँ भाषा का इस्तेमाल हाइरार्की बनाए रखने और अधीनस्थ की हैसियत याद दिलाने के लिए किया जाता रहा है। कोई "उच्च" पदासीन व्यक्ति अक्सर अपने से कम पद, कम आय, निम्न जाति या कम उम्र के व्यक्ति के प्रति 'तू' का प्रयोग अपनी श्रेष्ठता के प्रदर्शन के तौर पर करता रहा है। आईजीएमसी की इस घटना में, 'तू' डॉ. राघव के लिए शायद एक 'नॉर्मल' आदत रही हो, लेकिन मरीज के लिए यह संस्थागत अहंकार और अपमान का प्रतीक था, जो किसी मरीज को उसकी असहायता की भावना को और गहरा कर सकती है। और पंजाब, हरियाणा से भिन्न शिमला समेत पूरे हिमाचल प्रदेश में "तू" और "आप" का प्रयोग में स्पष्ट भिन्नता है। ऐसे मौकों पर "आप" ज्यादा अधिमान्य है।
कुछ इसी पूर्वाभ्यास को फिल्म ‘कबीर सिंह’ ने एक खतरनाक ग्लैमर प्रदान किया है। कबीर सिंह का चित्रण पेशेवर दक्षता के साथ-साथ एक भयंकर मैस्कुलिन/ अति पुरुषवादी व्यक्ति है जो बात-बात पर गुस्सा करता है, मारपीट करता है, न सम्मान की भाषा जानता है और न ही किसी तरह के एथिक्स। सिर्फ अपनी ईगो की संतुष्टि के लिए जीता हुआ प्रतीत होता है। आईजीएमसी के डॉ. राघव के व्यवहार में हमें 'कबीर सिंह' के इसी सिनेमाई आदर्शीकरण का एक वास्तविक प्रतिबिंब देखने को मिलता है। यह दर्शाता है कि कैसे लोकप्रिय संस्कृति पेशेवर पावर के दुरुपयोग को 'कूल' और 'शक्तिशाली' के रूप में सामान्य बना कर पेश कर सकती है।
इसके विपरीत, फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ प्रोफेसर अस्थाना के मुख से इसी अमानवीकरण की नीति को स्पष्ट शब्दों में कहलवाती है: “याद रखो, मरीज सिर्फ और सिर्फ एक बीमार शरीर है" यानी उससे जुड़ाव या "हमदर्दी" पेशे में शामिल नहीं। डॉ. राघव का 'तू' और हाथापाई, इस दृष्टिकोण की चरम परिणति है। जब मरीज सिर्फ एक 'बीमार शरीर' है, तो उस 'बॉडी' की भावनाएं, गरिमा या प्रतिक्रिया अप्रासंगिक हो जाती हैं। समस्या यह है कि यह 'बॉडी' इंसान है, और उस इंसान ने अपना अधिकार जताया, जिसका जवाब हिंसा के साथ दिया गया। निष्कर्षतः, 'तू' की यह लड़ाई केवल शब्दों की नहीं, बल्कि सम्मान, गरिमा और सार्वजनिक सेवा में शक्ति के समीकरण की लड़ाई है।
आधुनिक चिकित्सा पद्धति, अपनी उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति के बावजूद, पूँजीवादी उत्पादन-संबंधों के चंगुल में फँसती जा रही है। अस्पताल ‘सेवा केंद्र’ कम और ‘स्वास्थ्य उद्योग’ ज़्यादा लगने लगे हैं। मरीज ‘ग्राहक’ बन जाता है और डॉक्टर-मरीज का रिश्ता एक लेन-देन का समझौता। इस व्यवस्था में करुणा, धैर्य और सहानुभूति जैसे मानवीय मूल्य गौण हो जाते हैं। इस तथ्य के तमाम उदाहरण आप अपने आसपास लगभग प्रतिदिन घटते हुए अवश्य देखते होंगे।
बहरहाल, चिकित्स्क राघव का व्यवहार इसी नैतिक खोखलेपन का प्रतीक है। चिकित्सा नैतिकता की पहली शर्त है ‘प्राइमम नॉन नोसेरे’ – सबसे पहले, कोई नुकसान न पहुँचाए। यह नुकसान केवल शारीरिक नहीं, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भी हो सकता है। एक पीड़ित, संभवतः मानसिक रूप से कमज़ोर मरीज के साथ ‘तू-तड़ाक’ और फिर हाथापाई करना, इस मूल सिद्धांत की घोर अवहेलना है। यह दर्शाता है कि पेशेवर प्रशिक्षण में क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर तो ज़ोर दिया जाता है, लेकिन ‘बेडसाइड मैनर्स’ और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को गंभीरता से नहीं सिखाया जाता। 'मुन्ना भाई' के प्रोफेसर का लेक्चर इसी भावनात्मक निषेध के कुतर्क को व्यवस्थित रूप देता है, जिसके खिलाफ फिल्म स्वयं विद्रोह करती है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु की अध्यक्षता में घटना की जाँच के लिए नई कमिटी का गठन। फ़ोटो साभार: द न्यूज़ हिमाचल
घटना के बाद की प्रतिक्रियाएँ भी एक दिलचस्प सामाजिक नाट्य प्रस्तुत करती हैं। प्रशासन की झटकेदार प्रतिक्रिया पर गौर करते हैं: पहले निलंबन और फिर तत्काल बर्खास्तगी, सार्वजनिक रोष और मीडिया दबाव में लिया गया एक आत्मरक्षात्मक कदम लगता है। यह प्रदर्शित करता है कि प्रशासनिक तंत्र अक्सर संकट प्रबंधन के लिए सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि तात्कालिक जनता की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। बर्खास्तगी एक गंभीर दंड है, और इसे बिना गहरी पारदर्शी जांच के लागू करना स्वयं एक प्रशासनिक दोष है।
चिकित्सक समुदाय द्वारा तत्काल हड़ताल पर जाना एक सामूहिक पहचान की रक्षा का कृत्य था। यहाँ दो बातें सामने आती हैं: पहला, एक ‘साथी की गलती पर भी एकजुट रहने’ की सामंती/यूनियन संस्कृति, जो पेशेवर जवाबदेही के आगे एक आडंबर खड़ा करती है। दूसरा, चिकित्सकों की वास्तविक शिकायतें—जैसे अत्यधिक कार्यभार, अपर्याप्त सुरक्षा, और प्रशासनिक समर्थन की कमी—जो इस एक घटना के माध्यम से विस्फोटित हो गईं। हड़ताल ने अस्पतालों को ठप करके एक सामूहिक वार्ता की शक्ति (collective bargaining power) प्रदर्शित की। और यहाँ से घटना का सबसे क्षेत्रीय पहलू सामने आता है। मुख्यमंत्री की मध्यस्थता और अंततः दोनों पक्षों की माफ़ी व सुलह का मार्ग न केवल हड़ताल के दबाव का परिणाम था, बल्कि इसमें कुछ और सूक्ष्म कारक भी शामिल थे। ‘हिमाचल जैसे अपेक्षाकृत छोटे और सामाजिक रूप से जुड़े समाज में, व्यक्तिगत संबंध और सामुदायिक दबाव एक भूमिका निभाते हैं। संभव है कि डॉ. राघव के परिवार या संबंधियों ने उच्च स्तर पर पैरवी की हो, और ‘एक युवा की करियर एक गलती से बर्बाद न होने दें’ जैसी भावनात्मक अपील का असर हुआ हो। यह ‘दरियादिली’ या ‘माफी’ की भावना प्रशासनिक कठोरता पर भावनात्मक संबंधों और पारस्परिक पहचान की जीत दिखाती है। प्रशासन के लिए यह एक व्यावहारिक निकास (pragmatic exit) था। एक तरफ मरीजों की पीड़ा बढ़ रही थी, दूसरी तरफ हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएँ चरमरा गई थीं। ऐसे में, एक ‘समझौता’ सबसे कम राजनीतिक कीमत वाला रास्ता था। इसमें दोनों पक्षों को माफ़ी दिलाकर और सेवा बहाली का आश्वासन देकर तात्कालिक आग को बुझाया गया। हालांकि यह सुलह ‘मानवीय’ और ‘व्यावहारिक’ लग सकती है, लेकिन यह पेशेवर जवाबदेही (professional accountability) के सिद्धांत को गंभीर रूप से कमजोर करती है। एक गंभीर अनुशासनात्मक और संभावित आपराधिक मामला, जिसमें एक सार्वजनिक सेवक का मरीज से हाथापाई शामिल है, को ‘आपसी झगड़ा’ बता कर सुलझा लेना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। इससे यह संदेश जाता है कि संगठित शक्ति, राजनीतिक पहुँच और सामुदायिक लॉबीिंग गंभीर गलतियों के परिणामों को धुंधला कर सकती है। यह सुलह न्यायिक प्रक्रिया के बजाय एक राजनीतिक-सामाजिक समाधान था।

चिकित्सक और मरीज़ के बीच करवाई गई सुलह। फ़ोटो साभार : डेक्कन हेराल्ड
इस घटना से सबक लेते हुए, केवल एक डॉक्टर को दंडित या माफ़ करने से आगे बढ़कर व्यवस्थागत और सांस्कृतिक सुधार की ओर देखने की आवश्यकता है. मेडिकल शिक्षा में व्यावहारिक परिवर्तन की सख्त जरूरत है. मेडिकल पाठ्यक्रम में ‘मुन्ना भाई’ के दर्शन की भावना को शामिल करना होगा। सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, मेडिकल एथिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस को अनिवार्य और मूल्यांकन योग्य कोर कॉम्पीटेंसी बनाना होगा। डॉक्टर अस्थाना के लेक्चर को एक चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए, न कि एक पाठ के रूप में।
समाज और खासकर युवा चिकित्सकों को ‘कबीर सिंह’ जैसे टॉक्सिक रोल मॉडल से बचाना अत्यंत जरुरी है। यह बात ठीक से समझी जानी है कि पेशेवर सफलता और मानवीय संवेदनशीलता परस्पर विरोधी नहीं हैं। एक आदर्श डॉक्टर वह है जो कुशल भी है और करुणामय भी। यह सांस्कृतिक बदलाव समाज, मीडिया और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर लाना होगा। सभी सरकारी कर्मचारियों, समेत स्वास्थ्यकर्मियों के लिए ‘गरिमामय व्यवहार’ (Dignified Conduct) को सेवा शर्त का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना जरुरी है। इसके लिए निरंतर प्रशिक्षण और एक स्पष्ट आचार संहिता होनी चाहिए। मरीजों और कर्मचारियों दोनों के लिए एक त्वरित, पारदर्शी और निष्पक्ष आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ होना चाहिए, ताकि विवादों को अदालत या मीडिया में जाने से पहले ही निष्पक्षता से देखा, जाँचा और न्याय किया जा सके।
डॉक्टरों/ चिकित्सकों पर रोगी भार कम करना, सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत करना, पर्याप्त मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त स्टाफिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना ज़रूरी है जोकि किसी भी राज्य में शासन-प्रशासन की अहम जिम्मेदारी है। अन्यथा, एक थके-हारे तनावग्रस्त और असुरक्षित डॉक्टर / चिकित्स्क की व्यावहारिक संवेदनशीलता हर वक्त स्टेक पर हो सकती है ।
किसी भी पेशेवर व्यक्ति का अपने लाभार्थियों और हितधारकों के प्रति संवेदनशील तथा सहानुभूतिपूर्ण होना एक बुनियादी और अनिवार्य शर्त है। सरकारी डॉक्टर/चिकित्सक भी इसका अपवाद नहीं हैं। वे किसी भी राज्य में तुलनात्मक रूप से वेल-पेड होते हैं और उनके प्रशिक्षण तथा सेवाओं पर सार्वजनिक धन—अर्थात आम जनता के टैक्स से बने सरकारी खजाने का खासा हिस्सा खर्च होता है। जब सरकार किसी पेशे से जुड़े अधिकांश खर्चों को वहन करती है, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि वे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आम जनता को सेवाएँ देने के लिए हैं। इसलिए सभी सरकारी वेतनभोगी, विशेषकर चिकित्सक, सीधे तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह हैं और उनकी नियुक्ति का मूल उद्देश्य जनसेवा है।
अन्ततः यह कहा जा सकता है कि आईजीएमसी की यह घटना केवल हिमाचल की नहीं, बल्कि देश के समूचे सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र और सार्वजनिक सेवा के लिए आत्ममंथन की एक गंभीर चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि तकनीकी दक्षता के बिना नैतिक संवेदनशीलता खोखली है, और नैतिक संवेदनशीलता के बिना तकनीकी दक्षता खतरनाक हो सकती है। किसी भी तरह की हिंसा का प्रयोग, हाथापाई, हड़ताल और अंतिम सुलह—ये सभी चरण एक बड़ी कहानी के अध्याय हैं। यह कहानी है अधिकार, सत्ता, सामर्थ्य और प्रभुत्व के दुरुपयोग, संस्थागत जवाबदेही के अभाव, एक ऐसी प्रणाली की जो संकट आने पर दंड या समझौता तो कर लेती है, पर स्थायी सुधार के लिए संरचनात्मक बदलाव से कतराती है, उसमें फेल हो जाती है, और उन सांस्कृतिक संकेतों की जो पेशेवर हिंसा को रोमांटिसाइज करते हैं।
असली इलाज इस बीमार प्रणाली का है। और इस इलाज का पहला कदम है ‘कबीर सिंह’ की अहंकारी विरासत को त्यागकर ‘मुन्ना भाई’ की मानवीय ‘झप्पी’ के दर्शन को अपनाना - न सिर्फ अस्पतालों के वार्डों में, बल्कि हमारी मेडिकल शिक्षा, हमारे सिनेमा, हमारे प्रशासन और हमारी सामूहिक समझ में। क्योंकि अंततः, हर मरीज सिर्फ एक बीमार शरीर नहीं, एक इंसान है जिसका अपना आत्मसम्मान है और सिर्फ जीने ही नहीँ बल्कि सम्मान से जाने की चाह भी। और हर सार्वजनिक सेवक सिर्फ एक वेतनभोगी नहीं, एक जवाबदेह सेवक है। उनके बीच का रिश्ता केवल लेन-देन का नहीं, विश्वास और गरिमा का होना चाहिए। उसी विश्वास की पुनर्स्थापना ही इस घटना से निकलने वाला सबसे बड़ा सबक है।
(लेखक अंग्रेजी के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं और समय-समय पर समकालीन सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।