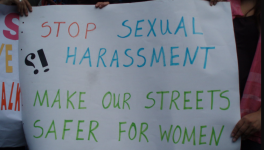लैंगिक बजट: केंद्र को केरल से क्या सीखने की ज़रूरत है?
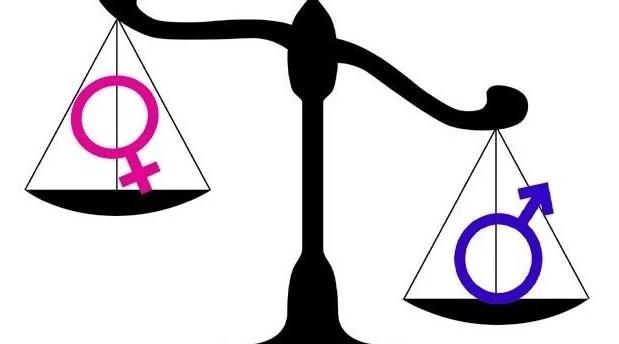
किसी भी देश के केंद्रीय बजट से उस देश की महिलाओं को सहायता मिलने और बढ़ती लैंगिक असमानताओं को कम करने की अपेक्षा की जाती है। लैंगिक असमानताएं, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कम शैक्षणिक भागीदारी, कम वेतन भत्तों, संपदा-संसाधन तक कम पहुंच के जरिए प्रदर्शित होती हैं।
"2018 के UNDP लैंगिक असमानता पैमाने" पर भारत की स्थिति 162 देशों में 122 वीं थीं। भारत ना केवल इस सूची में सबसे आगे रहने वाले नार्वे से बहुत पीछे था, बल्कि चीन (39), श्रीलंका (86), भूटान (99) और म्यांमार (106) से भी बहुत पीछे था।
UNDP के इस पैमाने में स्वास्थ्य, राजनीतिक सशक्तिकरण और संबंधित देशों के श्रम बाज़ार में महिलाओं की भागीदारी को शामिल किया जाता है। इससे पता चलता है कि भारत तीनों ही आयामों में काफ़ी पीछे था। यह हमारे समाज में श्रम के साथ-साथ दूसरे क्षेत्रों में व्याप्त असमता को दिखाता है।
जब 2020 में जब सरकार ने लैंगिक बजट का दस्तावेज़ जारी किया, तो काफ़ी आशाएं लगाई जा रही थीं। लेकिन बजट में किए गए आवंटन भारतीय समाज के पितृसत्तात्मक ढांचे को बदलने में नाकामयाब रहा है। जबकि यही पितृसत्तात्मक ढांचा लैंगिक असमानता का मूल कारण है। इसलिए समस्या से निपटने के लिए जिस स्तर पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, वह नहीं की गई।
केरल बजट ने कुछ मुद्दों का समाधान किया है, जिससे असमान तरीके से बंटे हुए संसाधनों की समस्या का कुछ हद तक हल हो सकता है। लेकिन यह बजट राष्ट्रीय बजट की तुलना में काफ़ी कम है। इस लेख में हम दो मुद्दे उठाएंगे, जो 2020 के लैंगिक बजट में शामिल हैं, हम उनकी केरल की प्रगतिशील प्रक्रिया से तुलना करेंगे। केरल बजट के दस्तावेज़ में वह दिशानिर्देश भी शामिल हैं, जिनमें बताया गया है कि कैसे इस मुद्दे का समाधान किया जाएगा और कैसे लैंगिक असमानता से उपजने वाले नतीजों को हल किया जा सकता है।
बजट आवंटन में दिखावा: लैंगिक समस्या को दरकिनार किया गया
लैंगिक बजट, 2020 में जितना पैसा दिया गया, वह कुल बजट आवंटन के पांच फ़ीसदी से भी कम है। लैंगिक बजट पेश करने के 15 साल बाद भी ऐसा किया जाना सिर्फ़ दिखावे का प्रतीक है। यह लैंगिक भेद को दूर करने में केंद्र की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दिखाता है। दूसरी तरफ केंद्र की तुलना में बहुत कम संसाधनों वाले केरल में कुल बजट आवंटन का 18.4 फ़ीसदी हिस्सा राज्य लैंगिक बजट के लिए आवंटित किया गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक विकास, महत्वकांक्षाओं की पूर्ति और 'सेवा करने वाला समाज' को लैंगिक असमानता को दूर करने वाले तीन स्तंभ बताए। यह ऊपरी तौर पर आदर्श नज़र आते हैं, लेकिन जब इन्हें अलग-अलग करके देखा जाता है, तो यह दावे भ्रामक नज़र आते हैं।
'जेंडर बजट स्टेटमेंट-GBS' को दो हिस्सों में बताया जाता है: (अ) ऐसी सरकारी योजनाएं, जिनमें आवंटित पैसे का 100 फ़ीसदी इस्तेमाल महिला कार्यक्रमों में होता है। इन्हें पार्ट-A आवंटन कहा जाता है। (ब) GBS के पार्ट-B आवंटन में वह पैसा शामिल होता है, जिनमें किसी सरकारी योजना का 30 से 99 फ़ीसदी आवंटन महिलाओं के लिए होता है।
भारत में, 2020-21 के दौरान, पार्ट-A में सिर्फ़ 28,568 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ, जो कुल लैंगिक बजट आवंटन का सिर्फ़ 19 फ़ीसदी था। मतलब महिलाओं के लिए जो लैंगिक बजट पेश किया गया, उसका 19 फ़ीसदी हिस्सा ही ऐसा है, जो पूरी तरह सिर्फ़ महिलाओं की भलाई के लिए उपयोग किया जाएगा। GBS का बाकी 1.14 लाख करोड़ रुपये का आवंटन दूसरे हिस्से (पार्ट-B) में शामिल योजनाओं से आता है। मतलब अलग-अलग मंत्रालयों की योजनाओं से। यहां बड़ी समस्या मंत्रालयों का भागीदारी में ढीला-ढाला रवैया है। केवल 18 विभागों और मंत्रालयों ने ही GBS के तहत आवंटन किए हैं। ज़्यादातर आवंटन (एक तिहाई) ग्रामीण विकास मंत्रालय और महिला एवम् बाल विकास मंत्रालय की तरफ से किए गए हैं।
मौजूदा लैंगिक असमानताओं को बजट नीतियों के ज़रिए समझने और उन्हें दूर करने के लिए जरूरी है कि सभी मंत्रालय और विभाग "अनिवार्य" तौर पर आवंटन करते वक़्त एक लैंगिक नज़रिया अपनाएं। दूसरी बात, जैसा 'इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डिवेल्पमेंट' की हेड आशा कपूर मेहता कहती हैं, जिन योजनाओं की ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा घोषणा होती है, वह सिर्फ़ महिला केंद्रित नहीं होतीं। ऊपर से GBS के पार्ट-A में होने वाले आवंटन (जो सिर्फ़ महिलाओं के लिए होना चाहिए) में प्रधानमंत्री आवास योजना भी शामिल है। जबकि यह योजना 100 फ़ीसदी महिलाओं के लिए नहीं है। यह तो सामान्य तौर पर भी सिर्फ़ महिलाओं की जरूरत को पूरा नहीं करती।
ऊपर से इन योजनाओं में उपयोग ना किए जा सकने वाले पैसे की दिक्कत भी आती है। उदाहरण के लिए 2019-20 में महिला एवम् बाल विकास मंत्रालय अपने हिस्से का 667 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाया। हम GBS को लेकर जो दिखावटीपन देखते हैं, दरअसल वो लैंगिक नज़रिए के प्रति कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति का नतीज़ा है।
ज़रूरत है कि कर्मचारी के तौर पर पहचान मिले: नहीं दिया जा रहा बकाया
केरल का लैंगिक बजट एक नज़रिए से केंद्र से अलग है। केरल का बजट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्टार्ट-अप मिशन (जिसमें "केरला वीमेन इन स्टॉर्ट अप्स" भी शामिल है) के साथ-साथ गैर-IT सेक्टर में अलग-अलग तरह से महिलाओं की कर्मचारी के तौर पर जरूरत को बढ़ावा दे रहा है। इसमें KSIDC की नवोन्मेषी योजनाएं भी शामिल हैं। केरल के बजट में से 12 करोड़ रुपये उद्योग विभाग को आवंटित होते हैं, जिसमें छोटे उद्यमियों को सहायता देने के लिए राशि भी शामिल है। साथ में 2 करोड़ रुपये मल्टी-स्टोरी इंडस्ट्रियल एस्टेट का नेतृत्व करने वाली महिला उद्यमियों के लिए भी दिए जाते हैं।
यह अंतर केरल और केंद्र में विचारधारा की स्थिति में फर्क के चलते हैं। कैसे दोनों सरकारें भविष्य के समाज के लिए महिलाओं की भूमिका और उनके अधिकारों को देखती हैं, वह लैंगिक बजट से व्यवहार करने के दोनों के तरीकों में दिख जाता है। गौर करें कि केंद्रीय बजट के उपशीर्षक "महिला, बाल और सामाजिक कल्याण (अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग)" के वर्ग "केयरिंग सोसायटी" में ही महिलाओं का ज़्यादातर जिक्र है। 2020-21 का लैंगिक बजट, महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को "केयरिंग सोसायटी" जैसी सनक तक सीमित कर देता है, इसमें महिला आंदोलनों के कई दशकों के संघर्ष से हासिल ज़मीन को दरकिनार कर दिया गया। यह संघर्ष का ही नतीज़ा था कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं की कर्मचारियों के तौर पर जरूरत को दो बार मान्यता दी गई। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास का वायदा किया गया था। उस पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि अर्थव्यवस्था में किए गए ढांचागत् बदलावों से महिलाओं पर 'प्रतिरोधी प्रभाव" पड़ रहा है। अब केंद्रीय बजट फिर लैंगिक ज़िम्मेदारी के लिए केयर (परवाह) शब्द को शामिल कर महिलाओं के काम को "स्वैच्छिकता या स्वाबलंबन" से जोड़ रहा है।
यह बताता है कि भारत में पितृसत्तात्मक चीजों का कैसे नीतिगत् दस्तावेज़ों के साथ सामंजस्य बनाया जाता है और यह किस तरह असली काम करने वाली महिलाओं पर असर डालता है। उदाहरण के लिए तमाम तरह की सामाजिक सुविधाएं प्रदान करने वाली ASHA और आंगनवाड़ी महिलाकर्मी आज भी "स्वयंसेवी/वालेंटियर" ही बनी हुई हैं, जिसके चलते ना तो उनके पास पेशेवर सुरक्षा मौजूद है और ना ही उन्हें नियमित वेतन मिलता है। यहां तक कि उन्हें कर्मचारी के तौर पर भी मान्यता प्राप्त नहीं है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर सुविधा देने वाले काम को वैतनिक काम में बदलने की अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। इस तरह वह मौका भी खो दिया, जिसके ज़रिए महिलाओं के लिए कम होती नौकरियों के सवाल को हल किया जा सकता था। महिलाओं के लिए कम होते मौके, श्रमशक्ति भागीदारी की उनकी गिरती दर से प्रदर्शित हो जाती है।
केरल लैंगिक बजट में महिलाओं को कर्मचारियों के तौर पर मान्यता दी गई है। महिलाओं के लिए कोझीकोड के जेंडर पार्क (महिला एवम् बाल विकास के अंतर्गत) में 2020-21 के लिए इंटरनेशनल वीमेन्स ट्रेड सेंटर (IWTC) नाम के एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लगाने की योजना है। इसके लिए आवंटित 200 करोड़ रुपये के अलावा, आजीविका उद्धार के लिए 250 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन की घोषणा की गई है। बिना वांछित वेतन के "सुविधा", या अवैतनिक स्वयंसेवी के तौर पर "सुविधा" देने के चलते भारत में महिलाओं पर बहुत भार पड़ा है। इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को स्मार्टफोन देने से, जबकि उसकी पेशेवर सुरक्षा निश्चित नहीं किया जाता या उसके भत्तों को हिस्से में देने की व्यवस्था होती है, उसकी कर्मचारी के तौर पर स्थिति बेहतर नहीं हो सकती है।
केंद्रीय GBS को, केरल की तरह, महिलाओं द्वारा उठाए जाने वाले असमान भार का समाधान करना था और उन्हें वैतनिक काम देना था। GBS महज़ दिखावा है, जो पितृसत्तात्मक समाज की तरह "सेवा" प्रदान करने वाले कामों को महिलाओं के जिम्मे डाल देता है, जबकि ना तो उन्हें नौकरी में सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है और महिलाओं को वेतन भी कम दिया जाता है। इन तरह के प्रावधानों से निकट भविष्य में देश को लैंगिक समानता का लक्ष्य कतई हासिल नहीं होगा।
लेखक स्कूल ऑफ़ मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ़ हैदराबाद में पोस्टग्रेजुएट छात्र हैं। यह उनके निजी विचार हैं।
इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।