उत्तराखंड का नया लिव-इन-रिलेशनशिप क़ानून किसके लिए है?
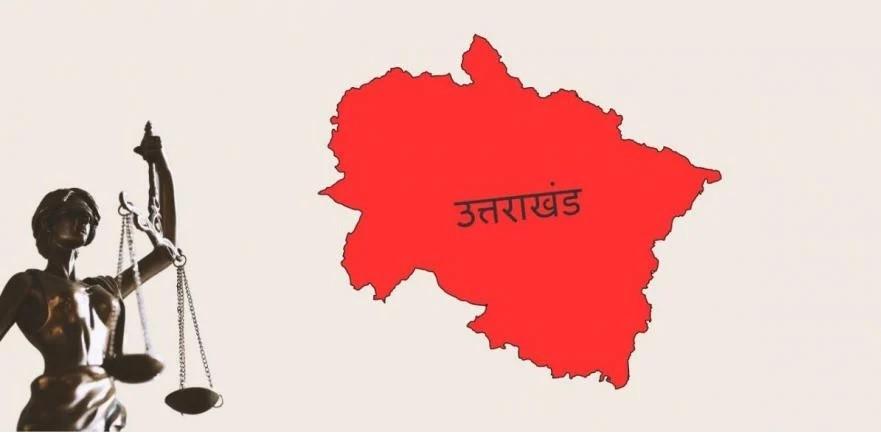
जब कोई हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से प्रेरित होकर बनाए गए उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक की तीन सौ सतहत्तर धाराओं को पढ़ना समाप्त करता हैतो उसे भारतीय कानून के इतिहास की एक विचित्र और नई चीज़ का सामना करना पड़ता है।
भाग-3 इस व्यापक कानून का वह एक अध्याय है जो लिव-इन संबंधों को रेगुलेट करने के लिए समर्पित है।
क़ानून में इस तरह का एक नया और आधुनिक जोड़ उस चीज को कानूनी मान्यता देता है जो अब तक भारतीय समाज और कानून दोनों में वर्जित थी। स्वाभाविक रूप से यह बहुत उत्साह पैदा करती है।
कई वकीलों और विशेषज्ञों की टिप्पणियां और स्पष्टीकरण यहां और यहां पढे जा सकते हैं। लेकिन इसके प्रावधानों और स्थापित कानून की एक साथ थोड़ी सी भी जांच करने से यह सवाल उठता है कि: यह प्रस्तावित कानून किसके लिए है? इससे क्या हासिल होगा, क्या इससे मदद मिलेगी और यह काम कैसे करेगा?
विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है कि यह किन महिलाओं की मदद करना चाहता है
लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं का शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से शोषण होना आम बात है। खंड 3(4)(बी) लिव-इन संबंधों को "साझा घर" में "विवाह की प्रकृति वाले संबंध" के रूप में परिभाषित करता है।
इस पूर्व वाक्यांश को अपरिभाषित छोड़ दिया गया है, जो हमें इसके अर्थों के सुराग खोजने के लिए प्रेरित करता है जहां यह वर्तमान में मौजूद है: यह, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 है।
इस अधिनियम में, उन महिलाओं के दायरे का विस्तार किया गया है जो विवाह की प्रकृति के रिश्ते में रह रही हैं और जिन्हें इस क़ानून के ज़रिए संरक्षित किया जा सकता है। लेकिन इसमें किसे शामिल किया जाए यह तय करना विवाद का विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कुछ मानदंडों के आधार पर लिव-इन रिलेशनशिप ऐसे रिश्तों का हिस्सा हो सकता है। अर्थात्, साझा घर में रहने के साथ-साथ, उन्हें यह करना होगा:
1. समाज के सामने खुद को जीवनसाथी के समान माने।
2. उनकी उम्र विवाह करने की हो।
3. अविवाहित होने सहित कानूनी विवाह में दाखिल होने के लिए योग्य होना।
4. स्वेच्छा से सहवास करना और दुनिया के सामने खुद को लंबे समय तक जीवनसाथी के समान दर्शाना।
क़ानून की इस व्याख्या की वजह से संभावित रूप से अपमानजनक रिश्तों में कई महिलाओं को असुरक्षित छोड़ दिया गया है। सबसे पहले, यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या बहुत संकीर्ण थी, क्योंकि अदालत ने पहले ही, पिछले निर्णयों में, घोषित कर दिया था कि लंबे समय तक एक साथ रहने वाले महिला और पुरुष को मेंटेनेंस के लिए एक-दूसरे से विवाहित माना जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे स्पष्ट रूप से "विवाह की प्रकृति" में साथ रहने वालों, जिसे "कीप" कहा जाता है, के बारे में यह भी कहा है कि सभी लिव-इन रिश्ते विवाह की प्रकृति में नहीं होंगे यानि उन्हे विवाह के समान नहीं माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या यह जांच करने की कोशिश करती है कि क्या कोई रिश्ता विवाह जैसा दिखता है, न कि इस बात की ओर कि क्या किसी रिश्ते में किसी दुरुपयोग की संभावना है।
घरेलू हिंसा अधिनियम (डी वी एक्ट) ने केवल पहले से ही विवाहित पुरुष के साथ रिश्ते में महिलाओं को शामिल करने के लिए "पत्नी" शब्द की परिभाषा का विस्तार करने के लिए मलिमथ समिति की रिपोर्ट की सिफारिश का सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं किया था।
इसमें स्पष्ट रूप से "विवाह की प्रकृति" वाक्यांश जोड़ा गया है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि समिति की चिंता लिव-इन रिलेशनशिप नहीं बल्कि उन महिलाओं के बारे में थी जो दोहरे विवाह में थीं, जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी क्योंकि ऐसी महिलाओं का पुरुषों द्वारा शोषण किया जाता था। इसके बावजूद, कई अपमानजनक रिश्तों को सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से बाहर रखा गया।
तब कोई यह कह सकता है कि शायद विधेयक का भाग-3 सटीक रूप से इस बात को संबोधित करता है: यह संदेह से परे है कि जो महिलाएं महत्वपूर्ण समय और प्रतिबद्धता वाले रिश्ते में हैं, लेकिन शादी के करीब नहीं हैं, उन्हें कानून का लाभ मिलेगा।
इसमें साथ रहने वालों जोड़ों के साथ-साथ वे रिश्ते भी शामिल हो सकते हैं जिनमें महिलाओं का शोषण होने की संभावना होती है, भले ही वे विवाह के समान हों। लेकिन विधेयक के पाठ में "विवाह की प्रकृति" की परिभाषा में किए गए बदलावों और बदले में विरोधाभास पैदा करने के कारण इसका समर्थन करना कठिन हो जाता है।
लिव-इन के मतलब को लेकर असमंजस
सबसे पहले, विधेयक में निम्नलिखित के बीच एक महत्वपूर्ण मिश्रण है: 1) विवाह की प्रकृति पर कानून, 2) लिव-इन रिलेशनशिप की परिभाषा, 3) लिव-इन रिलेशनशिप का समाज के लिए क्या मतलब है।
विवाह की प्रकृति एक शर्त है कि लिव-इन रिलेशनशिप क्या है, जिसमें महत्वपूर्ण समय शामिल है (उपरोक्त शर्त 4)। लेकिन क्लॉज387 यह भी मांग करता है कि लिव-इन रिलेशनशिप को एक महीने के भीतर पंजीकृत किया जाए।
तो फिर यह कौन सा है, एक महीना या महत्वपूर्ण समय? भले ही यह पहले वाला ही क्यों न हो, केवल एक महीने में समाज के लिए जीवनसाथी (उपरोक्त शर्त 1) जैसा दिखने वाला रिश्ता हासिल करना मुश्किल है।
परिभाषा विवाह पर विचार कर रही है जबकि खंड 387 चीजों को आकस्मिक रखना चाहता है। ऐसा लगता है कि विधेयक के दोनों प्रावधानों को एक-दूसरे से अपने संबंधों के बारे में मुख़ातिब होने की ज़रूरत है।
दूसरा, परिभाषा अव्यावहारिक हो सकती है। यदि हम दो लोगों को उनके रिश्ते के बारे में कैसा महसूस करते हैं, इसके आधार पर जीवनसाथी के समान होने का आकलन करते हैं, तो यह चीजों को और अधिक जटिल बना देता है।
एक जोड़ा अनिश्चित काल तक एक साथ रह सकता है यदि उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वे जीवनसाथी हैं। एक महीने से अधिक समय तक अपंजीकृत लिव-इन संबंधों का अपराधीकरण असंभव हो जाएगा। यहां तक कि अगर उनके रिश्ते में किसी बिंदु पर, जोड़े ने फैसला किया है कि उनका रिश्ता 'विवाह के समान' है, तो कानून की अदालत के लिए यह निर्धारित करना मुश्किल होगा कि यह तारीख एक महीने की पंजीकरण अवधि की गणना कब से शुरू होगी।
ऐसा लगता है कि कानून इस बात को लेकर भ्रमित है कि वह किसकी मदद करना चाहता है। अगर यह महिलाओं की मदद करना चाहता है तो किस तरह के रिश्ते वाली महिलाएं? दोहरे विवाह में रहने वाली? एक-साथ रहने वाली? व्यभिचारी? परिस्थितियां? 'रिश्ते की प्रकृति' की स्पष्ट परिभाषा की कमी पहले से ही समस्याएं पैदा कर रही है, जैसे कि न्यायाधीशों ने द्विविवाह में महिलाओं को भी शामिल करने से रोकने के लिए नए मानदंडों का आविष्कार किया है।
नया कानून इन समस्याओं को और बढ़ा देता है। यह एक मुख्य वाक्यांश को अपरिभाषित छोड़ देता है लेकिन वाक्यांश के कानूनी रूप से कथित अर्थ के साथ विरोधाभास भी डाल देता है। यह महिलाओं को लिव-इन रिलेशनशिप से भरण-पोषण का दावा करने में सक्षम बनाना चाहता है, फिर भी उन्हें इस तरह से परिभाषित करता है कि यह सबसे अच्छे रूप में विवेकपूर्ण और सबसे खराब रूप से अव्यवहारिक हो जाता है।
फिर यह कहना मुश्किल है कि भाग-3 महिलाओं की किस प्रकार मदद करेगा, या तो वर्तमान कानून से अधिक या बिल्कुल भी नहीं। कानून के लिए, कानून को संहिताबद्ध करना पूरी तरह से स्वीकार्य है।
लेकिन नए प्रावधानों को पेश करने में, कानून मौजूदा कानून को खत्म कर देता है, कार्यान्वयन को कठिन बना देता है और पहले से ही न्यायिक विवेक से प्रभावित क्षेत्र में विवेक की गुंजाइश बढ़ जाती है।
महिलाओं को भरण-पोषण के माध्यम से परित्याग से बचाने के लिए सहायता सुनिश्चित करने के लिए "लिव-इन रिलेशनशिप को विनियमित करने" के अपने उद्देश्य में, यह व्यापक प्रावधान बनाता है, जिससे उत्पीड़न की पर्याप्त संभावना पैदा होती है।
सबसे विचित्र समलैंगिक विरोधी कानून'
पिछले साल, सुप्रियो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि समलैंगिक जोड़े शादी करने के अधिकार के हकदार नहीं हैं। मुख्य कारण यह है कि विवाह एक धार्मिक संस्था होने के कारण इसमें हस्तक्षेप करना अदालत की शक्तियों से बाहर है।
समलैंगिकों के लिए सिविल यूनियन या आम कानूनी विवाह की संभावना को भी बहुमत जजों द्वारा संसद या कार्यपालिका द्वारा नीतिगत निर्णय न होने के कारण खारिज कर दिया गया था, और कहा कि यह अदालत के हाथों में नहीं है। मजे की बात यह है कि यहां धर्म कारण नहीं था।
समलैंगिक लोग इस विधेयक के प्रमुख लाभार्थी हो सकते थे। इससे पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक समलैंगिक जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया था। घुसपैठ की एक डिग्री और राज्य की मान्यता के साथ एक पंजीकृत लिव-इन रिलेशनशिप इसे एक सिविल यूनियन के समान बना देगा। "विवाह की प्रकृति" की अनुमानित परिभाषा वैसे भी सामान्य कानून विवाह की परिभाषा से ली गई है।
लेकिन विधेयक दो लोगों के बीच लिव-इन संबंधों को परिभाषित करता है: एक पुरुष और एक महिला। बहुपत्नी, समलैंगिक, समलैंगिक, गैर-बाइनरी, ट्रांसजेंडर और, कई मामलों में, उभयलिंगी संबंधों को कानून के लाभों से बाहर रखा गया है।
बाइनरी ट्रांस-पुरुषों और ट्रांस-महिलाओं को संभावित रूप से शामिल किया जा सकता है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह घोषणा की गई है कि सभी व्यक्तिगत कानूनों में उन्हें सुप्रियो में "पुरुष" और "महिला" की परिभाषाओं में शामिल किया जाएगा।
व्यक्तिगत संबंधों में राज्य की महत्वपूर्ण घुसपैठ को देखते हुए, अधिकांश समलैंगिक व्यक्ति बाहर किए जाने से खुश हो सकते हैं।
लेकिन जो दिलचस्प बात सामने आती है वह वही है जो सुप्रियो की कार्यवाही पर लटकी हुई थी: कुछ ऐसी चीज़ की इच्छा करना जो अवांछनीय हो, लेकिन समाज के समान रूप से सम्मानित सदस्य के रूप में व्यवहार किए जाने के लिए महत्वपूर्ण हो।
समलैंगिक लोगों को राज्य की घुसपैठ से बचाने में, एक विधायिका अंततः सीधे लोगों के खिलाफ भेदभाव करने वाला पहला कानून बनाने में सफल हो सकती है। लेकिन कोई भी उत्सव इस अंतर्निहित धारणा से प्रभावित होगा कि सुप्रियो के सभी न्यायाधीशों के महत्वपूर्ण बयानों के बावजूद, राज्य समलैंगिक लोगों की उपेक्षा कर रहा है।
यहां मुद्दा यह है कि समलैंगिक लोग एक प्रमुख समूह हैं जो लिव-इन रिलेशनशिप की कानूनी मान्यता से लाभान्वित हो सकते हैं। उन्हें बाहर करके, भाग-3 अपने अस्तित्व को उचित ठहराने में और भी विफल हो जाता है।
निष्कर्ष
कोई कह सकता है कि कानून, केवल युवा पार्टनर्स की नैतिक रूप से निगरानी करना चाहता है। नई भारतीय न्याय संहिता में व्यभिचार के अपराधीकरण के हालिया रिवाइवल/पुनरुद्धार को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके पूर्ववर्ती को असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद, यह पहली बार नहीं होगा कि राज्य अपने निवासियों के नैतिक कार्यों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
विधेयक उत्तराखंड के गैर-निवासियों पर लागू होता है, जो एक महीने के भीतर लिव-इन स्टेटमेंट जमा न करने पर आपराधिक दंड देता है, इसमें विशेष रूप से "साझा घरों" के भीतर किराए का आवास शामिल है और 21 वर्ष से कम उम्र के पार्टनर्स का नोटिस उनके माता-पिता को भेजता है, जो नैतिक मामले पर राज्य के नियंत्रण का विस्तार है।
बाद वाला, आखिरकार, एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां दो अठारह वर्षीय लोग अपने माता-पिता को सूचित किए बिना शादी कर सकते हैं, लेकिन एक बीस वर्षीय व्यक्ति कानूनी तौर पर अपने माता-पिता को सूचना दिए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश नहीं कर सकता है।
समानता के अधिकार न्यायशास्त्र के तहत इस तरह के भेदभाव को बनाए रखना कठिन है, जिसके लिए आवश्यक है कि भेदभाव के लिए कानून के उद्देश्य और भेदभाव के बीच एक उचित संबंध हो।
उत्तराखंड में हाल की घटनाएं, जैसे कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के साथ मारपीट और हत्या, और समलैंगिक याचिकाकर्ताओं का अदालत के सामने मुकर जाना यह दर्शाता है कि इस तरह का कानून एक वैध उद्देश्य पूरा कर सकता है।
लेकिन यह विधेयक जिस स्थिति में है, वह इसे बहिष्करणीय और भ्रमित करने वाला बनाकर उन लोगों की मदद करने में विफल रहता है जिन्हें लिव-इन संबंधों में राज्य के समर्थन की आवश्यकता होती है।
उत्तराखंड विधान सभा के बुद्धिमान विधायकों को यह याद रखना चाहिए कि संवैधानिक नैतिकता को राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि भाग-3 पुरानी नैतिकता को लागू करने के लिए एक उपकरण मात्र बनकर न रह जाए।
फरहान ज़िया, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, अहमदाबाद में एक कानूनी सशक्तिकरण सुविधाकर्ता हैं।
सौजन्य: द लीफ़लेट
मूल अंग्रेजी लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: For Whom is Uttarakhand’s New Live-in Relationship Law?
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।





















