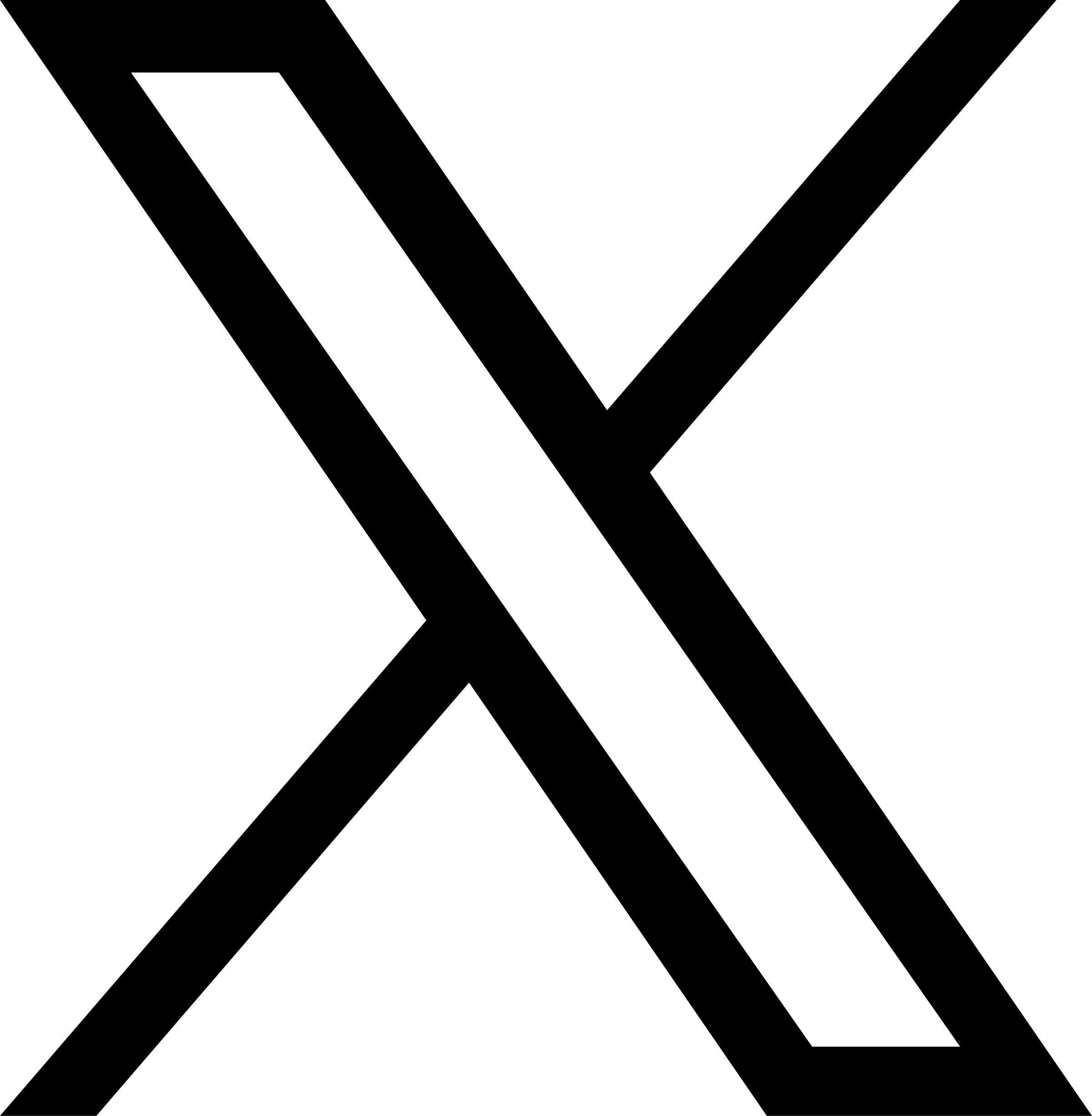सट्टेबाजी, टैरिफ़ की धमकी और कामगार

यह तो एक जानी-मानी बात रही है कि सट्टेबाजी, किसी माल की तंगी की बुनियादी स्थिति को, जमाखोरी को बढ़ावा देने के जरिए और बिगाड़ सकती है। यहां तक कि सट्टेबाजी, किसी बुनियादी तंगी के बिना ही पूरी तरह से कृत्रिम तरीके से तंगी भी पैदा कर सकती है और इस तरह से मेहनतकश जनता की जिंदगियों की बर्बादी कर सकती है और तब तो खासतौर पर ऐसी बर्बादी कर सकती है, जब सट्टा बाजार की शिकार होने वाली वस्तु, जिंदगी के लिए बुनियादी जरूरत की चीज हो।
मुद्रा बाजार सट्टेबाजी और मेहनतकशों पर चोट
मिसाल के तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रिटिश राज के जमाने में, भारत के पूर्वी मोर्चे पर घाटे की वित्त व्यवस्था के जरिए संचालित युद्ध के खर्चे के चलते, खाद्यान्न बाजार में फालतू मांग की जिस स्थिति के चलते, 1943 के बंगाल के अकाल में 30 लाख लोग मारे गए थे, उस संकट को अनाज की जमाखोरी ने और बढ़ाने का काम किया था। लेकिन, आज का नव-उदारवादी निजाम कुछ ऐसा करता है, जो इससे भी बढ़कर है। नव-उदारवादी निजाम, न सिर्फ मेहनतकश जनता के गुजारे के खर्च को सीधे-सीधे मालों के बाजारों में सट्टेबाजी पर निर्भर बनाता है, बल्कि उसे मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी पर भी निर्भर बना देता है।
चूंकि नव-उदारवादी निजाम में पूंजी के प्रवाहों पर, जिसमें वित्तीय प्रवाह भी शामिल हैं, नियंत्रण हटाए जा चुके होते हैं और विनिमय की दरें बाजार से तय हो रही होती हैं, सटोरिये अगर मिसाल के तौर पर डालर के रूप में फंड किसी देश से बाहर ले जाने की प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं, तो इससे उस देश की मुद्रा की विनिमय दर का अवमूल्यन हो जाता है, जिससे स्थानीय मुद्रा में आयातों की कीमतें बढ़ जाती हैं। और अगर इन आयात में तेल जैसी आवश्यक लागत सामग्री भी शामिल होती है तो, इससे समग्रता में ही उस अर्थव्यवस्था में लागत में उछाल आता है। और इससे मुद्रास्फीति पैदा होती है जो वास्तविक मजदूरियों में गिरावट पैदा करती है या इससे भी अधिक सामान्य रूप से मेहनतकशों की वास्तविक आय में गिरावट लाती है।
वास्तव में एक ऐसी दुनिया में, जहां मुनाफे का हिस्सा तयशुदा होता है, इस तरह के लागत उछाल से पैदा होने वाली मुद्रास्फीति, मेहनतकश जनता की वास्तविक आमदनियों के निचोड़े जाने पर ही खत्म हो सकती है। मेहनतकशों की वास्तविक आमदनियों को इस तरह इसलिए निचोड़ा जाता है क्योंकि उनकी मुद्रा आमदनियों को, कीमतों के साथ जोड़ा नहीं जाता है। इसलिए, नव-उदारवादी निजाम की असली निशानी यह है कि इसमें करोड़ों मेहनतकशों की वास्तविक जीवन दशाओं को, मुट्ठीभर अंतर्राष्ट्रीय सटोरियों की झकों और लालचों के भरोसे छोड़ दिया जाता है।
वित्त के पलायन और अंतर्प्रवाह में विसंगति
किसी को यह लग सकता है कि जिस तरह से वित्तीय बहिर्प्रवाह की कोई भी प्रवृत्ति, विनिमय दर के अवमूल्यन के जरिए, मेहनतकश जनता की जीवन दशाओं में गिरावट पैदा करती है, उसी तर्क से इसकी विपरीत प्रवृत्ति यानी वित्त के ऐसे अंत:प्रवाह आने की प्रवृत्ति का, जो किसी भी दौर के स्वायत्त रूप से तय होने वाले चालू खाता घाटों से फालतू हों, पहली स्थिति से उल्टा असर होना चाहिए और इसके चलते संबंधित देश की मुद्रा की विनिमय दर में बढ़ोतरी होनी चाहिए और इस तरह, मेहनतकश अवाम की दशा में सुधार लाते हुए, गुजारे के खर्च में कमी होनी चाहिए। लेकिन, वास्तव में ऐसा होता नहीं है और वित्त के अंतप्रवाहों और बहिप्रवाहों के प्रभावों में हम एक विसंगति देखते हैं। जब बाहर से वित्त का प्रवाह आता है, अगर इसके प्रभाव से विनियम दर में बढ़ोतरी होने दी जाती है, तो संबंधित देश का घरेलू उत्पादन, आयात के मुकाबले में गैर-प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। इस तरह घरेलू उत्पादन सिकुड़ेगा और आयात बढ़ेगा और अगर उस देश का केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप नहीं करता है तो, आयात में बढ़ोतरी का पैमाना इतना बड़ा रखना होगा कि वह अतिरिक्त वित्तीय प्रवाहों का सोख सकता हो। ऐसी सूरत में संबंधित देश खुद अपने ‘‘निरुद्योगीकरण’’ के लिए वित्त जुटाने के लिए, अपने सिर पर विदेशियों का कर्ज चढ़ा रहा होगा, जोकि जाहिर है कि सरासर बेतुकी बात होगी।
ऐसी बेतुकी स्थितियों से बचने के लिए, तीसरी दुनिया के देशों के केंद्रीय बैंक, विनिमय दर को बढऩे से रोकने के लिए हस्तक्षेप करते हैं और अतिरिक्त वित्तीय प्रवाह को, संचित विदेशी मुद्रा भंडारों के रूप में जमा कर के रखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यही करता आ रहा था।
इसलिए, वित्तीय अंतर्प्रवाह और वित्तीय बहिर्प्रवाह में विसंगति इस चीज में निहित है कि जहां बहिर्प्रवाहों से विनिमय दर में अवमूल्यन होता है और इसलिए लागत उछाल से पैदा होने वाली मुद्रास्फीति के जरिए मेहनतकशों की वास्तविक आमदनियों को सिकोड़ा जाता है, वहीं अंतर्प्रवाहों को अतिरिक्त संचित कोष के रूप में जमा कर के रख भर लिया जाता है और इसका विनियम दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बेशक, इस तरह के संचित कोष का हाथ में होना, वित्तीय बहिर्प्रवाहों के खिलाफ धक्का सोखने वाले गद्दे का काम करता है और इसलिए जब भी ऐसे बहिप्र्रवाह होते हैं, इन संचित कोषों में कुछ विदेशी मुद्रा निकाल दी जाती है, जिससे विनिमय दर में अवमूल्यन को रोका जा सके। लेकिन, चूंकि संचित विदेशी मुद्रा कोष में से यह निकासी, विनिमय दर में अवमूल्यन की प्रत्याशाओं को प्रबल करने का काम करती है और इसलिए वित्त के और बहिप्र्रवाह का कारण बनती है, केंद्रीय बैंक सामान्य तौर पर विदेशी मुद्रा संचित कोष खाली नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए, वे विनियम दर में अवमूल्यन को पूरी तरह से रोकते भी नहीं हैं। इसलिए, थोड़ा अवमूल्यन होता है और थोड़ी संचित कोष में कमी होती है। कुल मिलाकर इसका नतीजा यह होता है कि मेहनतकश जनता की वास्तविक आमदनियों को सिकोड़ा जा रहा होता है, जैसा कि भारत में हाल के महीनों में होता रहा है।
इस तरह बुनियादी विसंगति और इसलिए हमारी बुनियादी प्रस्थापना की वैधता ज्यों की त्यों बनी रहती है यानी यही कि वित्तीय बहिर्प्रवाहों से तो विनिमय दर में अवमूल्यन होता है और इसलिए मेहनतकश जनता की वास्तविक आमदनियों में गिरावट आती है, जबकि वित्तीय अंतप्र्रवाहों को चालू विनिमय दरों पर संचित कोष के रूप में जमा भर कर लिया जाता है और इसका विनिमय दर को बढ़ाने वाला कोई प्रभाव नहीं होता है। यह विसंगति वक्त गुजरने के साथ विनिमय दर में एक निरंतर गिरावट के रूप में सामने आती है और नव-उदारवादी निजाम में भारत में हम ठीक यही देखते आए हैं। भारत में आर्थिक ‘‘उदारीकरण’’ के आने से ऐन पहले, 10 नवंबर 1990 को जब चंद्रशेखर ने सरकार ने सत्ता संभाली थी, विनिमय दर एक डालर बराबर 17.50 रु0 की थी। और 15 नवंबर 2025 को इन पंक्तियों के लिखे जाने तक, विनिमय दर एक डालर बराबर 88.50 रु0 हो चुकी है। नव-उदारवाद के दौर में रुपए का इतना भारी अवमूल्यन हुआ है। एक ओर 400 फीसद से अधिक का यह अवमूल्यन है और दूसरी ओर, आजादी के बाद से नव-उदारीकरण से पहले के पूरे दौर में, यानी 1947 से 1990 तक, 33.3 फीसद अवमूल्यन ही हुआ था।
ट्रंप टैरिफ, तेल के दाम और मेहनतकशों पर चोट
इस सब का संबंध तीसरी दुनिया में एक नव-उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित प्रवृत्ति से है। इसके अलावा एक और भी रास्ता है जिससे तीसरी दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था, नव-उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत आयात लागत उछाल संचालित मुद्रास्फीति की शिकार हो जाती है और इसे आज ट्रंप के टैरिफ हमले के संदर्भ में देखा जा सकता है। ट्रंप आज भारत के खिलाफ इस आधार पर दंडात्मक टैरिफ थोप रहा है कि भारत, रूसी तेल खरीदने के जरिए, रूस के खिलाफ अमरीका तथा अन्य साम्राज्यवादी देशों द्वारा इकतरफा तरीके से लगायी गयी पाबंदियों का उल्लंघन कर रहा है। चूंकि नव-उदारवादी निजाम के अपनाए जाने से भारत की आत्मनिर्भरता को कमजोर किया जा चुका है और चूंकि मोदी सरकार नव-उदारवादी नीतियों को पलटना नहीं चाहती है और उसके पास अमरीका के खिलाफ जवाबी कदम उठाने के लिए हिम्मत भी नहीं है, उसने पूरी तरह से अमेरिकी दबाव के सामने घुटने टेक दिए हैं और रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए तैयार हो गयी है। भारत की सरकार तो इस सचाई को स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन ट्रंप ने साफ-साफ शब्दों में इस बात का एलान कर दिया है और उनकी बात पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं है।
भारत का रूस से तेल खरीदना बंद करना, दो अलग-अलग कारणों से देश में तेल की कीमतें बढ़ाएगा। पहला कारण तो यही है कि रूसी तेल चूंकि सस्ता है, उसकी जगह तुलनात्मक रूप से महंगा तेल ले रहा होगा और इस तरह रूस से तेल नहीं खरीदना, वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर भी भारत में तेल की कीमतें बढ़ा रहा होगा। दूसरे कारण का संबंध इस तथ्य से है कि अगर रूस को तेल की आपूर्ति से काट दिया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें खुद ब खुद बढ़ जाएंगी क्योंकि इस सूरत में विश्व अर्थव्यवस्था में तेल की मांग के मुकाबले में, कुल मिलाकर तेल की आपूर्ति में कमी हो गयी होगी। इससे भारत में तेल की कीमतें और बढ़ जाएंगी।
देश में तेल की कीमतों के बढऩे से, अर्थव्यवस्था में लागत मूल्य उछाल आएगा और यह खत्म होगा, मेहनतकश जनता की वास्तविक आमदनियों को सिकोडऩे पर। इसलिए, रूस से तेल खरीदना बंद करने के जरिए भारत के अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेकने का तेल की कीमतों पर ठीक वही असर पड़ेगा, जो विनिमय दर में अवमूल्यन का पड़ता है। और इसके फलस्वरूप ठीक उसी तरह से देश के मेहनतकशों की आय को सिकोड़ा जा रहा होगा।
अमेरिकी साम्राज्यवादी दीदादिलेरी
रूस के खिलाफ अमरीकी पाबंदियां सिर्फ राजनीतिक-रणनीतिक कारणों से ही नहीं थोपी गयी हैं बल्कि इसलिए भी थोपी गयी हैं ताकि अपेक्षाकृत महंगे अमेरिकी तेल के लिए बाजार के आकार में बढ़ोतरी की जा सके। यूरोप को अमेरिका पहले ही अपने हिसाब से रास्ते पर ला चुका है और वह सस्ती रूसी ऊर्जा की जगह पर, कहीं महंगी अमेरिकी ऊर्जा को लाने के जरिए, ऐसा काम कर चुका है जिसे आर्थिक हराकीरी या आत्महत्या ही कहा जा सकता है। ऊर्जा के इस तरह प्रतिस्थापन के जरिए, जर्मनी बाकायदा निरुद्योगीकरण के रास्ते पर चल पड़ा है और जर्मन मजदूर पहले ही एक बहुत ठंडी सर्दी की मुश्किलें झेल चुके हैं। अब अमेरिका के ऊर्जा बाजार को बड़ा करने के लिए, भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों में भी मेहनतकश जनता को और तकलीफें झेलनी होंगी।
यह अमेरिका की साम्राज्यवादी दीदादिलेरी का ही जोरदार एलान है कि वह खुल्लमखुल्ला, दुनिया भर के मेहनतकशाों से कुर्बानियों की मांग कर रहा है और वह भी सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने ऊर्जा बाजार का आकार बढ़ाकर, अपने ही आर्थिक स्वार्थों को आगे बढ़ा सके। और यह अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा बांहें मरोड़े जाने के सामने, वर्तमान भारत सरकार के पूरी तरह से लाचार होकर रह जाने का भी जोरदार एलान है। यह सरकार, उस अमेरिकी प्रशासन को खुश करने के लिए, जोकि अमेरिकी स्वार्थों को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, भारतीय मेहनतकशों के हितों की बलि देने के लिए तैयार है।
(लेखक दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आर्थिक अध्ययन एवं योजना केंद्र में प्रोफ़ेसर एमेरिटस हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।