हिंदी भाषा को थोपना राज्यों की स्वायत्तता पर एक और हमला होगा
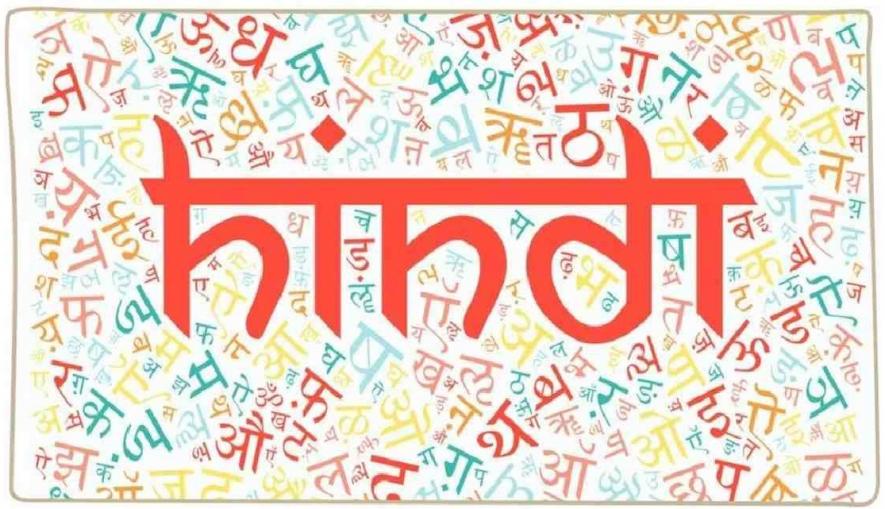
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद की राजभाषा समिति के नेतृत्व में तैयार अपनी 11वीं रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है, जिसके ज़रिए यह सिफारिश की गई है कि देश में "हिंदी का इस्तेमाल शिक्षा और अन्य गतिविधियों के संबंध में एक माध्यम के रूप में सभी तकनीकी और गैर-तकनीकी संस्थानों में किया जाना चाहिए और अंग्रेजी के इस्तेमाल को वैकल्पिक बनाया जाना चाहिए।"
केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), नवोदय विद्यालय (एनवी), केंद्रीय विद्यालय (केवी), और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं।
पृष्ठभूमि
1963 के राजभाषा अधिनियम ने 1976 में समिति के निर्माण की अनुमति दी थी। इसमें संसद से तीस सदस्यों का पैनल होता है; जिसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। यह आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के इस्तेमाल के विकास का मूल्यांकन करता है और राष्ट्रपति को सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट पेश करता है।
संविधान सभा में हिन्दी पर बहस मुख्य रूप से आर.वी. धुलेकर के नेतृत्व में हुई थी, जिन्होंने कहा था कि जो लोग हिंदी नहीं जानते वे भारत में रहने के लायक नहीं हैं। अन्य सदस्यों के विरोध के बावजूद, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अपना लिया था। हालाँकि, एक समझौते के रूप में, यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेजी भी 15 वर्षों तक संघ की राजभाषा रहेगी।
हालांकि, इस समझौते का विरोध हुआ। कोयंबटूर से संविधान सभा में प्रतिनिधि टी ए रामलिंगम चेट्टियार के अनुसार, भाषाई मुद्दा "शायद दक्षिण भारत के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है।" उन्होंने कहा कि दक्षिण के लिए हिन्दी अंग्रेजी जितनी ही विदेशी भाषा है।
जब 15 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ, तो गैर-हिंदी भाषी भारत के महत्वपूर्ण इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, खासकर तमिलनाडु में इनका बड़ा ज़ोर था। जनवरी 1965 में, मदुरै में दंगे शुरू हुए और तेजी से मद्रास तक फेल गए थे। विरोध के कारण, केंद्र ने आधिकारिक भाषा अधिनियम पारित किया गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी जाएगी।
भारत में भाषाओं की बहुलता
संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत में आधिकारिक रूप से 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत में 100 से अधिक गैर-अनुसूचित भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक की आबादी 10,000 से अधिक बोली बोलने वालों की है। इसकी 1,800 मातृभाषाएं, 700 से अधिक विभिन्न भाषाएं, कई बोलियां, और गैर-मान्यता प्राप्त या छोटी भाषाएं हैं।
भारत में लगभग 56 प्रतिशत लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा नहीं मानते हैं। हालांकि, यहां तक कि जिन आंकड़ों के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग हिंदी बोलते दिखाए गए हैं, वे भी उलझे हुए आंकड़े हैं।
1961 और 2011 के बीच, भारत की जनसंख्या का 30.39 प्रतिशत (यानि 13.34 करोड़ आबादी) हिन्दी बोलने वालों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, जो 43.63 प्रतिशत (52.83 करोड़) तक पहुँच गई थी। हालांकि, ऐसा अन्य भाषाओं की कीमत पर हुआ, जिन भाषाओं को न तो सम्मान मिला और बिना उनकी विशेषताओं को साझा किए उन्हे हिन्दी में शामिल कर लिया गया। जनगणना के आंकड़ों की जांच से पता चलता है कि यह उधार ली गई महिमा है जिसका आनंद हिन्दी उठा रही है। कुरमाली और मगही या मगधी पर विचार करें, जिन्हें 1971 की जनगणना रिपोर्ट में हिंदी के तहत मातृभाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
जनगणना रिपोर्ट में भाषा वर्गीकरण में 1971 के संशोधन से काफी प्रभाव पड़ा था। 1961 में, केवल दस मातृभाषाओं- अवधी, बघेलखंडी, ब्रज भाषा, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़ी, खडीबोली, लारिया, लोधी, परदेसी और पावर- को हिंदी के तहत वर्गीकृत किया गया था। हालाँकि, 1971 की जनगणना रिपोर्ट में 48 विभिन्न भाषाओं को हिंदी मातृभाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
हिन्दी और राज्य
तमिलनाडु में कांग्रेस सरकार ने 1967 में जब हिंदी थोपी तो विवाद के कारण उसे सत्ता से उखाड़ फेंक दिया गया था, यह वह आंदोलन था जिससे द्रमुक उभरी थी। इसी तरह की राय कभी-कभी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में व्यक्त की जाती है। कई राज्य सरकारें हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल नहीं करती हैं या इसे अपने त्रि-भाषा फॉर्मूले में भी शामिल नहीं करती हैं।
हिंदी को एक जरूरी भाषा बनाने के अलावा, केरल और कर्नाटक ने अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को संस्थागत रूप दिया है। तेलुगु सभी सरकारी स्कूलों में एक जरूरी या अनिवार्य विषय है, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अंग्रेजी माध्यम को लागू करने के लिए एक नई पहल की है। हिंदी शिक्षा पर कम ध्यान दिया गया है। इसी तरह, पूर्वोत्तर में हिंदी सीखना और पढ़ाना कभी भी पसंदीदा गतिविधि नहीं रही है।
भारत की संघीय प्रणाली काफी अनिश्चित है और सबसे खराब स्थिति में है। इसे अक्सर "अर्ध-संघवाद" या "केंद्रीय पूर्वाग्रह का संघवाद" कहा जाता है, जो राज्यों की स्वायत्तता को लगातार चुनौती देती है।
रिपोर्ट कहती है कि "हिंदी का प्रचार केवल केंद्र सरकार के लिए नहीं होना चाहिए। सभी राज्य सरकारों को भी इसे अपने संवैधानिक दायित्वों में शामिल करना चाहिए। समिति को राज्य सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने का अधिकार होना चाहिए।"
यहां मुख्य शब्द "राज्य की सहमति" है, जिसे भुला नहीं जाना चाहिए। हिंदी थोपने को अलग-थलग नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे भारत में सत्ता के केंद्रीकरण के एक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए।
जबकि राजनीतिक रूप से, राज्यों के पास हमेशा से कानून बनाने की शक्ति बहुत कम रही है। संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत विधान के विषयों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया है: संघ सूची, जिस पर संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची, जिसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, और समवर्ती सूची, जहां संघ और राज्य संयुक्त रूप से कानून बना सकते हैं।
संघीय सूची में सबसे अधिक सूचियाँ हैं, जो संसद के विधायी क्षेत्राधिकार को और अधिक व्यापक बनाती हैं। संसद के पास अवशिष्ट शक्तियाँ भी हैं, जिसका अर्थ है कि वह उन विषयों पर कानून बना सकती है जो सूचियाँ बनाते समय किसी सूची शामिल नहीं थे, जैसे कि ई-कॉमर्स आदि। समवर्ती सूची के संबंध में संसद को राज्य विधानसभाओं पर अधिक शक्ति हासिल है।
इसलिए, राज्यों से चर्चा किए बिना केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों के कारण राज्यों को अक्सर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम जैसे कई राजनीतिक नेताओं ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि जब केंद्र ने 2021 में तीन कृषि विधेयकों को पारित किया था तो उस समय भी कृषि राज्य सूची का एक हिस्सा था।
राजकोषीय संघवाद ढलान पर है। इसका उपयुक्त उदाहरण, केंद्र द्वारा चुपचाप बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया है, जो प्रबंधन, पूंजी, लेखा परीक्षा और परिसमापन के मामले में सहकारी बैंकों पर आरबीआई के नियामक नियंत्रण का विस्तार करता है। राज्य सूची की प्रविष्टि 32 सहकारी समितियों के "निगमन, विनियमन और समापन" से संबंधित मुद्दों से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, संघ सूची की प्रविष्टि 43 संसद के दायरे से सहकारी संगठनों के निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित विषयों को छूट देती है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 (FY21) के बाद से, जब 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक इसे 41 प्रतिशत होना चाहिए था, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 29-32 प्रतिशत के बीच मँडरा रहा है। राज्यों को कर राजस्व में भारी गिरावट को सहन करने के लिए मजबूर किया गया, भले ही राजकोषीय हस्तांतरण के ज़रिए निचोड़े गए कर का एक बड़ा हिस्सा केंद्रीय कर संग्रह में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि केंद्र ने अतिरिक्त शुल्क और उपकर से होने वाले अप्रत्याशित लाभ को साझा नहीं किया है जिसे पेट्रोल और डीजल जैसे सामानों पर लगाया जाता है।
हिंदी थोपने की नीतियां भारत की संस्कृति के व्यापक समरूपीकरण के साथ-साथ राज्यों की सांस्कृतिक और भाषाई स्वायत्तता की अवहेलना करने का एक ज़बरदस्त प्रयास है। हिंदी को थोपना न केवल गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करने का एक विश्वासघाती रूप है, बल्कि भारतीय राष्ट्र की संघीय प्रकृति पर भी हमला है।
लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक हैं।
मूल रूप से अंग्रेज़ी में प्रकाशित साक्षात्कार को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंः
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।























