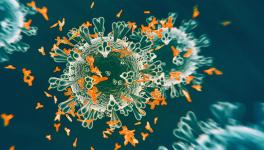दिल्ली में मध्य जुलाई तक Covid-19 चरम स्तर तक पहुंचेगा: डॉ. संजय राय, एम्स

पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर संजय के. राय भारत में नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव का अध्ययन कर रहे हैं और वायरस के व्यवहार का अंदाज़ा लगाने के लिए डॉ. राय आंकड़ों की व्याख्या भी करते हैं। दुनिया भर में इस वायरस से अब तक पांच लाख लोगों की मौत हो चुकी है।
डॉ. राय का एपिडेमियोलॉजी का ज्ञान बहुत गहरा है। उनका अकादमिक रिकॉर्ड अतुलनीय है। वे दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स) के सेंटर फॉर कम्यूनिटी मेडिसिन में प्रोफेसर हैं। अब तक उनके 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। फिलहाल डॉ. राय भारत में इंफ्लूएंजा के असर पर रिसर्च कर रहे हैं। वे नेशनल AIDS नियंत्रण संगठन को तकनीकी मदद भी करते हैं।
इस इंटरव्यू में डॉ राय नोवेल कोरोना वायरस से जूझने में भारत की रणनीति का विश्लेषण करेंगे और आने वाले महीनों में वायरस की दिशा बताएंगे।
चूंकि आप और मैं दोनों ही दिल्ली में रहते हैं, इसलिए हमारे शहर से ही शुरू करते हैं : हम कोरोना वायरस के मामलों में चरम पर पहुंचने के कितने दूर हैं?
यह कहना बहुत मुश्किल है कि हम चरम से कितनी दूर हैं, क्योंकि यह बीमारी एक नए कोरोना वायरस से फैल रही है, जो हमारे लिए पूरी तरह नया है। कुल मामलों की संख्या और कुल टेस्ट में संक्रमित लोगों की संख्या जैसे मानकों के हिसाब से दिल्ली में मध्य जुलाई तक, इसमें एक हफ़्ता आगे-पीछे कर लीजिए, तब तक कोरोना वायरस के मामले अपने चरम पर पहुंच जाएंगे।
29 जून तक दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 80,196 थी। चरम स्तर से मतलब काफ़ी ज़्यादा मामले हो जाना है। क्या अगले 15 दिनों में हम बड़ी संख्या में कोरोना के मामलों का बढ़ना देखने वाले हैं।
नहीं, हमें कोरोना केस में बहुत बड़ा उछाल देखने को नहीं मिलेगा। नोवेल कोरोना वायरस की एपिडेमियोलॉजी से पता चलता है कि ज़्यादातर केसों में लोगों में लक्षण ही नहीं हैं या फिर बहुत कम लक्षण दिखाई देते हैं। यह चीज आम लोगों को पता है। इसलिए वह लोग टेस्ट कराते ही नहीं हैं। जब शुरुआत में कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी थी, तब होम आईसोलेशन का प्रावधान नहीं था। तब डर था कि जो लोगो भी पॉजिटिव टेस्ट होंगे, उन्हें दो हफ़्तों के लिए सांस्थानिक क्वारंटीन किया जाएगा। इस तरह उनका अपने परिवार और दुनिया से पूरी तरह कटाव हो जाएगा।
अगर आपको याद हो तो ICMR ने सीरो सर्विलांस किया था, यह एक ब्लड टेस्ट है, जिसमें किसी व्यक्ति में एंटीबॉडीज़ की मौजूदगी का पता किया जाता है। यह एंटीबॉडी शरीर में SARS-CoV-2 से लड़ने के लिए पैदा होती हैं।
ज़ाहिर तौर पर यह एंटीबॉडीज़ दूसरे बीमारियों से लड़ने वाले एंटीबॉडीज़ से काफ़ी अलग होंगी?
हां, बिल्कुल। हजारों किस्म के कोरोना वायरस होते हैं, लेकिन उनमें से केवल सात ही इंसान को संक्रमित करते हैं। यहां तक कि सामान्य सर्दी भी कोरोना वायरस स्ट्रेन के चलते होती है। हालांकि कुछ किस्म के एंटीबॉडीज़ की मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि सीरो स्क्रीनिंग की जाने के कम से कम 14 दिन पहले व्यक्ति नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित हुए था। शरीर को SARS-CoV-2 से जूझने वाली एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए 2 से 6 हफ़्ते लगते हैं।
दूसरे शब्दों में कहें तो दिल्ली के 80,196 मामले सिर्फ उन्हीं लोगों का आंकड़ा है, जिनके लक्षण स्पष्ट थे।
यह उन लोगों की संख्या प्रदर्शित करता है, जो कई वजहों से स्वास्थ्य ढांचे के संपर्क में आ गए और टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए गए। बल्कि 80,196 में से 50 फ़ीसदी मामले बिना लक्षण वाले लोगों के थे।
क्या इस बात का कोई अनुमान है कि दिल्ली में कितने लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं?
सबसे अच्छा अनुमान सीरोसर्विलांस के ज़रिए लगाया जा सकता है, जो फिलहाल दिल्ली में किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की दो करोड़ आबादी में संक्रमितों का आंकड़ा 10 फ़ीसदी से कम नहीं होगा। मतलब करीब़ 20 लाख लोगों में नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण होगा।
जब संबंधित शहर अपने चरम पर पहुंचता है, तब क्या होता है?
चरम स्तर का मतलब होता है कि संबंधित आबादी के एक निश्चित हिस्से ने नोवेल कोरोना वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। यह प्राकृतिक जरिया है, जिससे किसी वायरस की दर धीमी होती है।
मैं आपको एक कल्पनीय उदाहरण देता हूं। चूंकि यह पूरी तरह नया वायरस है, इसलिए पूरी आबादी इसके प्रति अतिसंवेदनशील है। यहां एक बुनियादी रिप्रोडक्शन नंबर (RO) की अवधारणा है, जिसमें औसत एक व्यक्ति द्वारा संक्रमित किए गए व्यक्तियों का आंकड़ा मापा जाता है। अगर RO 3 है, तो इसका मतलब है कि संबंधित शख्स तीन लोगों को संक्रमित कर रहा है, अगले तीन लोग 9 लोगों को संक्रमित करेंगे। यह 9 लोग मिलकर 27 लोगों को और इसी तरीके से चलता रहेगा।
जैसा हमने ऊपर बातचीत में कहा कि दिल्ली की 10 फ़ीसदी आबादी वायरस से संक्रमित हो चुकी है, अब उनमें वायरस के खिलाफ़ प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो चुका है। इसका मतलब है कि दिल्ली की 20 फ़ीसदी आबादी को दोबोरा कोरोना वायरस संक्रमित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रभावी रिप्रोडक्शन नंबर (R) 3 से 2 पर आ जाएगा। मतलब एक व्यक्ति केवल दो लोगों को ही संक्रमित करेगा। दो व्यक्ति चार को और ऐसा ही चलता रहेगा। ''हर्ड इम्यूनिटी'' के ज़रिए इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हमें किसी समुदाय में SARS-CoV-2 की 50 से 60 फ़ीसदी दर चाहिए होगी।
तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली जैसे ही अपने चरम स्तर पर पहुंचेगी, कोरोना वायरस के मामले कम होना शुरू हो जाएंगे। कितने वक़्त तक दिल्ली चरम पर रहेगी?
यह दिल्ली की आबादी में जुड़ने वाले ''वर्जिन'' या नोवेल कोरोना वायरस के प्रति अतिसंवेदनशील लोगों की संख्या पर निर्भर करता है। कोई शहर नई आबादी या तो नए शिशुओं की पैदाईश से जोड़ता है या फिर प्रवास के ज़रिए। हमारे पास जितने सबूत हैं, जिन लोगों को एक बार कोरोना वायरस हो चुका है, उनमें यह दोबारा नहीं होगा।
लेकिन यह कल बदल भी सकता है। फिलहाल नोवेल कोरोना वायरस स्व-नियंत्रित है। किसी संक्रमण पर प्रतिक्रिया देने के लिए शरीर को दो हफ़्ते का वक़्त लगता है। शरीर इस दौरान एंटीबॉडीज़ पैदा करता है, जो वायरस को मारते हैं। कोविड-19 केवल चार से पांच महीने पुराना है। जो लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, उनमें वायरस से जूझने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ होंगी।
सामान्य सर्दी के लिए प्रतिरोधक क्षमता तीन महीने होती है। 2002-03 में आए SARS-Cov-1 में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता दो साल थी। जहां तक कि SARS-CoV-2 की बात है, हमारे पास फिलहाल प्रतिरोधक क्षमता की अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम सिर्फ़ इतना कह सकते हैं कि जितनी लंबी प्रतिरोधक क्षमता चलेगी, कुल मामलों की संख्या में उतनी ही गिरावट आएगी।
मुंबई, चेन्नई और पूरे भारत के बारे में क्या? चरम स्तर पर पहुंचने के लिए कितना वक़्त लगेगा?
भारत में हर राज्य अलग देश की तरह है। दिल्ली जुलाई मध्य में चरम पर पहुंचेगी। आप मुंबई के लिए एक महीना जोड़ सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, जहां संक्रमण काफ़ी कम है, वहां अगले कुछ महीनों में शायद ही उच्चतम स्तर पहुंचे।
बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बारे में क्या?
हमारे पास इन राज्यों के उस तरह के आंकड़े नहीं हैं, जिनके ज़रिए हम यह दावा कर पाएं कि वहां संक्रमण दर कम है। इसे पता करने का सबसे बेहतर तरीका सीरोसर्विलांस है। फिर भी जितनी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं, मुझे लगता है कि इन राज्यों में संक्रमण दिल्ली, चेन्नई और मुंबई से कम है।
29 जून तक उत्तर प्रदेश में 21,737, बिहार में 8,979 और झारखंड में 2,339 मामले हैं। क्या इन कम मामलों की वजह कम टेस्टिंग हो सकती है क्या?
निश्चित तौर पर, कम आंकड़ों के पीछे यही वज़ह है। फिर भी हमें पॉजिटिविटी रेट- ''कुल टेस्ट की तुलना में पॉजिटिव पाए गए लोगों'' की दर को ध्यान में रखना होगा। मैंने हाल का आंकड़ा नहीं देखा है। लेकिन 15 दिन पहले इन तीन राज्यों के लिए यह दर काफ़ी कम थी। मतलब अगर 100 लोगों के टेस्ट हुए, तो मुंबई और दिल्ली में 30 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि इन राज्यों में सिर्फ़ पांच लोग ही पॉजिटिव मिले।
इन सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रवासी वापस लौटे, फिर भी इनमें पॉजिटिविटी रेट कम कैसे है?
इन तीन राज्यों ने प्रवासियों को अनिवार्य तौर पर दो हफ़्ते के लिए क्वारंटीन की रणनीति अपनाई थी, जिसके चलते यह लोग सीधे अपने परिवार में नहीं जा पाए थे। निश्चित तौर पर इससे मदद मिली होगी।
आप गुवाहाटी और चेन्नई में दोबारा लागू किए गए लॉकडाउन को किस प्रकार से देखते हैं?
अब हमारे पास इस चीज के पर्याप्त सबूत हैं कि मास्क, हाथ धोना और शारीरिक दूरी बनाए रखने जैसे उपाय भी लॉकडाउन की तरह प्रभावी हैं। जबकि लॉकडाउन का दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं पर असर होता है। लोग सिर्फ़ कोविड-19 से ही नहीं मर रहे हैं। दूसरे लोग कैंसर जैसी बीमारियों से भी मारे जा रहे हैं। लॉकडाउन में आर्थिक पहलू को भी ध्यान में रखना होगा।
जिसका प्रभाव दीर्घकालीन होगा। हमें अगले दो से तीन महीनों में इसके प्रभावों के बारे में पता चलेगा। लेकिन लॉकडाउन का स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव तुरंत दिखने लगता है। स्वास्थ्य सेवाएं लॉकडाउन में बुरे तरीके से प्रभावित हुई हैं। लॉकडाउन सही रणनीति नहीं है। इसके ज़रिए बीमारी को फैलने से नहीं रोका जा सकता, केवल इसे धीमा किया जा सकता है।
हमें कोविड-19 के साथ रहने की आदत डालनी होगी। इन आदतों में मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखना, हाथ धोना और ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना शामिल है। कुछ तरीके मौजूद हैं, जिनके ज़रिए हम इस बीमारी के फैलाव को धीमा कर सकते हैं।
आप भारत के लॉकडाउन को किस तरीके से देखते हैं, जिसे दुनिया के सबसे कड़े लॉ़कडाउन में से एक माना गया?
शुरुआती चरण (लॉकडाउन के पहले चरण में) में देश नोवेल कोरोना वायरस के लिए तैयार नहीं था। अगर उद्देश्य लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बताना था, तो लॉकडाउन को मैं मान्यता दे सकता हूं। अगर लॉ़कडाउन के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं में इज़ाफा करना उद्देश्य था, तो भी मैं उसका समर्थन करता हूं।
लेकिन अब तक मुझे ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं मिला, जिसके ज़रिए मैं लॉकडाउन के उद्देश्य को साफ़-साफ़ समझ पाऊं। हालांकि अगर लॉकडाउन का उद्देश्य कोरोना वायरस को खत्म करना था, तो मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। जैसा मैंने पहले ही बताया, वायरस के फैलने की दर को धीमा किया जा सकता है, इसे रोका नहीं जा सकता। बल्कि वायरस को खत्म करने की बात सोचना भी मूर्खतापूर्ण है।
क्या आपको लगता है, पहले चरण के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया जाना सही था?
नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉकडाउन, नोवेल कोरोना वायरस को चुनौती नहीं दे सकता, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। हर भारतीय ने लॉकडाउन की बड़ी कीमत चुकाई है। कोरोना वायरस के मामले अब भी तेजी से बढ़ रहे हैं।
क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन प्रधानमंत्री मोदी को ग़लत सलाह दिए जाने का नतीजा था?
मैं प्रधानमंत्री की गंभीरता पर शक नहीं करता। लेकिन यह संभव हो सकता है कि उन्हें ग़लत सलाह दी गई हो।
क्या हम यह मानते हैं कि अब कोरोना वायरस का सामुदायिक संक्रमण हो रहा है? 18 दिन पहले, 11 जून को ICMR के निदेशक बलराम भार्गव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत में सामुदायिक संक्रमण नहीं है।
सामुदायिक संक्रमण का मतलब है किसी शख़्स में संक्रमण कैसे पहुंचा, उसका पता न लगाया जा सकना। दिल्ली और मुंबई के ज़्यादातर मामलों में हम वायरस के संक्रमण स्रोत का पता नहीं लगा पाए।
11 जून को ICMR के निदेशक ने सीरोसर्विलांस का आंकड़ा भी जारी किया था, जिसमें 30 अप्रैल की रेफरेंस डेट थी। उसके मुताबिक़, भारत की 0.73 फ़ीसदी आबादी संक्रमित हो चुकी है। 30 अप्रैल को कुल मामलों की संख्या 35,500 के आसपास थी। अगर हम 0.73 फ़ीसदी आबादी को संख्या में बदलें, तो आंकड़ा एक करोड़ के आसपास मिलेगा। लेकिन तब मामलों की संख्या 35,500 बताई गई। इसका मतलब है कि हम बाकी के लोगों की पहचान करने में नाकामयाब रहे हैं।
यह ज़ाहिर तौर पर सामुदायिक संक्रमण का न नकारा जा सकने वाला सबूत है। फिर भी ICMR इसे नहीं मान रही है। संगठन बेतुकी बात करते हुए कहता है कि भारत में बिना सामुदायिक संक्रमण के हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर ली जाएगी (डॉ. राय हंसते हैं)। बल्कि ICMR का एक रिसर्च पेपर भी मानता है कि 30 से 40 फ़ीसदी मामलों की पहचान नहीं की जा सकी।
सामुदायिक संक्रमण को न मानने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है?
मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूं? आपको उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए?
क्या आप मानते हैं कि नोवेल कोरोना वायरस का डर बहुत हद तक कम हो गया है?
मुझे लगता है कि डर हमारे बीच ही मौजूद है, भले ही सरकार ने इसे गायब करने की कोशिश की हो। इस डर की एक बड़ी वजह यह है कि नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है, हम इससे व्यवहार के आदी नहीं हैं।
भारत में हालात कब सामान्य होंगे?
अगले साल की शुरुआत तक तो कतई नहीं हो सकते।
आप कह रहे हैं कि अगले साल की शुरुआत तक हालात सामान्य होंगे, क्या तब तक हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी या फिर हम हर्ड इम्यूनिटी विकसित कर चुके होंगे?
कई वैक्सीन विकास के अग्रिम चरणों में हैं। जैसे चीन, अमेरिका या ब्रिटेन में। भारत में अगले दो हफ़्तों में एक वैक्सीन ट्रायल में जाएगा। लेकिन दुनिया अब भी वैक्सीन पाने से 6 महीने दूर है। मान कर चलिए कि वैक्सीन बहुत कारगर है। लेकिन तब भी कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर कितने वक़्त में हम दुनिया की पूरी आबादी के लिए वैक्सीन बना लेंगे? क्या हम दुनिया के हर आदमी को को वैक्सीन लगाने में कामयाब रहेंगे?
आपको लगता है कि अगले 6 महीनों में भारत में हर्ड इम्यूनिटी का विकास हो जाएगा और हम पहले की तरह रहने लगेंगे?
हां, न्यूयॉर्क में कोरोना के मामलों में गिरावट किसी खास कोशिश की वजह से नहीं हुई है। वह प्राकृतिक गिरावट है, जो हर्ड इम्यूनिटी की वजह से हुई है। आप धारावी के बारे में भी ऐसा ही कह सकते हैं। दिल्ली में भी ऐसा ही होगा।
कोई व्यक्ति, जिसे टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसे सांस्थानिक क्वारंटीन में भेजा जाना चाहिए या फिर होम क्वारंटीन में, इस बात पर काफ़ी तीखा विमर्श जारी है। आपको क्या बेहतर लगता है?
मैं होम क्वारंटीन के पक्ष में हूं। हमारा स्वास्थ्य ढांचा बहुत दबाव में है। होम क्वारंटीन से स्वास्थ्य तंत्र पर दबाव कम होता है। किसी संक्रमित व्यक्ति को सिर्फ़ दवाइयों की ही जरूरत नहीं होती, उसे अच्छे तरीके से खाना भी खिलाना होता है। अगर कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की हालत गंभीर नहीं है, तो उसे घर पर ही आईसोलेशन में रखा जाना चाहिए। यह सही बात है कि भारत के हर घर में आईसोलेशन की व्यवस्था नहीं है। उस मामले में सांस्थानिक क्वारंटीन किया जाना ही एकमात्र विकल्प होता है।
अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Delhi Should Reach Covid-19 Peak Mid-July, Predicts AIIMS Professor Sanjay Rai
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।