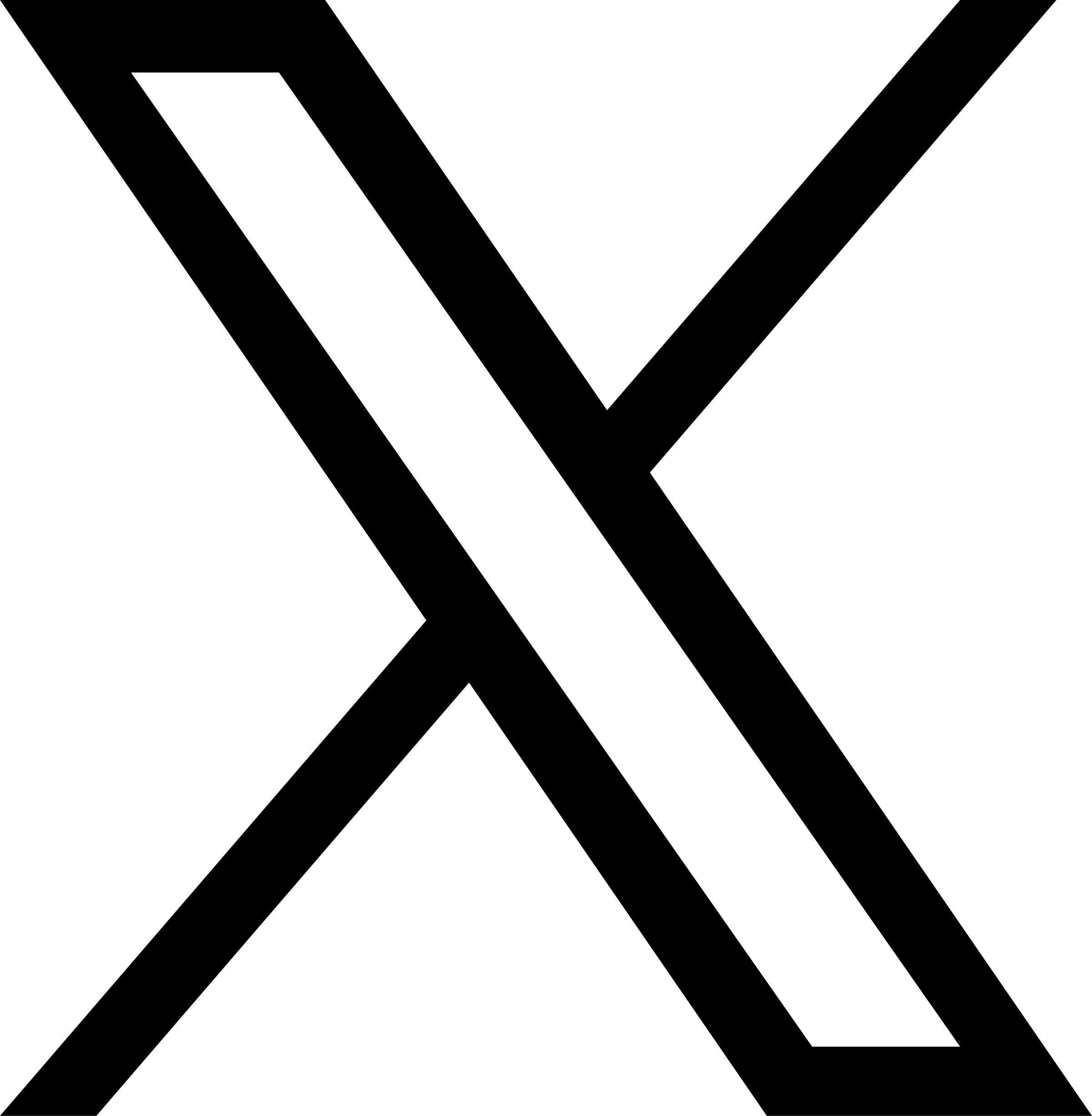अपने बिहार की बदहाली देखकर हैरी को बुरा क्यों नहीं लगता?

2004 में कांग्रेसी नेता और दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार ने द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इस विषय पर चर्चा करते हुए कहा था कि राज्य से बाहर रहने वाले वे बिहारी जन जो बेहतर खा-कमा रहे हैं या अनिवासी बिहारी अपने पैतृक भूमि के उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं? यानी उस बिहार के लिए क्या कर सकते हैं, जो प्रति व्यक्ति जीडीपी के लिहाज से सभी राज्यों में सबसे गरीब है। कुमार का सुझाव था कि "किसी भूले-भटके प्रयोजन में किसी एक प्रोजेक्ट पर दान दे देने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यदि एनआरबी [अनिवासी बिहारी लोगों] को एकजुट रखा जाए, तो जो बदलाव देखने को मिल सकते हैं वे काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।''
आर्थिक तौर पर बिहार को बदल डालने के लिए अनिवासी बिहारियों को एकजुट करने की बात तो भूल ही जाइए। यहाँ तक कि वे बिहारी प्रवासी मजदूरों को मदद पहुंचाने तक के लिए एकजुट नहीं हो सके, जिन्होंने अपने घरों तक पहुँचने के लिए सैकड़ों मील दूरी का सफर इस तपती गर्मी के मौसम में, भूखे प्यासे, जेब में बिना पैसे के, पुलिस के हाथों मार खाते हुए पूरा किया, जिनके कन्धों पर इस राष्ट्रीय लॉकडाउन को लागू कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिससे कि इस नवीनतम कोरोनावायरस के सामुदायिक प्रसारण पर रोक लगाई जा सके।
यह निराशाजनक तस्वीर किसी दूर-दराज के इलाके की नहीं है बल्कि दिल्ली की है, जहाँ मीडिया सहित नौकरशाही, अकादमिक जगत और असंख्य पेशों पर बिहारियों का वर्चस्व बना हुआ है। बिहारी मजदूरों की दुर्दशा के प्रति उनकी उदासीनता को देखते हुए लेखक अमितवा कुमार द्वारा टाइम्स ऑफ़ इंडिया की कहानी में किया गया यह दावा झूठा सा लगता है: "आप बिहार से लड़के को बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन आप लड़के के भीतर बसे बिहार को कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते।"
प्रवासी मजदूरों की कल्पना के अभिन्न अंग के रूप में बिहार हमेशा से बना रहा है, जिसे कि भूख और कोविड-19 की बीमारी जो कि नवीनतम कोरोनावायरस के चलते चारों ओर फ़ैल रही है, से बचने के लिए उनके अपने-अपने घरों की ओर निकल भागने में देखा जा सकता है। जबकि इसके विपरीत अनिवासी बिहारी जो कि ताकतवर और समृद्ध हैं, और जो दिल्ली को ही अपना घर मानते हैं और जहाँ पर एक दिन वे सेवानिवृत्त होंगे और अंतिम साँस लेंगे, के लिए बिहार अब स्मृतियों में याद के रूप में बनकर रह गया है।
बिहारियों के इन दो समूहों को अलग करना इनके भिन्न वर्गों, संस्कृति और इतिहास की खाई को दर्शाता है।
एक श्रेणी के बतौर इन अनिवासी बिहारियों के दिल्ली में छाने को 1970 के दशक के उत्तरार्ध से देखा जा सकता है। वे आये तो यहाँ अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए थे, लेकिन फिर कभी लौट कर घर नहीं गए। इस मामले में वे अपने से पहले की बिहारी पीढ़ी से भिन्न थे जो राज्य के बाहर से अपनी शिक्षा-दीक्षा पूरी किये, लेकिन हमेशा से अपनी जड़ों से ही जुड़े रहे। कई बार शारीरिक तौर पर लेकिन मानसिक तौर पर तो करीब-करीब हमेशा ही जुड़े थे।
द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के लिए 1998 के अपने लेख में दिवंगत पत्रकार अरविंद एन दास ने बिहार के ऐसे तीन प्रकाशपुंजों को सूचीबद्ध किया था। इसमें राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था, के साथ जगजीवन राम जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जातिगत अपमान का जमकर मुकाबला किया था, और जयप्रकाश नारायण, जो संयुक्त राज्य अमेरिका गए और एक समाजवादी के बतौर लौटे थे। इन सभी ने व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व किया, हालांकि इनके जमाने में कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए बिहार से बाहर निकल भागने की होड़ नहीं लगती थी।
यह सब 1970 के दशक के अंत में और 1980 के दशक के दौरान बदलना शुरू हो चुका था। बिहारियों ने उच्च शिक्षा हासिल करने के नाम पर दिल्ली में एक झुण्ड की शक्ल में आना शुरू कर दिया था। इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी थी कि आपातकाल के खिलाफ चले आंदोलन ने बिहार में कॉलेज शिक्षा व्यवस्था को बाधित कर दिया था। यह स्थिति 1980 के दशक में भी उभरी जिसे दास ने "शैक्षणिक माफिया" नाम दिया, जिसने शैक्षणिक संस्थानों की एक श्रृंखला ही स्थापित कर दी थी। इन सब चीजों ने राजनीतिक-शैक्षणिक उद्यमियों के लिए धन का अंबार खड़ा करने में मदद की, बदले में छात्र चाहे समय बर्बाद करें पर वे अपने लिए प्रतिष्ठित डिग्री हासिल करने में सक्षम थे।
अब चूँकि सार्वजनिक और निजी दोनों ही शिक्षा क्षेत्रों में विकल्प लगातार धूमिल पड़ते दिख रहे थे, इसे देखते हुये बिहारियों ने दिल्ली प्रस्थान के लिए कतार लगा दी। उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखी मिशनरी स्कूलों से की थी और जहाँ तक अंग्रेजी बोलने और जो संस्कृति इसके साथ जुडी है, खासकर उन छात्रों के मुकाबले, जैसे कि दून स्कूल और मेयो कॉलेज वाले छात्रों से मुकाबले में वे खुद के बलबूते पर टिके रह सकते थे। इनमें से ज्यादातर बच्चे उन लोगों के थे जो नौकरशाही के भीतर उच्च पदों पर कार्यरत थे, बड़े जमीनों के मालिक थे या तत्कालीन ज़मींदारी वर्ग से आते थे, या बिजनेस और पेशेवर एलीट परिवारों से थे। शिक्षा के लिए दिल्ली में आकर रहना उनके लिए एक अनुष्ठान था, जिसे उन्हें करना ही था।
लेकिन बिहार से शिक्षा की चाह रख आने वालों में एक भारी संख्या ऐसे लोगों की भी थी जो अंग्रेजीदां पृष्ठभूमि से नहीं आते थे। उन्हें अवमानना के तौर पर हैरी के तौर पर पेश किया गया था, एक शब्द जो उनकी चाहत का चरित्र चित्रण करता था, जो इसके लिए बेकरार थे, भले ही उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो बेहद कुशाग्र बुद्धि के भी थे। महानगरीय संस्कृति से अनजान होने के नाते उनका मखौल उड़ाया गया; उनके बिहारी-नेस पर कई चुटकुले गढ़े गए। उनकी बढ़ती संख्या ने राज्य के मिशनरी स्कूल से आने वाले छात्रों तक को कलंकित कर डाला था। बिहार का हर छात्र अब हैरी था, यह एक नामकरण था, जो पिछड़ेपन और संकीर्णता को दर्शाता है।
अनजाने में ही सही लेकिन इस सांस्कृतिक विभ्रम ने हैरीयों को घेर रखा था, जिसने कईयों को अपने बिहारी-पने को कमतर करने और कुछ को तो पूरी तरह से ही त्यागने के लिए प्रेरित कर डाला था। इसके स्थान पर उन्होंने खुद को महानगरीय पहचान को अपनाने और उसके हिसाब से ढालने में झोंक डाला। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने बिहारी-पने को कुछ लोगों द्वारा दृढ़तापूर्वक सामने रखने की कोशिशें भी की गईं, कह सकते हैं कि एक ऐसे बिहारी के रूप में खुद को प्रदर्शित करने जिसे अपनी पहचान को लेकर कोई शर्मिंदगी नहीं है। इस तरह के प्रयास उस डरावने प्रभावों की ओर इशारा करते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अपनी पहचान को लेकर संघर्ष उठ खड़ा होता है।
इसके अलावा कई अन्य कारक भी थे, जिन्होंने बिहारियों को अपनी प्रांतीय पहचान से दूर करने में अपनी भूमिका निभाई थी। इसमें से एक तो यह है कि बिहारी पहचान कुछ उस तरह के संघर्षों के बीच से नहीं उभरी थी जैसा कि दक्षिण भारत में भाषाई समुदायों द्वारा छेड़ी गई थी। 1911-12 में बिहार को बंगाल से निकालकर अलग किया गया था और फिर 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा को बिहार से अलग कर दिया गया। किसी दूसरे के लिए बिहारी भाषाई व्यक्तित्व को वृहत्तर हिंदी पहचान द्वारा आसानी से समाहित किया जा सकता है, चाहे वहां जीवंत तौर पर कई बोलियों का अस्तित्व ही क्यों न हो।
बिहार की क्षेत्रीय और भाषाई पहचान में सरासर लचीलेपन वाली स्थिति में यह बात अपनेआप जुड़ी है कि हैरी के लिए अपने सांस्कृतिक परिवेश में बदलाव के लिए कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा करने पर उसे इसका लाभ ही मिलता है। महानगरीय संस्कृति को अपनाने में जिसे अंग्रेजी और हिंदी के मुखौटे से खुद को ढंकने से हैरियों को पिछड़ेपन और प्रांतवाद की धारणा से पीछा छुड़ाने में मदद मिलती है, हालांकि कैरियर चमकाने या किसी तरह अपना काम निकलवाने के मामले में बिहारी संभ्रांत नेटवर्क पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है।
इस सांस्कृतिक मुखौटे ने हैरियों और जनसाधारण के बीच में एक खाई को जन्म दिया है। अपने निबंध में दास इस ओर इशारा करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिहारी मजदूरों के प्रवाह को जहाँ उन्हें हरित क्रांति की शुरूआत करने के लिए शोषणकारी मज़दूरी की दरों पर कड़ी मेहनत करनी पड़ी, कभी भी बिहारी बुद्धिजीवियों के लिए यह चिंता का सबब नहीं बन पाया था।
बिहार से “मांसपेशियों के सफाये” से होने वाले दुष्परिणामों पर बहस के बजाय बुद्धिजीवियों ने "बौद्धिक पलायन (सफाए)" के निहितार्थ पर खुद को केंद्रित किया। इसके महत्व को उन्हीं हैरियों ने रेखांकित किया था जो राज्य से गए तो अध्ययन के लिए थे, लेकिन अपने ही आंतरिक सांस्कृतिक राक्षसों से नूरा कुश्ती में लगे थे, और अंततः कह सकते हैं कि दिल्ली और उसके गुड़गांव और नोएडा जैसे उपनगरों में खुद को जमाने में जुटे हुए थे। अच्छी खासी संख्या में कई तो भारत से बाहर जाकर बस चुके थे। आज इनकी कई विदेशी विश्वविद्यालयों, आईटी, स्वास्थ्य सेवा और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में मौजूदगी देखी जा सकती है।
लालू प्रसाद यादव और अन्य पिछड़े वर्गों के उदय के कारण भी संभवतः इन हैरियों को दिल्ली में ही स्थायी तौर पर अपना ठिकाना बनाने के लिए आधार प्रदान करा दिया था। फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में कहीं न कहीं वर्ग-जाति की धार तो थी थी। इन अपहरण की घटनाओं में जो पीड़ित पक्ष था वो हैरियो के सामाजिक समूह से संबंधित थे, अब उनकी दुश्चिंताएं इस शक्तिशाली नैरेटिव के चलते बढती जा रही थी कि यादव की बदौलत बिहार में अब जंगलराज कायम हो चुका है। इन हैरियों ने अपने निष्कर्ष में एक पिछड़े, सामाजिक रूप से भरे हुए बिहार से दूर रहना ही बेहतर रहेगा, ठीक जैसे निष्कर्ष पर विदेशों में बसने से पहले एनआरआई प्रवासी अपने देश के बारे में निकालते हैं।
इसके बावजूद एनआरआई भारतीयों को भारत में संकटकाल की घड़ी में अपनी ओर से प्रतिक्रिया रखते देखा जा सकता है, हालाँकि अक्सर वे खुद को जातीय और धार्मिक विवादों में राज्य की भूमिका की आलोचना करने तक सीमित रखते हैं, जैसा कि हाल के वर्षों में इसे देखा गया है। लेकिन हैरियों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, जो अपने साथी बिहारियों के कष्टों को कम करने के लिए एक दबाव समूह के रूप में एकजुट नहीं हो सके।
इस असफलता में उस हिंदी-अंग्रेजी वाली पहचान का काफी कुछ लेना-देना है, जिसे इन हैरियों ने अपना लिया था। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में मलयालियों की तरह उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वे यहाँ पर अल्पसंख्यक के तौर पर हैं। जबकि दक्षिण भारत में एक अल्पसंख्यक समूह के रूप में अपनी मौजूदगी के बावजूद उसी हिंदी पहचान को इस लॉकडाउन के दौरान हैरियों को आपस में एक मजबूत जोड़ मिला है।
उदाहरण के रूप में सीमांत कुमार सिंह, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), बेंगलुरु के उदाहरण को ही ले लें। बिहार में वापस आने वाले नेटवर्क के जरिये बेंगलुरु में फंसे 450 बिहारी प्रवासी मजदूरों के एक समूह में से किसी एक ने किसी तरह से सिंह को खाने की व्यवस्था कर देने के लिए संपर्क किया था। उन्होंने उन सभी के लिए राशन का प्रबंध किया। जल्द ही उनका फोन नंबर बिहार, झारखंड और ओडिशा के निवासियों के लिए सबसे बड़ी राहत प्राप्त करने का केंद्र बन बन गया, उन सभी राज्यों के निवासियों के लिए जो 85 साल पहले एक समग्र राज्य साझा करते थे।
31 मार्च से सिंह को 60,000 प्रवासी मजदूरों के लिए सूखे राशन पैकेट का इंतजाम करने का श्रेय जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ स्थानीय आबादी ने उनके इन प्रयासों को सफल बनाने में भरपूर मदद पहुंचाई है। प्रवासी मजदूरों को राहत प्रदान कराने के लिए शुरुआती आवेग लेकिन बेंगलुरु के आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैरियों की ओर से ही मिल सका था। चारदीवारी की सुरक्षा वाले एक आवासीय परिसर में रहने वाली उत्तर प्रदेश की एक 14 वर्षीय लड़की ने यहाँ के निवासियों से प्रवासी मजदूरों के बीच वितरण के लिए दैनिक सूखा राशन पैकेट प्रदान करने के लिए पैसे एकत्र करने से इसकी शुरुआत की थी।
बेंगलुरु की इस कहानी से दिल्ली के हैरियों को शर्म आनी चाहिए, जो अपनी सारी ताकत और पैसे के बावजूद बिहारी जन-सामान्य की मदद के लिए आगे आने में विफल रहे। एक युवा बिहारी प्रशासनिक अधिकारी, जिसने हिंदी ह्रदय प्रदेशों से बाहर जाकर इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी स्नातक की उपाधि हासिल की थी और खुद के हैरी की पहचान को बेहद मामूली तौर पर झेला था, का कहना है कि "एक सांस्कृतिक ईकाई के तौर पर हैरी आज एक बार फिर से खुद को परिभाषित करने के दौर से गुजर रहा है।“ वे कहते हैं, हैरियों के बीच में आजकल एक नई प्रवृत्ति जन्मी है, अब वे खुद को मैथिली या मगही उप-क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान के साथ प्रस्तुत करते हैं।
“एक ओर जहाँ उप-क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान हमें बिहारी-भोजपुरी संस्कृति से पृथक तौर पर दर्शाने में मदद करती है, जिसे आम तौर पर नीची निगाह से देखा जाता है। वहीँ दूसरी ओर यह हमें अन्य हिंदी भाषी राज्यों से आने वाले भिन्न समूह के रूप में स्थापित कराता है” उस युवा अधिकारी का कथन था।अपने 1998 के निबंध में दास ने चेतावनी दी थी कि "अगर बिहार ने खुद को नहीं बदला तो यह भारत को अपनी छवि में ढाल देगा।" लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका है। उल्टा इण्डिया और दिल्ली ने ही हैरियों को बदल कर रख दिया है, जैसा तौर-तरीका भारतीय अभिजात्य वर्ग का है। गरीबों के कष्ट उन्हें अब छू भी नहीं पाते वहीँ अपने राजनीतिक आकाओं को उनकी अक्षम्य मूर्खताओं की ओर इंगित करने का इनमें साहस नहीं है। हैरी के पास भूनने के लिए एक अलग मछली है, बजाय कि वो परेशान हो कि बिहार में गरीबों का क्या हो रहा है।
(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं विचार व्यक्तिगत हैं।)
अंग्रेज़ी में यह लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।