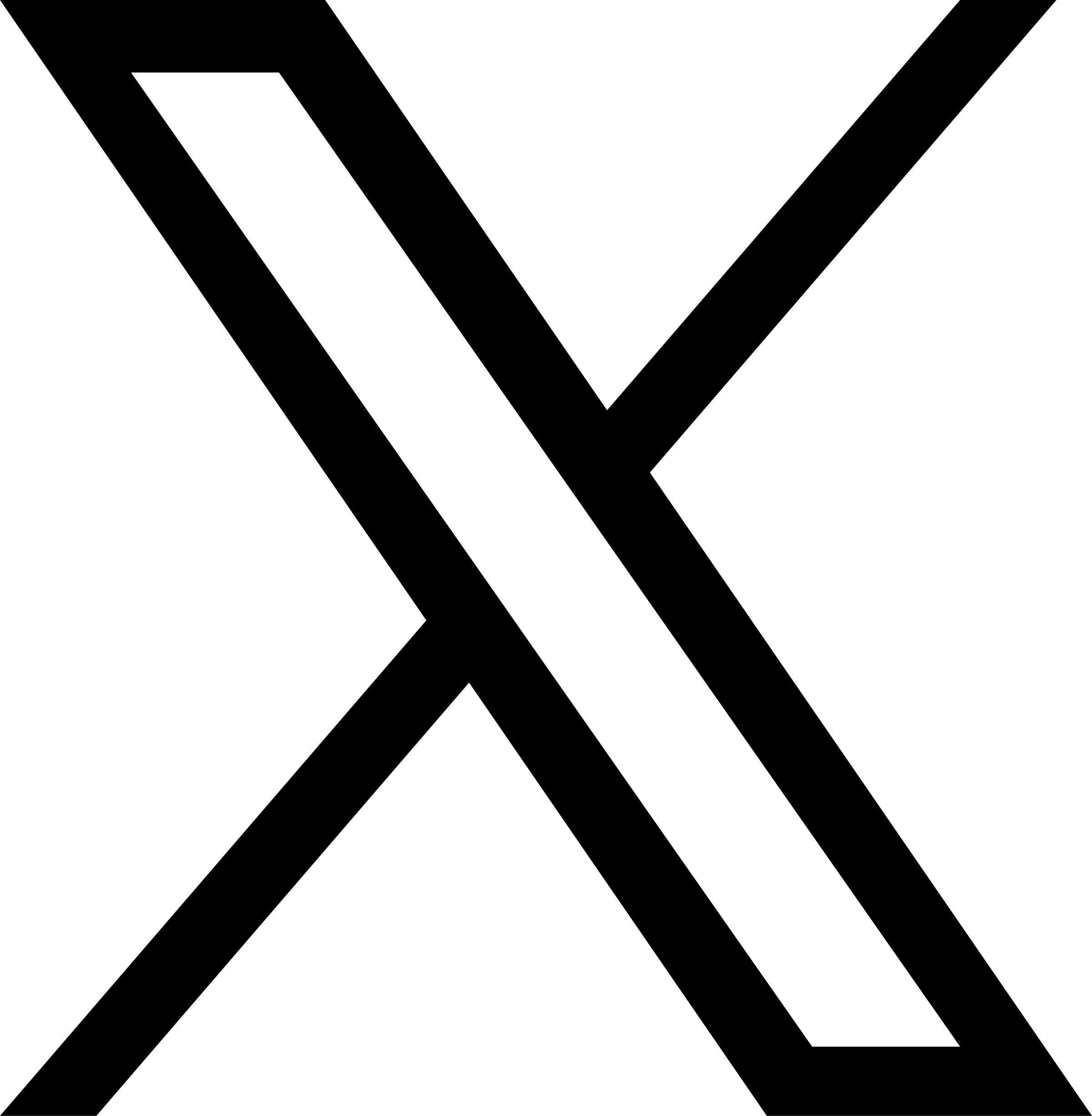"रक़्स करना है तो फिर पांव की ज़ंजीर न देख..." : मजरूह सुल्तानपुरी पुण्यतिथि विशेष

’‘मैं अकेला ही चला था जानिब-ए-मंज़िल मगर/लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया’’ उर्दू अदब में ऐसे बहुत कम शे’र हैं, जो शायर की शिनाख़्त बन गए और आज भी सियासी, समाजी महफ़िलों और तमाम ऐसी बैठकों में कहावतों की तरह दोहराए जाते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी गर अपनी ज़िन्दगी में इस शे’र के अलावा कुछ और नहीं लिखते, तब भी वे इस शे’र के बदौलत ही अदबी दुनिया में अलग से उनकी एक पहचान होती। ये बेशकीमती शे’र है ही ऐसा, जो आज भी हज़ारों की भीड़ को आंदोलित, प्रेरित करने का काम करता है। इस शे’र को लिखे हुए एक लंबा अरसा गुज़र गया, मगर इस शे’र की तासीर ठंडी नही हुई। उर्दू अदब में मजरूह सुल्तानपुरी का आग़ाज़ जिगर मुरादाबादी की शायरी की रिवायतों के साथ हुआ और आख़िरी वक़्त तक उन्होंने इसका दामन नहीं छोड़ा। मजरूह सुल्तानपुरी शुरू में तरक़्क़ीपसंद तहरीक की विचारधारा और सियासत से रजामंद नहीं थे। इस विचारधारा से उनके कुछ इख़्तिलाफ़ (विरोध) थे, लेकिन बाद में वे इस तहरीक के सरगर्म हमसफ़र बन गए। उनका यक़ीन इस बात में पुख़्ता हो गया कि समाजी मक़सद के बिना कोई भी अज़ीम आर्ट पैदा नहीं हो सकती। एक बार उनका यह ख़याल बना, तो उनकी शायरी बामक़सद होती चली गई। मजरूह सुल्तानपुरी की शायरी का शुरूआती दौर, आज़ादी के आंदोलन का दौर था। उस वक़्त जो भी इंक़लाबी मुशायरे होते, वे उनमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते। उनकी ग़ज़लों में तरन्नुम और सादगी का दिलकश मेल होता था। मजरूह की शुरू की ग़ज़लों को यदि देखें, तो उनमें एक बयानिया लहज़ा है, लेकिन जैसे-जैसे उनका तजुर्बा बढ़ा, उनकी ग़ज़लों की ज़बान और मौजूआत में नुमायां तब्दीली पैदा हुई और इशारियत (सांकेतिकता) और तहदारी (गहराई) में भी इज़ाफ़ा हुआ। तरक़्क़ीपसंद तहरीक के शुरुआती दौर का अध्ययन करें, तो यह बात सामने आती है कि तरक़्क़ीपसंद शायर और आलोचक ग़ज़ल विधा से मुतमईन नहीं थे। उन्होंने अपने तईं ग़ज़ल की पुरजोर मुख़ालिफ़त की, उसे जानबूझकर नज़रअंदाज़ किया।
यहां तक कि शायर-ए-इंक़लाब जोश मलीहाबादी, तो ग़ज़ल को एक काव्य विधा की हैसियत से मुर्दा करार देते थे। विरोध के पीछे अक्सर यह दलीलें होती थीं कि ग़ज़ल नए दौर की ज़रूरतों के लिहाज़ से नाकाफ़ी ज़रिया है। कम अल्फ़ाज़ों, बहरों-छंदों की सीमा का बंधन ख़ुलकर कहने नहीं देता। लिहाज़ा उस दौर में उर्दू अदब में मंसूबाबंद तरीक़े से नज़्म आई। फ़ैज़ अहमद फै़ज़, अली सरदार जाफ़री, साहिर लुधियानवी, कैफ़ी आज़मी, वामिक जौनपुरी और मजाज़ वगैरह शायरों ने एक से बढ़कर एक नज़्में लिखीं। हालांकि इन लोगों ने ग़ज़लें भी लिखीं, लेकिन मजरूह ने सिर्फ ग़ज़ल लिखी।
मजरूह सुल्तानपुरी ने ना सिर्फ ग़ज़लें लिखीं, बल्कि वे उन शायरों में शामिल रहे, जिन्होंने ग़ज़ल की हमेशा तरफ़दारी की और इसे ही अपने जज़्बात के इज़हार का ज़रिया बनाया। ग़ज़ल के बारे में उनका नज़रिया था,‘‘मेरे लिए यही एक मोतबर ज़रिया है। ग़ज़ल की ख़ुसूसियत उसका ईजाजो-इख्तिसार (संक्षिप्तता) और ज़ामइयत (संपूर्णता) व गहराई है। इस ऐतिबार से ये सब से बेहतर सिन्फ़ (विधा) है।’’ ग़ज़ल की जानिब मजरूह की ये बेबाकी और पक्षधरता आख़िर समय तक क़ायम रही। ग़ज़ल के विरोधियों से उन्होंने कभी हार नहीं मानी। प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक सदस्य सज्जाद ज़हीर ने अपनी क़िताब ‘रौशनाई’ में मजरूह सुल्तानपुरी की ग़ज़ल की जानिब इस जज़्बे और हिम्मत की दाद देते हुए लिखा है,‘‘मजरूह को बंबई में गोया दो मोर्चों पर जंग करनी पड़ती थी। एक तरफ वह अपने पहले के रिवायती ग़ज़ल गायकों और शाइरों से तरक़्क़ीपसंदी के उसूलों को सही मनवाने के लिए लड़ते, दूसरी तरफ तरक़्क़ीपसंद लेखकों की अक्सरियत से ग़ज़ल को स्वीकार कराने और उसकी अहमियत को तसलीम करवाने के लिए उन्हें असाधारण साहित्यिक वाद-विवाद करना पड़ता।’’ अलबत्ता रिवायती ग़ज़ल के घिसे-पिटे मौज़ू और तर्जे बयान को उन्होंने अपनी तरफ़ से बदलने की पूरी कोशिश की। जिसमें वे कामयाब भी हुए। मजरूह की शायरी में रूमानियत और इंक़लाब का बेहतरीन संगम है। ऐसी ही उनकी एक ग़ज़ल के कुछ अश्आर इस तरह से हैं, ‘‘अब अहले-दर्द (दर्दवाले आशिक) ये जीने का अहतिमाम (प्रबंध) करें/उसे भुला के गमे-ज़िंदगी (जीवन के दुःख) का नाम करें।/........गुलाम रह चुके, तोड़ें ये बंदे-रुसवाई (बदनामी की जंजीर)/खुद अपने बाजू-ए-मेहनत (परिश्रम करने वाली बांहों का) का एहतिराम करें।’’
मजरूह सुल्तानपुरी की इस बात से हमेशा नाइत्तेफ़ाक़ी रही, कि मौजूदा ज़माने के मसायल को शायराना रूप देने के लिए ग़ज़ल नामौज़ू है, बल्कि उनका तो इससे उलट यह साफ मानना था,‘‘कुछ ऐसी मंजिलें हैं, जहां सिर्फ ग़ज़ल ही शायर का साथ दे सकती है।’’ कमोबेश यही बात काजी अब्दुल गफ़्फ़ार, मजरूह की एक मात्र शायरी की क़िताब ‘ग़ज़ल’ की प्रस्तावना में लिखते हुए कहते हैं, ‘‘मजरूह का शुमार उन तरक़्क़ीपसंद शायरों में होता है, जो कम कहते हैं और (शायद इसलिए) बहुत अच्छा कहते हैं। ग़ज़ल के मैदान में उसने वह सब कुछ कहा है, जिसके लिए बाज तरक़्क़ीपसंद शायर सिर्फ नज़्म का ही पैराया ज़रूरी और नागु़जीर (अनिवार्य) समझते हैं। सही तौर पर उसने ग़ज़ल के कदीम शीशे (बोतल) में एक नई शराब भर दी है।’’ काजी अब्दुल गफ़्फ़ार की यह बात सही भी है। मजरूह की एक नहीं, कई ऐसी ग़ज़लें हैं जिसमें विषय से लेकर उनके कहन का अंदाज़ निराला है। मसलन ‘‘सर पर हवा-ए-जुल्म चले सौ जतन के साथ/अपनी कुलाह कज है उसी बांकपन के साथ।’’, ‘‘जला के मश्अले-जां हम जुनूं-सिफात चले/जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले।’’ मजरूह, मुशायरों के कामयाब शायर थे। ख़ुशगुलू (अच्छा गायक) होने की वजह से जब वे तरन्नुम में अपनी ग़ज़ल पढ़ते, तो श्रोता झूम उठते थे। ग़ज़ल में उनके बग़ावती तेवर अवाम को आंदोलित कर देते। वे मर मिटने को तैयार हो जाते।
मजरूह सुल्तानपुरी के कलाम में हालांकि ज्यादा ग़ज़लें नहीं हैं। उनकी क़िताब ‘ग़ज़ल’ में सिर्फ 50 ग़ज़लें ही संकलित हैं, लेकिन इन ग़ज़लों में से किसी भी ग़ज़ल को कमजोर नहीं कह सकते। उन्होंने अदबी कलाम कम लिखा, लेकिन बेहतर और लाजवाब लिखा। मिसाल के तौर पर उनकी एक नहीं, ऐसी कई ग़ज़लें हैं जिनमें उन्होंने समाजी और सियासी मौज़ूआत को कामयाबी के साथ उठाया है। इनमें उनके बगावती तेवर देखते ही बनते हैं। मुल्क की आज़ादी की तहरीक में ये ग़ज़लें, नारों की तरह इस्तेमाल हुईं। ‘‘सितम को सर-निगूं (झुका सर), जालिम को रुसवा हम भी देखेंगे/चले ऐ अज़्मे बग़ावत (बग़ावत का निश्चय) चल, तमाशा हम भी देखेंगे/...... ज़बीं (माथे) पर ताजे-जर (पूंजी-रूपी ताज), पहलू में जिंदा (जेलखाना), बैंक छाती पर/उठेगा बेकफन कब ये जनाजा हम भी देखेंगे।’’
मजरूह सुल्तानपुरी की शुरूआती दौर की ग़ज़लों पर आज़ादी के आंदोलन का साफ़ असर दिखलाई देता है। दीगर तरक़्क़ीपसंद शायरों की तरह, उनकी भी ग़ज़लों में मुल्क के लिए मर-मिटने का जज़्बा नज़र आता है। ये ग़ज़लें सीधे-सीधे अवाम को संबोधित करते हुए लिखी गई हैं। ‘‘यह जरा दूर पे मंज़िल, यह उजाला, यह सुकूं/ख़्वाब को देख अभी ख़्वाब की ताबीर न देख/देख जिंदां से परे, रंगे-चमन, जोशे-बहार/रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख।’’ अवामी मुशायरों में तरक़्क़ीपसंद शायर जब इस तरह की ग़ज़लें और नज़्में पढ़ते थे, तो पूरा माहौल मुल्क की मुहब्बत से सराबोर हो जाता था। लोग कुछ कर गुज़रने के लिए तैयार हो जाते थे। अप्रत्यक्ष तौर पर ये अवामी मुशायरे अवाम को बेदार करने का काम करते थे। ख़ास तौर से मजरूह की शायरी उन पर गहरा असर करती। लंबे संघर्षों के बाद, जब मुल्क आज़ाद हुआ तो मजरूह सुल्तानपुरी ने इस आज़ादी का इस्तेकबाल करते हुए लिखा,‘‘अहदे-इंक़लाब आया, दौरे-आफ़ताब (सूर्य का युग) आया/मुन्तज़िर (प्रतीक्षित) थीं ये आंखें जिसकी एक ज़माने से/अब ज़मीन गायेगी, हल के साज़ पर नग़मे/वादियों मे नाचेंगे हर तरफ तराने से/अहले-दिल (दिलवाले) उगायेंगे ख़ाक से महो-अंजुम (चांद-सितारे)/अब गुहर (मोती) सुबक (कम कीमत का) होगा जौ के एक दाने से/मनचले बुनेंगे अब रंगो-बू (रंग और गंध) के पैराहन (लिबास)/अब संवर के निकलेगा हुस्न (सौंदर्य) कारखाने से।’’ मजरूह सुल्तानपुरी ने साल 1945 से लेकर साल 2000 तक हिंदी फ़िल्मों के लिए गीत लिखे। अपने पचपन साल के फ़िल्मी सफ़र में उन्होंने 300 फ़िल्मों के लिए तक़रीबन 4000 गीतों की रचना की। फ़िल्मी दुनिया में इतना लंबा समय और इतने सारे गीत किसी भी गीतकार ने नहीं रचे हैं। फ़िल्मी गीतों ने मजरूह सुल्तानपुरी को खूब इज़्ज़त, शोहरत और पैसा दिया। बावजूद इसके वे अदबी काम को ही बेहतर समझते थे। अपने फ़िल्मी गीतों के बारे में उनका कहना था,‘‘फ़िल्मी शायरी मेरे लिए ज़रिया-ए-इज़्ज़त नहीं, बल्कि ज़रिया-ए-मआश (जीविका का साधन) है। मैं अपनी शायरी को कुछ ज़्यादा मैयारी (ऊंचे स्तर की) भी नहीं समझता। इसके ज़रिए मुझे कोई अदबी फ़ायदा भी नहीं पहुंचा है, बल्कि फ़िल्मी मसरूफ़ियत मेरी शेर-गोई (काव्य लेखन) की रफ़्तार में हाइल रही।’’ यह बात सही भी है। फ़िल्मी गानों की मसरूफ़ियत के चलते, वे ज़्यादा अदबी लेखन नहीं कर पाये। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी लिखा, वह उन्हें ऊंचे ग़ज़लकार के दर्जे में शामिल करने के लिए काफ़ी है।
मजरूह सुल्तानपुरी वामपंथी विचारधारा के थे और अपनी इसी विचारधारा की वजह से उन्हें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि उन्हें ज़ेल भी जाना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। वही किया, जो उन्हें पसंद था। जो उनका ज़मीर बोलता था। गु़लाम भारत में वे अंग्रेज हुक़ूमत से टक़्क़र लेते रहे, तो आज़ादी के बाद भी सत्ता और सत्ताधारियों की ग़लत नीतियों के प्रति उनका आलोचनात्मक रुख बरकरार रहा। अपनी एक नज़्म में तो उन्होंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ख़िलाफ़ एक तल्ख़ टिप्पणी कर दी। ‘‘मन में जहर डॉलर के बसा के/फिरती है भारत की अहिंसा/ख़ादी के केंचुल को पहनकर/ये केंचुल लहराने न पाए/अमन का झंडा इस धरती पर/किसने कहा लहराने न पाए/ये भी कोई हिटलर का है चेला/मार लो साथ जाने न पाए/कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू/मार ले साथी जाने न पाए।’’ ज़ाहिर है कि इस टिप्पणी से मुल्क में उस वक्त हंगामा मच गया। महाराष्ट्र सरकार को यह बात नाग़वार गुजरी। मजरूह को मुंबई की आर्थर रोड जेल में डाल दिया गया। उनसे कहा गया कि यदि वे सरकार से माफ़ी मांग लेंगे, तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी सरकार के आगे बिल्कुल भी नहीं झुके और उन्होंने साफ़ कह दिया कि जो लिख दिया, सो लिख दिया। माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। जेल की अंधेरी रातें भी उनका हौसला नहीं तोड़ पाईं। वे वहां भी लगातार साहित्य साधना करते रहे। कारावास में भी उन्होंने अपनी कई बेहतरीन ग़ज़लें लिखीं।‘‘मैं कि एक मेहनत-कश, मैं कि तीरगी-दुश्मन (अंधेरे का शत्रु)/सुब्हे-नौ इबारत है, मेरे मुस्कराने से/अब जु़नूं (उन्माद) पे वो साअत (क्षण) आ पड़ी कि ऐ ‘मजरूह’/आज जख़्मे-सर (सर का घाव) बेहतर, दिल पे चोट खाने से।’’ या फिर ‘‘दस्ते-मुन्इम (पूंजीपति का हाथ) मेरी मेहनत का खरीदार सही/कोई दिन और मैं रुसवा-सरे-बाज़ार सही/फिर भी कहलाऊंगा आवारा-ए-गेसू-ए-बहार (वसंत-रूपी केशों का आवारा दीवाना)/मैं तेरा दामे-ख़िजां (पतझड़ के जाल) लाख गिरफ़्तार सही।’’
24 मई, साल 2000 को 80 साल की उम्र में मजरूह सुल्तानपुरी इस दुनिया से हमेशा के लिए रुख़्सत हो गए।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।